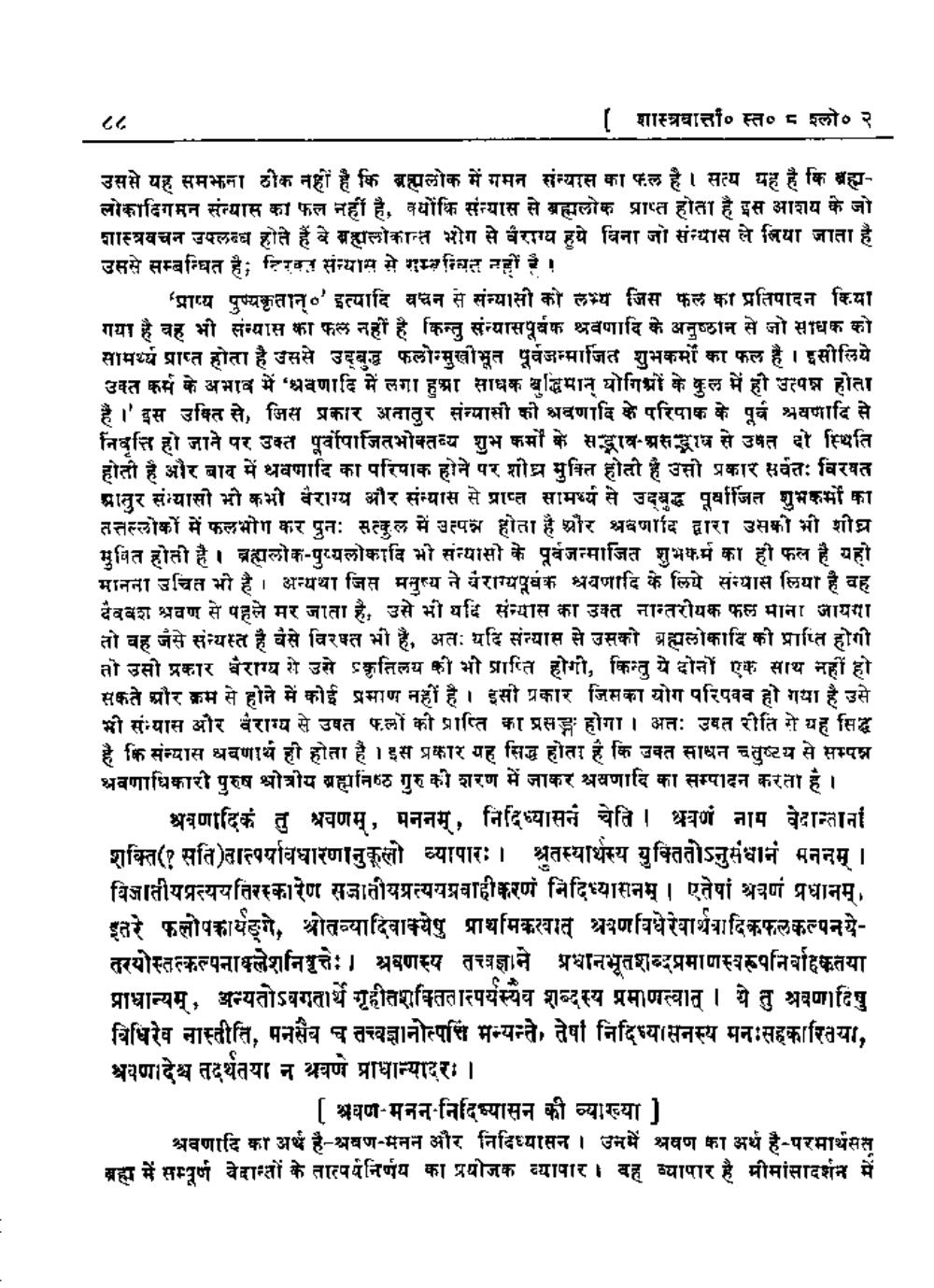________________
८८
[ शास्त्रवा० स्त० ८ श्लो०२
उससे यह समझना ठीक नहीं है कि ब्रह्मलोक में गमन संन्यास का फल है । सत्य यह है कि ब्रह्मलोकादिगमन संन्यास का फल नहीं है, क्योंकि संन्यास से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है इस आशय के जो शास्त्रवचन उपलब्ध होते हैं वे ब्रह्मलोकान्त भोग से वैराग्य हुये विना जो संन्यास ले लिया जाता है उससे सम्बन्धित है; हिरवर संन्यास से गम्भ क्वित नहीं है।
'प्राप्य पुण्यकृतान्०' इत्यादि बचन से संन्यासी को लभ्य जिस फल का प्रतिपादन किया गया है वह भी संन्यास का फल नहीं है किन्तु संन्यासपूर्वक श्रवणादि के अनुष्ठान से जो साधक को सामर्थ्य प्राप्त होता है उससे उद्बुद्ध फलोन्मुखीभूत पूर्वजन्माजित शुभकर्मो का फल है । इसीलिये उक्त कर्म के अभाव में 'श्रवणादि में लगा हुआ साधक बुद्धिमान् योगिनों के कुल में ही उत्पन्न होता है।' इस उक्ति से, जिस प्रकार अनातुर संन्यासी को श्रवणादि के परिपाक के पूर्व श्रवणादि से निवृत्ति हो जाने पर उक्त पूर्वोपाजितभोक्तव्य शुभ कर्मों के सद्भाव-असद्भाव से उबत दो स्थिति होती है और बाद में थवणादि का परिपाक होने पर शीघ्र मुक्ति होती है उसी प्रकार सर्वतः विरवत मातुर संन्यासी भी कभी वैराग्य और संन्यास से प्राप्त सामर्थ्य से उद्बुद्ध पूजित शुभकर्मों का तत्तल्लोकों में फल भोग कर पुनः सत्कुल में उत्पन्न होता है और श्रवणादि द्वारा उसको भी शीघ्र मुक्ति होती है। ब्रह्मलोक-पुण्यलोकादि भी संन्यासो के पूर्वजन्माजित शुभकर्म का ही फल है यही मानना उचित भी है। अन्यथा जिस मनुष्य ने बराग्यपूर्वक श्रवणादि के लिये संन्यास लिया है वह देववश श्रवण से पहले मर जाता है, उसे भी यदि संन्यास का उक्त नान्तरीयक फल माना जायगा तो वह जैसे संन्यस्त है वैसे विरक्त भी है, अतः यदि संन्यास से उसको ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति होगी तो उसी प्रकार बैराग्य से उसे प्रकृतिलय की भी प्राप्ति होगी, किन्तु ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते और क्रम से होने में कोई प्रमाण नहीं है। इसी प्रकार जिसका योग परिपक्व हो गया है उसे भी संन्यास और वैराग्य से उषत फलों की प्राप्ति का प्रसङ्ग होगा। अत: उषत रीति गे यह सिद्ध है कि संन्यास धवणार्थ ही होता है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि उक्त साधन चतुष्टय से सम्पन्न श्रवणाधिकारी पुरुष श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर श्रवणादि का सम्पादन करता है।
श्रवणादिकं तु श्रवणम् , मननम् , निदिध्यासनं चेति । श्रवणं नाय वेदान्तानां शक्ति(? सति)तात्पर्यावधारणानुकूलो व्यापारः। श्रुतस्यार्थस्य युक्तितोऽनुसंधान मननम् | विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेण सजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणं निदिध्यासनम् । एतेषां श्रवणं प्रधानम्, इतरे फलोपकायेंगे, श्रोतव्यादिवाक्येषु प्राथमिकत्वात श्रवण विधेरेवावादिक्रफलकल्पनयेतरयोस्तत्कल्पनाफ्लेशनिवृत्तः। श्रवणस्य तत्वज्ञाने प्रधानभूतशब्दप्रमाणस्वरूपनिर्वाहकतया प्राधान्यम्, अन्यतोऽवगतार्थे गृहीतशक्तितात्पर्यस्यय शब्दस्य प्रमाणत्वात् । ये तु श्रवणादिषु विधिरेव नास्तीति, मनसैव च तत्त्वज्ञानोत्पत्ति मन्यन्ते, तेषां निदिध्यासनस्य मनःसहकारितया, श्रवणादेश्च तदर्थतया न अवणे प्राधान्यादरः ।
[श्रवण-मनन-निदिध्यासन की व्याख्या ) श्रवणादि का अर्थ है-श्रवण-मनन और निदिध्यासन । उनमें श्रवण का अर्थ है-परमार्थसस ब्रह्म में सम्पूर्ण वेदान्तों के तात्पर्यनिर्णय का प्रयोजक व्यापार। वह व्यापार है मीमांसादर्शन में