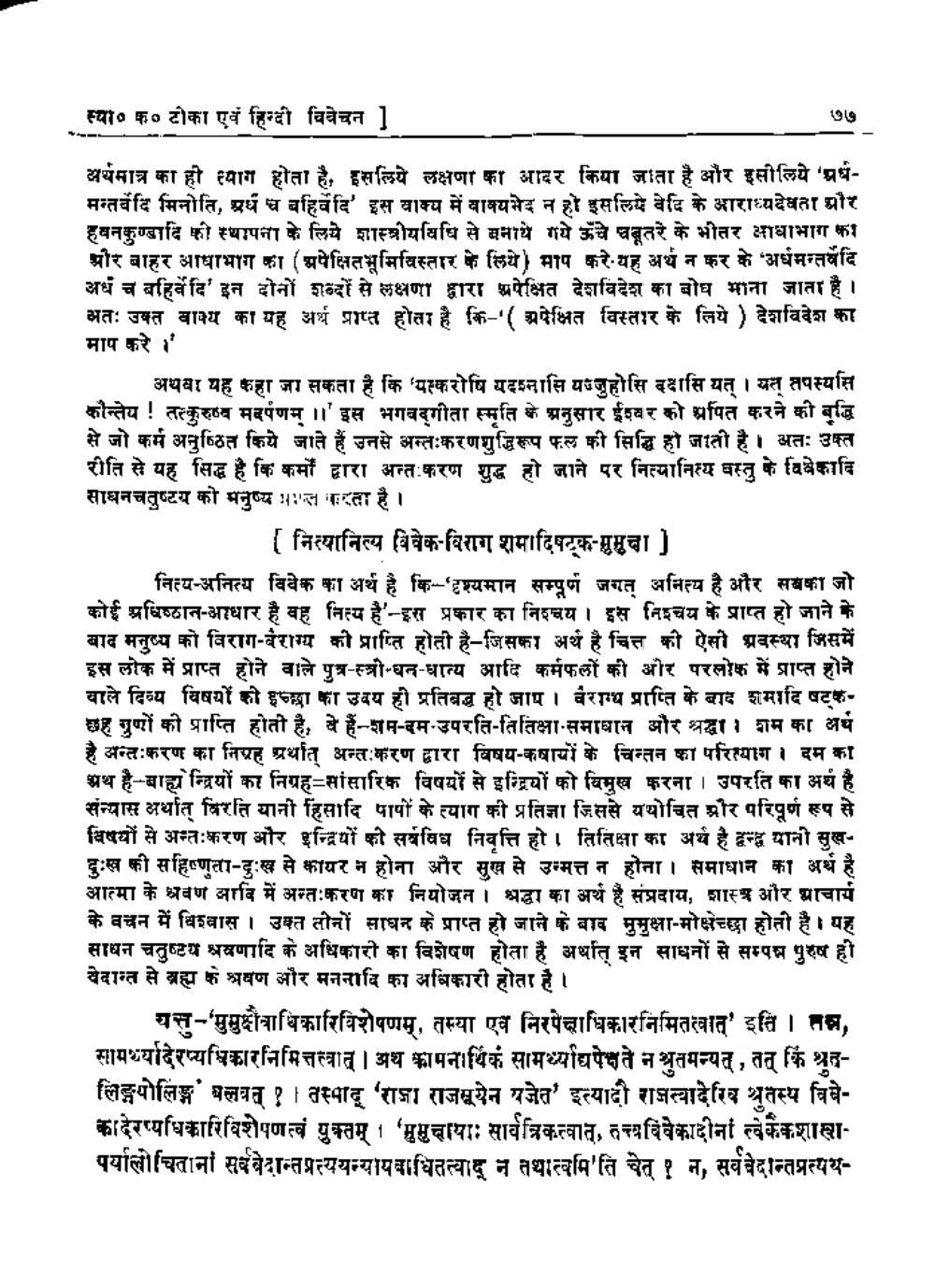________________
स्याका टोका एवं हिन्दी विवेचन ]
अर्थमात्र काही त्याग होता है, इसलिये लक्षणा का आदर किया जाता है और इसीलिये 'अर्धमन्तर्वेदि मिनोति, प्रधं च बहिर्वेदि' इस वाक्य में वाक्यभेद न हो इसलिये वेदि के आराध्यदेवता और हवनकुण्डादि की स्थापना के लिये शास्त्रीयविधि से बनाये गये ऊँचे चबूतरे के भीतर आधाभाग का
और बाहर आधाभाग का (अपेक्षितमिविस्तार के लिये माप करे यह अर्थ न कर के 'अर्धमन्तर्वेदि अधं च बहिर्वेदि' इन दोनों शब्दों से लक्षणा द्वारा अपेक्षित देशविदेश का बोध माना जाता है। अतः उक्त वाक्य का यह अर्थ प्राप्त होता है कि-'( अपेक्षित विस्तार के लिये ) देशविदेश का माप करे।'
अथवा यह कहा जा सकता है कि 'यस्करोषि यदनासि यजुहोसि वक्षासि यत् । यत् तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मर्पणम् ॥' इस भगवद्गीता स्मति के अनुसार ईश्वर को अपित करने की वृद्धि से जो कर्म अनष्ठित किये जाते हैं उनसे अन्तःकरणशखिरूप फल की सिद्धि हो जाती है। अतः उक्त रीति से यह सिद्ध है कि कर्मों द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाने पर नित्यानित्य वस्तु के विवेकादि साधनचतुष्टय को मनुष्य मन करता है ।
[ नित्यानित्य विवेक-विराग शमादिषट्क-मुमुक्षा) नित्य-अनित्य विवेक का अर्थ है कि-'दृश्यमान सम्पूर्ण जगत् अनित्य है और सबका जो कोई अधिष्ठान-आधार है वह नित्य है'-इस प्रकार का निश्चय । इस निश्चय के प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य को विराग-वैराग्य को प्राप्ति होती है-जिसका अर्थ है चित्त की ऐसी अवस्था जिसमें इस लोक में प्राप्त होने वाले पुत्र-स्त्री-धन-धान्य आदि कर्मफलों की और परलोक में प्राप्त होने वाले दिव्य विषयों को इच्छा का उवय ही प्रतिबद्ध हो जाप । वैराग्य प्राप्ति के बाद शमादि षटकछह गुणों की प्राप्ति होती है, वे हैं-शम-बम-उपरति-तितिक्षा-समाधान और श्रद्धा। शम का अर्थ है अन्तःकरण का निग्रह प्रति अन्तःकरण द्वारा विषय-कषायों के चिन्तन का परित्याग । दमका अथ है-बाह्यन्द्रियों का निग्रह सांसारिक विषयों से इन्द्रियों को विमुख करना । उपरति का अर्थ है संन्यास अर्थात् विरति यानी हिसादि पापों के त्याग की प्रतिज्ञा जिससे यथोचित और परिपूर्ण रूप से विषयों से अन्तःकरण और इन्द्रियों को सर्वविध निवृत्ति हो । तितिक्षा का अर्थ है द्वन्द्व यानी सुखदुःख की सहिष्णुता-दुःख से कायर न होना और सुख से उन्मत्त न होना। समाधान का अर्थ है आत्मा के श्रवण आदि में अन्तःकरण का नियोजन । श्रद्धा का अर्थ है संप्रदाय, शास्त्र और प्राचार्य के वचन में विश्वास । उक्त तीनों साधन के प्राप्त हो जाने के बाद मुमुक्षा-मोक्षेच्छा होती है। यह साधन चतुष्टय श्रवणादि के अधिकारी का विशेषण होता है अर्थात् इन साधनों से सम्पन्न पुरुष ही वेदान्त से ब्रह्म के श्रवण और मननादि का अधिकारी होता है।
यसु-'मुमुक्षौवाधिकारिविशेषणम्, तस्या एव निरपेक्षाधिकारनिमितत्वात्' इति । तन्न, सामर्थ्यादेरप्यधिकारनिमित्तत्वात् । अथ कामनार्थिक सामर्थ्याधपेक्षते न श्रुतमन्यत् , तत् किं श्रुतलिङ्गयोलिङ्ग बलवत् ? । तस्माद् 'राजा राजसूयेन यजेत' इत्यादी राजत्वादेरिख श्रुतस्य विवेकादेरप्यधिकारिविशेषणत्वं युक्तम् । 'मुमुक्षायाः सार्वत्रिकत्वात्, त्यविवेकादीनां त्वेकैकशावापर्यालोचितानां सर्ववेदान्तप्रत्ययन्यायवाधितत्याद्न तथात्वमिति चेत् ? न, सर्ववेदान्तप्रत्यय