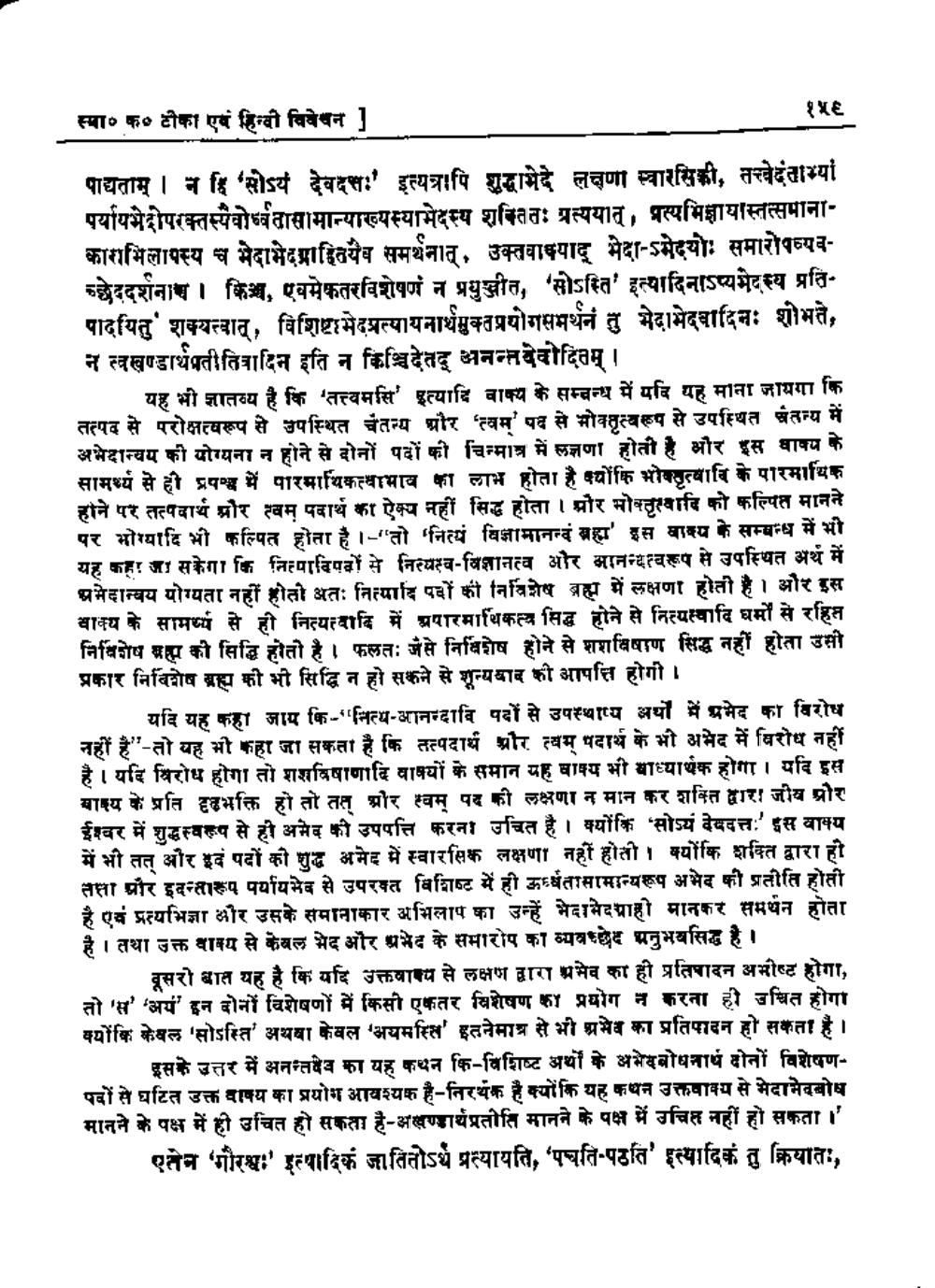________________
स्था क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ]
१५६
पाद्यताम् । न हि सोऽयं देवदतः' इत्यत्रापि शुद्धाभेदे लक्षणा स्वारसिकी, तत्त्वेदंताभ्यां पर्यायभेदोपरक्तस्यैवोलतासामान्याख्यस्याभेदस्य शक्तितः प्रत्ययात् , प्रत्यभिज्ञायास्तत्समानाकारामिलापस्य च भेदाभेदमाहितयैव समर्थनात् , उक्तवाफ्याद् भेदा-ऽमेदयोः समारोपव्यवच्छेददर्शनाच । किञ्च, एवमेकतरविशेषणं न प्रयुञ्जीत, 'सोऽस्ति' इत्यादिनाऽप्यभेदस्य प्रतिपादयितु शक्यत्वात् , विशिष्टाभेदप्रत्यायनार्थमुक्तप्रयोगसमर्थनं तु भेदाभेदवादिनः शोभते, न वखण्डार्थप्रतीतिवादिन इति न किश्चिदेतद् अनन्तदेवोदितम् ।।
यह भी ज्ञातव्य है कि 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्य के सम्बन्ध में यदि यह माना जायगा कि तत्पद से परोक्षत्वरूप से उपस्थित चैतन्य और 'त्वम' पद से मोक्तृत्वरूप से उपस्थित अंतन्य में अभेदान्वय की योग्यना न होने से दोनों पदों की चिन्मात्र में लक्षणा होती है और इस वाक्य के सामर्थ्य से ही प्रपश्व में पारमार्थिकत्वाभाव का लाभ होता है क्योंकि भोक्तृत्वारि के पारमार्थिक होने पर तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का ऐक्य नहीं सिद्ध होता । और मोक्तृत्वादि को कल्पित मानने पर भोग्यादि भी कल्पित होता है ।-"तो नित्यं विज्ञामानन्दं ब्रह्म' इस वाक्य के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकेगा कि नित्पाविपनों से नित्यत्व-विज्ञानत्व और मानन्द त्वरूप से उपस्थित अर्थ में अमेदान्बय योग्यता नहीं होती अतः नित्याटि पदों को विशेष ब्रह्म में लक्षणा होती है। और इस वाक्य के सामर्थ्य से ही नित्यत्वादि में अपारमार्थिकत्व सिद्ध होने से नित्यत्वादि धर्मों से रहित निविशेष ब्रह्म की सिद्धि होती है। फलतः जैसे निर्विशेष होने से शशविषाण सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार निविशेष ब्रह्म की भी सिद्धि न हो सकने से शून्यबाद की आपत्ति होगी।
यदि यह कहा जाय कि-नित्य-आनन्दादि पदों से उपस्थाप्य अर्यों में प्रभेद का विरोध नहीं है"-तो यह भी कहा जा सकता है कि तत्पदार्थ और त्वम् पदार्थ के भी अभेद में विरोध नहीं है । यदि विरोध होगा तो शशविषाणादि वाक्यों के समान यह वाक्य भी बाध्यार्थक होगा। यदि इस बाक्य के प्रति दृढभक्ति हो तो तत और स्वम पद की लक्षणा न मान कर शक्ति द्वारा जं ईश्वर में शुद्धस्वरूप से ही अमेव को उपपत्ति करना उचित है। क्योंकि 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्य में भी तत् और इदं पदों को शुद्ध अमेद में स्वारसिक लक्षणा नहीं होती। क्योंकि शक्ति द्वारा ही तप्ता और इदन्तारूप पर्यायमेव से उपरक्त विशिष्ट में ही कर्वतासामान्यरूप अभेद की प्रतीति होती है एवं प्रत्यभिज्ञा और उसके समानाकार अभिलाप का उन्हें भेदाभेदग्राही मानकर समर्थन होता है । तथा उक्त वाक्य से केवल भेद और अभेद के समारोप का व्यवच्छेद अनुभवसिद्ध है।
दूसरी बात यह है कि यदि उक्तवाश्य से लक्षण द्वारा प्रभेव का ही प्रतिपादन अमीष्ट होगा, तो 'स' 'अयं इन दोनों विशेषणों में किसी एकतर विशेषण का प्रयोग न करना ही उचित होगा क्योंकि केवल 'सोऽस्ति' अथवा केवल 'अयमस्ति' इतनेमात्र से भी अमेव का प्रतिपादन हो सकता है।
इसके उत्तर में अनन्तदेव का यह कथन कि-विशिष्ट अर्थों के अभेदबोधनार्थ दोनों विशेषणपदों से घटित उक्त वाक्य का प्रयोग आवश्यक है-निरर्थक है क्योंकि यह कथन उक्तवाक्य से मेदामेवबोष मानने के पक्ष में ही उचित हो सकता है-अखण्डार्थप्रतीति मानने के पक्ष में उचित नहीं हो सकता।'
एतेन 'गौरश्वः' इत्यादिकं जातितोऽथं प्रत्यायति, पचति-पठति' इत्यादिकं तु क्रियातः,