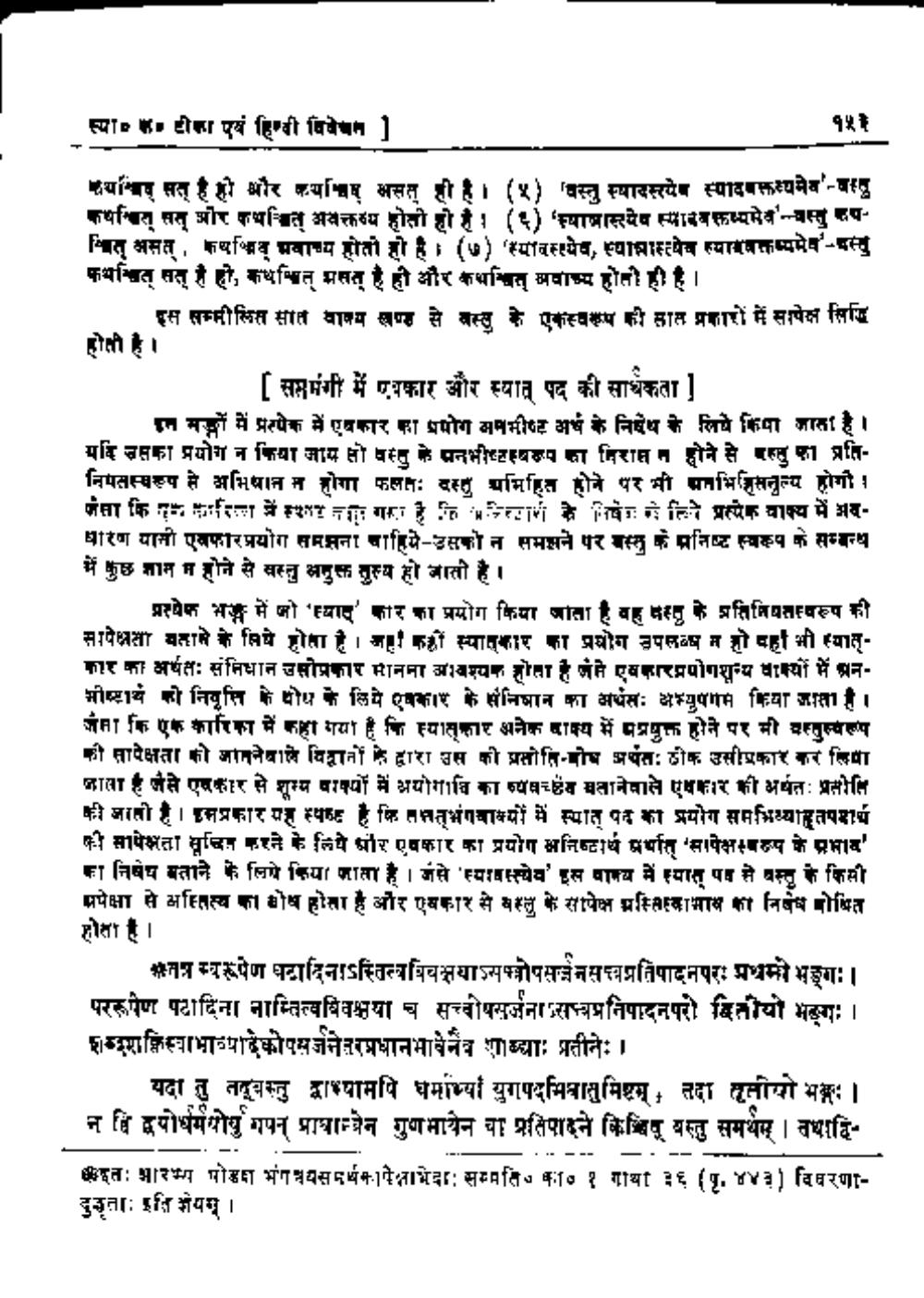________________
स्याटीका एवं हिन्दी विवेचन ]
१५॥
यांचा सत् है हो और कर्याचा असत् ही है। (५) 'वस्तु स्थावस्येव स्थाववतव्यमेव'-वस्तु कश्चित् सत् और कश्चित् अवक्तव्य होती ही है। (१) 'यात्रास्त्येव स्मारवक्तव्यमेवन्यस्तु उपबित् असत् , कश्चित् भवाच्य होती ही है। (७) स्यावस्त्येव, स्थानास्त्येव स्यावतम्यमेव-वस्तु कश्चित् तत् है हो, कथमित् मत्सत् है हो और कश्चित् अवाध्य होती ही है।
इस सम्मीलित सात वाक्य खण्ड से वस्तु के एकस्वरूप की सात प्रकारों में सापेक्ष सिद्धि होती है।
[ सप्तमंगी में प्रयकार और स्यात् पद की सार्थकता] इन मलों में प्ररपेक में एबकार का प्रयोग मममीष्ट अर्थ के निधेष के लिये किया जाता है। यदि उसका प्रयोग न किया जाय तो वस्तु के प्रनभीष्टापडपका निराप्त होने से बहतु का प्रतिनिपसास्वरूप से अभियान म होगा फलतः वस्तु अभिहित होने पर भी मतभिहसनुल्य होगी। अंसा कि मामला नगरा है कि मार्ग के नियमे लिये प्रत्येक वाक्य में अवधारण यानी एवफार प्रयोग समझना चाहिये-उसको न समझने पर वस्तु के प्रनिष्ट स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ शान न होने से वस्तु अनुक्त तुल्य हो जाती है।
प्रत्येक अङ्ग में जो 'यार' कार का प्रयोग किया जाता है वहस्तके प्रतिनियतस्वरूप की सापेक्षता बताने के लिये होता है। ना! कहाँ स्यातकार का प्रयोग उपलबब न हो वहाँ भी स्यातकार का अर्थतः संनिधान जसीप्रकार मानमा आवश्यक होता है जो एषकारप्रपोगशून्य वाक्यों में प्रानभीष्टार्थ को नियुक्ति के घोष के लिये एक्कार के निधान का अर्थसः अभ्युपगम किया जाता है। जमा कि एक कारिका में कहा गया है कि त्यातकार अनेक वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी यहतुस्वरूप की सापेक्षता को जागनेवाले विद्वानों के द्वारा अप्स को प्रसोति-बोध अर्थत: ठीक उसीप्रकार कर लिया जाता है जैसे एक्कार से शूम्म परक्यों में अयोगाधि का व्य य बतानेवाले एपकार की अर्थतः प्रसोति की जाती है। इमप्रकार यह स्पष्ट है कि तमतभंगवाक्पों में स्यात् पद का प्रयोग समभिव्याहतपार्य की सापेक्षता सूचित करने के लिये और एपकार का प्रयोग अनिष्टार्थ अर्थात् 'सापेक्षस्वरूप के प्रभाव' का निषेध बताने के लिये किया जाता है। जैसे 'स्याबस्स्येव' इस वामय में स्यात् पा से वस्तु के किसी प्रपेक्षा से अस्तित्व का कोष होता है और एक्कार से वस्तु के सापेक्ष मस्सिावाभाष का निषेध मोषित होता है।
मन्त्र स्वरूपेण घटादिनाऽस्तित्वविचक्षयाश्यत्रोपसर्जनसायप्रतिपादनपरः प्रथमो भगः । पररूपेण पटादिना नास्तित्वविवक्षया च सत्त्वोपसर्जना सम्वनिपादनपरो द्वितीयो भङ्गः । शम्दशक्तिस्वाभाव्यादेकोपसर्जनेतरप्रधानभावेनैव शाब्याः प्रतीनेः ।
यदा तु तद्वस्तु द्वाभ्यामपि धमाभ्यां युगपदमिवामिष्टम् । तदा तृतीयो भङ्गः । न विद्वयोधमयोयुगपन प्राधान्न गुणमायेन चा प्रतिपादने किश्चिवू यस्तु समर्थम् । तथाहि
इतः भारभ्य पोडमा भंगत्रयसमर्थनापेक्षाभेदा: सम्मति का० १ गाथा ३६ (पृ. ४४३) विधरणादुताः इति शेयम् ।