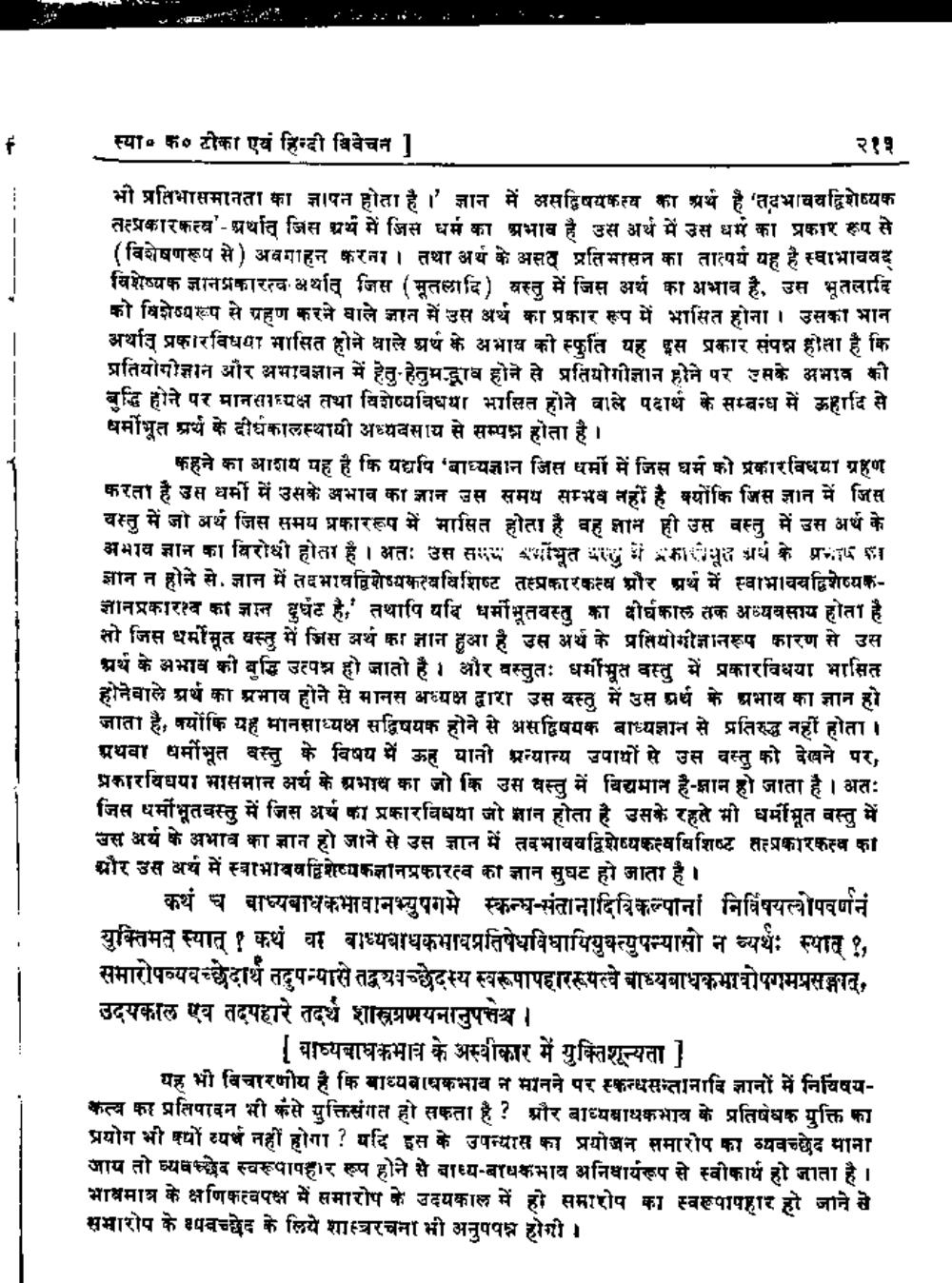________________
__ स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ]
भी प्रतिभासमानता का ज्ञापन होता है।' ज्ञान में असद्विषयकस्य का अर्थ है 'तदभावद्विशेष्यक तत्प्रकारकत्व'- अर्थात जिस प्रर्य में जिस धर्म का प्रभाव है उस अर्थ में उस धर्म का प्रकार रूप से (विशेषणरूप से) अवगाहन करना। तथा अर्थ के असद प्रतिमासन का तात्पर्य यह है स्वाभाववाद विशेष्यक ज्ञानप्रकारत्व अर्थात् जिस (मूतलादि) वस्तु में जिस अर्थ का अभाव है, उस भूतलादि को विशेष्य रूप से ग्रहण करने वाले ज्ञान में उस अर्थ का प्रकार रूप में भासित होना। उसका भान अर्थात प्रकारविधया मासित होने वाले अर्थ के अभाव को स्फुति यह इस प्रकार संपन्न होता है कि प्रतियोगीज्ञान और अमावज्ञान में देत-तम.दाव होने से प्रतियोगीज्ञान होने पर उसके बुद्धि होने पर मानसाध्यक्ष तथा विशेष्यविधया भासित होने वाले पदार्थ के सम्बन्ध में जहादि से धर्मीभूत अर्थ के दीर्घकालस्थायी अध्यवसाय से सम्पन्न होता है।
कहने का आशय यह है कि यद्यपि 'बाध्यज्ञान जिस धर्मों में जिस धर्म को प्रकारविधया ग्रहण करता है उस धर्मी में उसके अभाव का ज्ञान उस समय सम्भव नहीं है क्योंकि जिस ज्ञान में जिस वस्तु में जो अर्थ जिस समय प्रकाररूप में मासित होता है वह शाम ही उस वस्तु में उस अर्थ के अभाव ज्ञान का विरोधी होता है । अतः उस समय गाभुत याद में कारोभूत अर्थ के प्राम ज्ञान न होने से. ज्ञान में तदभावविशेष्यकरयविशिष्ट तत्प्रकारकत्व और अर्थ में स्वाभावयद्विशेष्यकज्ञानप्रकारश्व का ज्ञान दुर्घट है, तथापि यदि धर्माभूतवस्तु का दीर्घकाल तक अव्यवसाय होता है सो जिस धर्मो मूत वस्तु में जिस अर्थ का ज्ञान हुआ है उस अर्थ के प्रतियोगीजानरूप कारण से उस अर्थ के अभाव की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और वस्तुतः धर्मीभूत वस्तु में प्रकारविधया भासित होनेवाले अर्थ का प्रभाव होने से मानस अध्यक्ष द्वारा उस वस्त में उस प्रर्थ के प्रभाव का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह मानसाध्यक्ष सद्विषयक होने से असद्विषयक बाध्यज्ञान से प्रतिरुद्ध नहीं होता। प्रथवा धर्मोभूत वस्तु के विषय में ऊह यानी अन्यान्य उपायों से उस वस्तु को देखने पर, प्रकारविषय या भासमान अर्थ के प्रभाव का जो कि उस वस्त में विद्यमान है-ज्ञान हो जाता है। अतः जिस धर्मीभूतवस्तु में जिस अर्थ का प्रकार विधया जो ज्ञान होता है उसके रहते भी धर्मीभूत वस्तु में उस अर्य के अभाव का ज्ञान हो जाने से उस ज्ञान में तवभाववद्विशेष्यकत्वविशिष्ट तत्प्रकारकस्व का और उस अर्थ में स्वाभाववद्विशेष्यकज्ञानप्रकारत्व का ज्ञान सुघट हो जाता है।
कथं च बाध्यबाधकभावानभ्युपगमे स्कन्ध-संतानादिविकल्पाना निर्विषयत्वोपवर्णनं युक्तिमत स्यात् ? कथं वा बाध्यबाधकमावप्रतिषेधविधायियुक्त्युपन्यासो न व्यर्थः स्यात् ?, समारोपव्यवच्छेदार्थ तदुपन्यासे तद्ववच्छेदस्य स्वरूपापहाररूपत्वे बाध्यबाधकमावोपगमप्रसङ्गाव, उदयकाल एव तदपहारे तदर्थ शास्त्रप्रणयनानुपतेश्च ।
[पाध्यबाधकमात्र के अस्वीकार में युक्तिशून्यता] यह भी विचारणीय है कि बाध्यबाधकभाव न मानने पर स्कन्धसन्तानावि ज्ञानों में निविषयकत्व का प्रतिपावन भी कसे युक्तिसंगत हो सकता है ? और बाध्यबाधकभाव के प्रतिषेधक युक्ति का प्रयोग भी क्यों व्यर्थ नहीं होगा? यदि इस के उपन्यास का प्रयोजन समारोप का व्यवच्छेद माना जाय तो ध्यवच्छेव स्वरूपापहार रूप होने से बाध्य-बाधकभाव अनिवार्यरूप से स्वीकार्य हो जाता है। भावमात्र के क्षणिकरवपक्ष में समारोप के उदयकाल में हो समारोप का स्वरूपापहार हो जाने से समारोप के पवच्छेद के लिये शास्त्ररचना भी अनुपपन्न होगी।