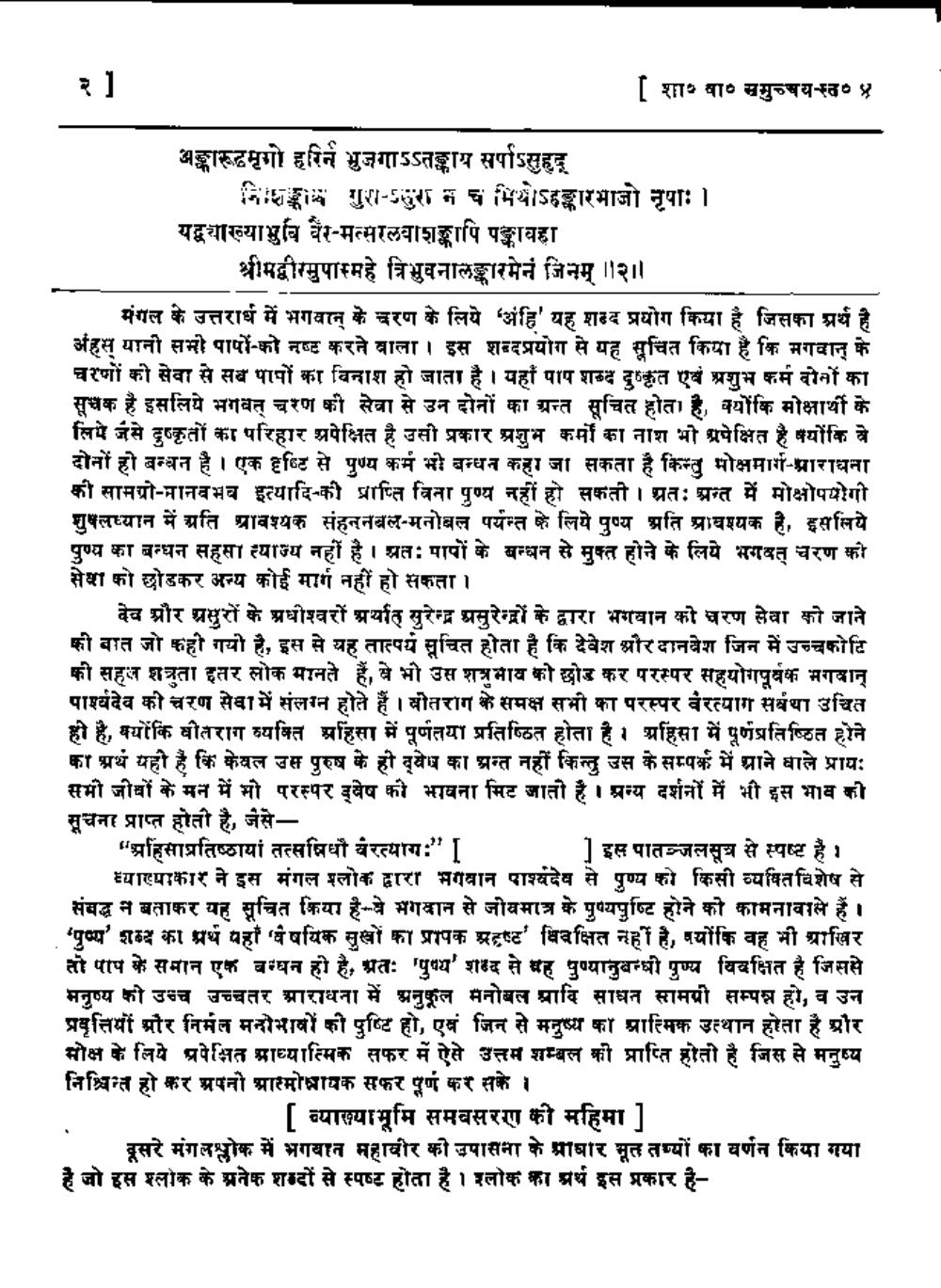________________
[ शा वा० समुच्चय-स्त०५
अङ्कारूढमृगो हरिनं भुजगाऽऽतङ्काय साऽसुहृद्
निशा गुरा-तुरा न च भियोऽहङ्कारभाजो नृपाः । यद्वयाख्याभुवि वैर-मत्सरलबाशङ्कापि पङ्कावहा
श्रीमद्वीरमुपास्महे त्रिभुवनालङ्कारमेनं जिनम् ।।२।। मंगल के उत्तरार्ध में भगवान के चरण के लिये 'हि' यह शब्द प्रयोग किया है जिसका अर्थ है अहस यानी समो पापों को नष्ट करने वाला। इस शब्दप्रयोग से यह सूचित किया है कि मगवान् के चरणों को सेवा से सब पापों का विनाश हो जाता है। यहाँ पाप शब्द दुष्कृत एवं अशुभ कर्म दोनों का सूचक है इसलिये भगवत् चरण की सेवा से उन दोनों का ग्रन्त सूचित होता है, क्योंकि मोक्षार्थी के लिये जसे दुष्कृतों का परिहार अपेक्षित है उसी प्रकार प्रशुभ कर्मों का नाश भो अपेक्षित है क्योंकि वे दोनों हो बन्धन है । एक दृष्टि से पुण्य कर्म भो बन्धन कहा जा सकता है किन्तु मोक्षमार्ग-प्राराधना की सामग्रो-मानवभव इत्यादि की प्राप्ति विना पुण्य नहीं हो सकती । प्रतः अन्त में मोक्षोपयोगी शुषलध्यान में अति प्रावश्यक संहननबल-मनोबल पर्यन्त के लिये पुण्य अति प्रावश्यक है, इसलिये पुण्य का बन्धन सहसा त्याज्य नहीं है । अत: पापों के बन्धन से मुक्त होने के लिये भगवत् चरण को सेश को छोडकर अन्य कोई मार्ग नहीं हो सकता।
देव और असुरों के अधीश्वरों अर्थात् सुरेन्द्र प्रसुरेन्द्रों के द्वारा भगवान को चरण सेवा को जाने की बात जो कही गयी है, इस से यह तात्पर्य सचित होता है कि देवेश और दानवेश जिन में उच्चकोटि की सहल शत्रुता इतर लोक मानते हैं, वे भी उस शत्रुभाव को छोड कर परस्पर सहयोगपूर्वक भगवान् पार्श्वदेव की चरण सेवा में संलग्न होते हैं । वीतराग के समक्ष सभी का परस्पर वैरत्याग सर्वथा उचित ही है, क्योंकि वीतराग व्यक्ति अहिंसा में पूर्णतया प्रतिष्ठित होता है। अहिंसा में पूर्णप्रतिष्ठित होने का अर्थ यही है कि केवल उस पुरुष के हो वेष का अन्त नहीं किन्तु उस के सम्पर्क में प्राने धाले प्रायः सभी जीवों के मन में भी परस्पर वेष को भावना मिट जाती है । अन्य दर्शनों में भी इस भाव की सूचना प्राप्त होती है, जैसे
"अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग:"[ ] इस पातञ्जलसूत्र से स्पष्ट है। ध्यापाकार ने इस मंगल श्लोक द्वारा भगवान पाश्चंदेव से पुण्य को किसी व्यक्तिविशेष से संबद्ध न बताकर यह सूचित किया है वे भगवान से जीवमात्र के पुण्यपुष्टि होने को कामनावाले हैं। 'पुण्य' शब्द का अर्थ यहाँ 'वैषयिक सुखों का प्रापक प्रदृष्ट' विवक्षित नहीं है, क्योंकि वह भी अाखिर तो पाप के समान एक बन्धन ही है, अतः 'पुण्य' शब्द से यह पुण्यानुबन्धी पुण्य विवक्षित है जिससे मनुष्य को उच्च उच्चतर आराधना में अनुकूल मनोबल प्रादि साधन सामग्री सम्पन्न हो, व उन प्रवृत्तियों और निर्मल मनोभावों की पुष्टि हो, एवं जिन से मनुष्य का प्रात्मिक उत्थान होता है और मोक्ष के लिये अपेक्षित प्राध्यात्मिक सफर में ऐसे उत्तम शम्बल की प्राप्ति होती है जिस से मनुष्य निश्चिन्त हो कर अपनी प्रारमोन्नायक सफर पूर्ण कर सके।
[ व्याख्याभूमि समवसरण की महिमा ] दूसरे मंगलश्लोक में भगवान महावीर की उपासना के प्राधार भूत तग्यों का वर्णन किया गया है जो इस श्लोक के अनेक शब्दों से स्पष्ट होता है । श्लोक का अर्थ इस प्रकार है