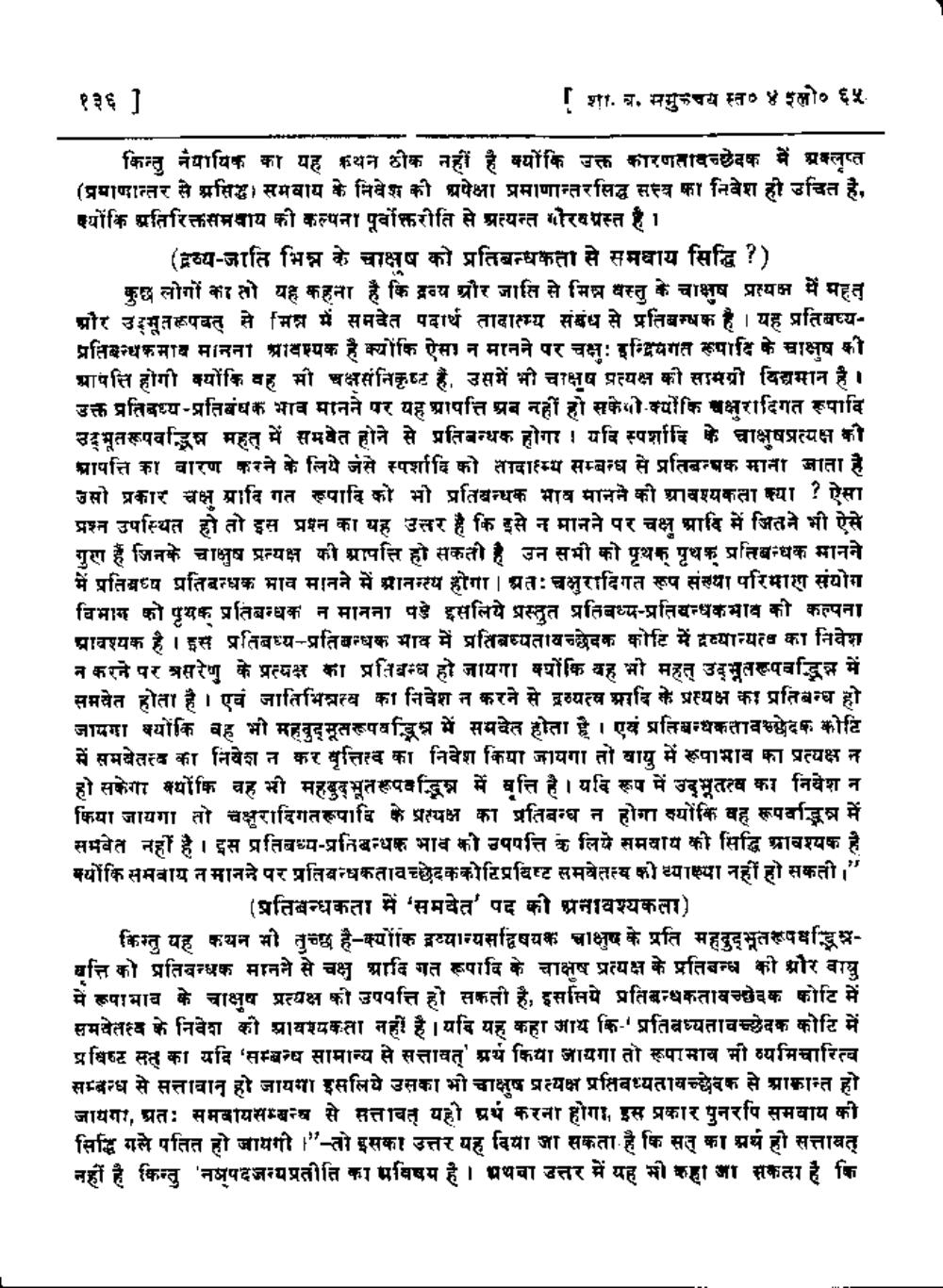________________
१३६ ]
[ शा. व. ममुरचय स्त०४ श्लो० ६५
किन्तु नैयायिक का यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि उक्त कारणतावच्छेदक में प्रक्लुप्त (प्रमाणान्तर से प्रसिद्ध समवाय के निवेश की अपेक्षा प्रमाणान्तरसिद्ध सत्त्व का निवेश ही उचित है, क्योंकि अतिरिक्तसमवाय की कल्पना पूर्वोत्तरीति से अत्यन्त गौरव ग्रस्त है।
(द्रव्य-जाति भिन्न के चाक्षष को प्रतिबन्धकता से समवाय सिद्धि ?) कुछ लोगों का तो यह कहना है कि द्रव्य और जाति से मिन्न वस्तु के चाक्षुष प्रत्यक्ष में महत और उमृतरूपवत् से मिन्न में समवेत पदार्थ तादात्म्य संबंध से प्रतिबन्धक है । यह प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमाव मानना आवश्यक है क्योंकि ऐसा न मानने पर चक्षुः इन्द्रियगत रूपादि के साक्षुष की आपत्ति होगी क्योंकि वह भी वक्षसंनिकृष्ट है, उसमें भी चाक्षष प्रत्यक्ष को सामग्री विद्यमान है। उक्त प्रतिबध्य-प्रतिबंधक भाव मानने पर यह प्रापत्ति प्रब नहीं हो सकेगी क्योंकि अक्षुरादिगत रूपादि उद्भूतरूपनि महत् में समवेत होने से प्रतिबन्धक होगा । यदि स्पर्शादि के चाक्षुषप्रत्यक्ष की प्रापत्ति का वारण करने के लिये जैसे स्पर्शादि को तावात्म्य सम्बन्ध से प्रतिबन्धक माना जाता है उसो प्रकार चक्षु प्रादि गत रूपादि को भी प्रतिबन्धक भाव मानने की अावश्यकता क्या ? ऐसा प्रश्न उपस्थित हो तो इस प्रश्न का यह उत्तर है कि इसे न मानने पर चक्षु आदि में जितने भी ऐसे गुरग हैं जिनके चाक्षुष प्रत्यक्ष की प्रापत्ति हो सकती है उन सभी को पृथक पृथक प्रतिबन्धक मानने में प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव मानने में प्रानन्स्य होगा | अतः चक्षुरादिगत रूप संस्था परिमाण संयोग विभाग को पृथक प्रतिबन्धक न मानना पड़े इसलिये प्रस्तुत प्रतिबध्य-प्रतिवन्धकमाव की का प्रावश्य स प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक भाव में प्रतिबध्यतावच्छेदक कोटि में ध्यान्यत्व का निवेश न करने पर सरेणु के प्रत्यक्ष का प्रतिबन्ध हो जायगा क्योंकि यह भी महत् उद्भूतरूपद्भिन्न में समवेत होता है। एवं जातिभिन्नत्व का निवेश न करने से व्यत्व प्रादि के प्रत्यक्ष का प्रतिबन्ध हो जायगा क्योंकि वह भी महमूतरूपनिन में समवेत होता है । एवं प्रतिबन्धकतावच्छेदक कोटि में समवेतत्व का निवेश न कर वृत्तिस्व का निवेश किया जायगा तो वायु में रूपामाव का प्रत्यक्ष न हो सकेगा क्योंकि वह भी महबुभूतरूपद्भिन्न में वृत्ति है । यदि रूप में उद्भूतत्व का निवेश न किया जायगा तो चक्षुरादिगतरूपादि के प्रत्यक्ष का प्रतिबन्ध न होगा क्योंकि वह रूपनि में समवेत नहीं है । इस प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक भाव को उपपत्ति के लिये समवाय की सिद्धि प्रावश्यक है क्योंकि समवाय न मानने पर प्रतिबन्धकतावच्छेदककोटिप्रविष्ट समवेतत्व को ध्याख्या नहीं हो सकती।"
(प्रतिबन्धकता में 'समवेत' पद की अनावश्यकता) किन्तु यह कथन मी तुच्छ है-क्योंकि द्रव्यान्यसद्विषयक चाक्षुष के प्रति महदुइभ्रतरूपद्भिश्नपत्ति को प्रतिबन्धक मानने से चक्षु प्रावि गत रूपावि के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रतिबन्ध की और वायु में रूपामाव के चाक्षुष प्रत्यक्ष की उपपत्ति हो सकती है, इसलिये प्रतिबन्धकतावच्छेदक कोटि में समवेतत्व के निवेश को प्रायश्यकता नहीं है । यदि यह कहा आय कि-'प्रतिबध्यतावच्छेदक कोटि में प्रविष्ट सत् का यदि सम्बन्ध सामान्य से सत्तावत्' प्रर्य किया जायगा तो रूपामाव भी व्यमिचारित्व सम्बन्ध से सत्तावान हो जायगा इसलिये उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रतिबध्यतावच्छेवक से प्राकान्त हो जायगा, प्रतः समवायसम्बन्ध से सत्तावत् यही प्रथं करना होगा, इस प्रकार पुनरपि समवाय की सिद्धि गले पतित हो जायगी।"-तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि सत् का अर्थ हो सत्तावत् नहीं है किन्तु 'नपदजन्यप्रतीति का विषय है । अथवा उत्तर में यह भी कहा जा सकता है कि