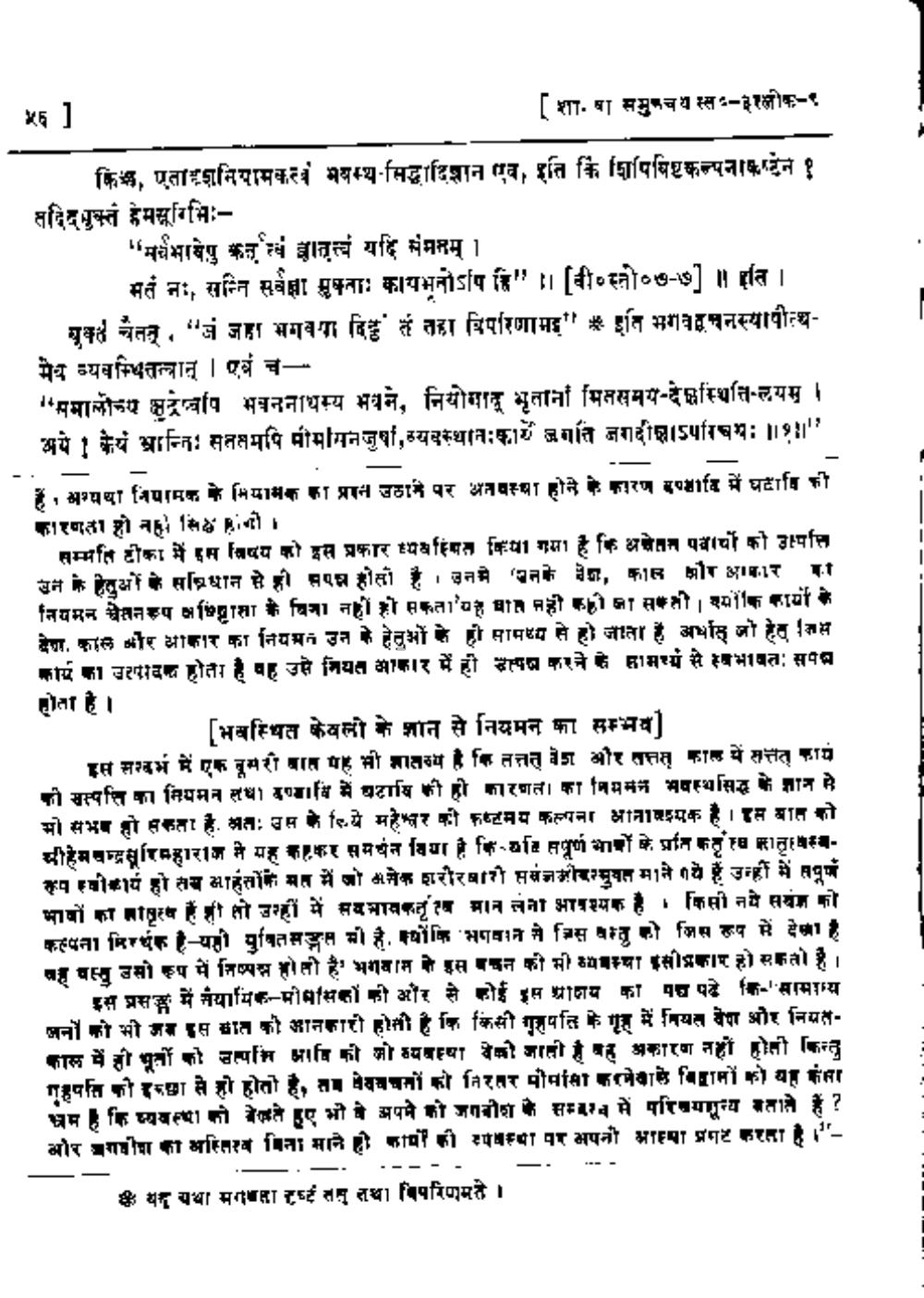________________
५६ ]
[ शा. पा समुच य स:-३श्लोक-
किश, एताशनियामकत्वं मयस्थ-सिद्धादिज्ञान एव, इति कि शिपिविष्टकल्पनाकादेन ? सविदयुक्त हेमगिभिः
"मभाषेषु अन्य बातृत्त्वं यदि मनम् ।
मतं नः, सन्नि सर्वशा मुफ्नाः कापभनोऽपि हि" ।। [वी०स्तो०७-७] ॥ इति । युक्त चैतत् . "जहा भगवा दिड तंतहा रिपरिणाम" * इति भगवतमानस्यापीत्थमेय व्यवस्थितन्त्रान् । एवं च-- "समालोच्य क्षुद्रपि भवननाथम्य भवने, नियोगानु भृताना मिससमय-देशस्थिति-लयम् । अये ! केयं भ्रान्तिः सतप्तमपि मीमामन जुषा, व्यवस्थानःकार्य जगांत जगदीशाऽपरिचयः ॥१॥" हैं । अन्यथा नियामक के मियामक का प्रान उठाने पर अवस्था होने के कारण सावि में घाव की कारणता हो नहीं मिली।
सम्मति टीका में इस विषय को इस प्रकार यवस्मित किया गया है कि अचेतन पदार्थो को उत्पत्ति उन हितुओं के सविधान से ही सपन्न होता है। उनमें 'चनके देश, काल और आकार का नियमन वेतनरूप आvिgासा के बिना नहीं हो सकता यह बात नही कहीमा सती । मौक कार्यो के देश, काल और आकार का नियम उन के हेतुभों के ही सामध्य से हो जाता है अर्थात् जो हेतु जिस कार्य का उत्पादक होता है वह उसे नियत आकार में ही उत्पन्न करने के मामध्यं से स्वभावतः सपना होता है।
[भवस्थित केवली के शान से नियमन का सम्भव) इस सम्वर्भ में एक दूसरी बात यह भी मातग्य है कि तत्तत् का और तत्तत् काल में सत्तत् कार्य की सत्पत्ति का नियमन तथा दण्डाधि में पदाधि की ही कारणता का मिममन भवस्थसिद्ध के कान में मो सभव हो सकता है. अत: उप्त के लिये महेश्वर की कष्टमय कल्पना आनावश्यक है। इस बात को मोहेमचन्द्र प्रतिमहाराज ने यह कहकर समधन विण है कि-यदि तपूर्ण भागों के प्रति कतच मातृवस्थ. रूप स्वीकार्य हो सब माहंसों कीमत में जो ममेक शरीरधारी सम्रजमोवस्मयात माने गये हैं उन्हीं में सपूर्ण भावों का विस्व हैशी तो उन्हीं में सबभावकत्व मान लेना आवश्यक है। किसी नये सद्या को कल्पना निरर्थक है-यही मुक्तिसङ्गत भी है. क्योंकि भगवान ने जिस वस्तु को जिस रूप में देना है वह वस्तु उसी रूप में निष्पन्न होती है। भगवान के इस बयान की मी व्यवस्था इसीप्रकार हो सकता है।
इस प्रसङ्ग में यायिक-मीमांसकों की और से कोई इस प्राशय का पत्र पढे कि-'सामान्य जनों को भी जब इस बात को आनकारी होती है कि किसी गृहपति के गृह में मियत वेषा और नियतकाल में ही भूतों को उत्पति आदि को को व्यवस्था की जाती है वह अकारण नहीं होती किन्तु महपति कोइरछा से ही होता है, ता देववचनों को निरसर पीमांसा करनेवाले विधामों को या सा भ्रम है कि व्यवस्था को बेलते इए भी वे अपने को जगवीश के सम्मान में परिणयानन्य बताते हैं? और बगीचा का अस्तित्व बिना माने ही कार्यों की स्पवया पर अपनी भाषा प्रगट करता है।"
* यार यथा मगवहारष्ट्र सम तथा विपरिणामते।