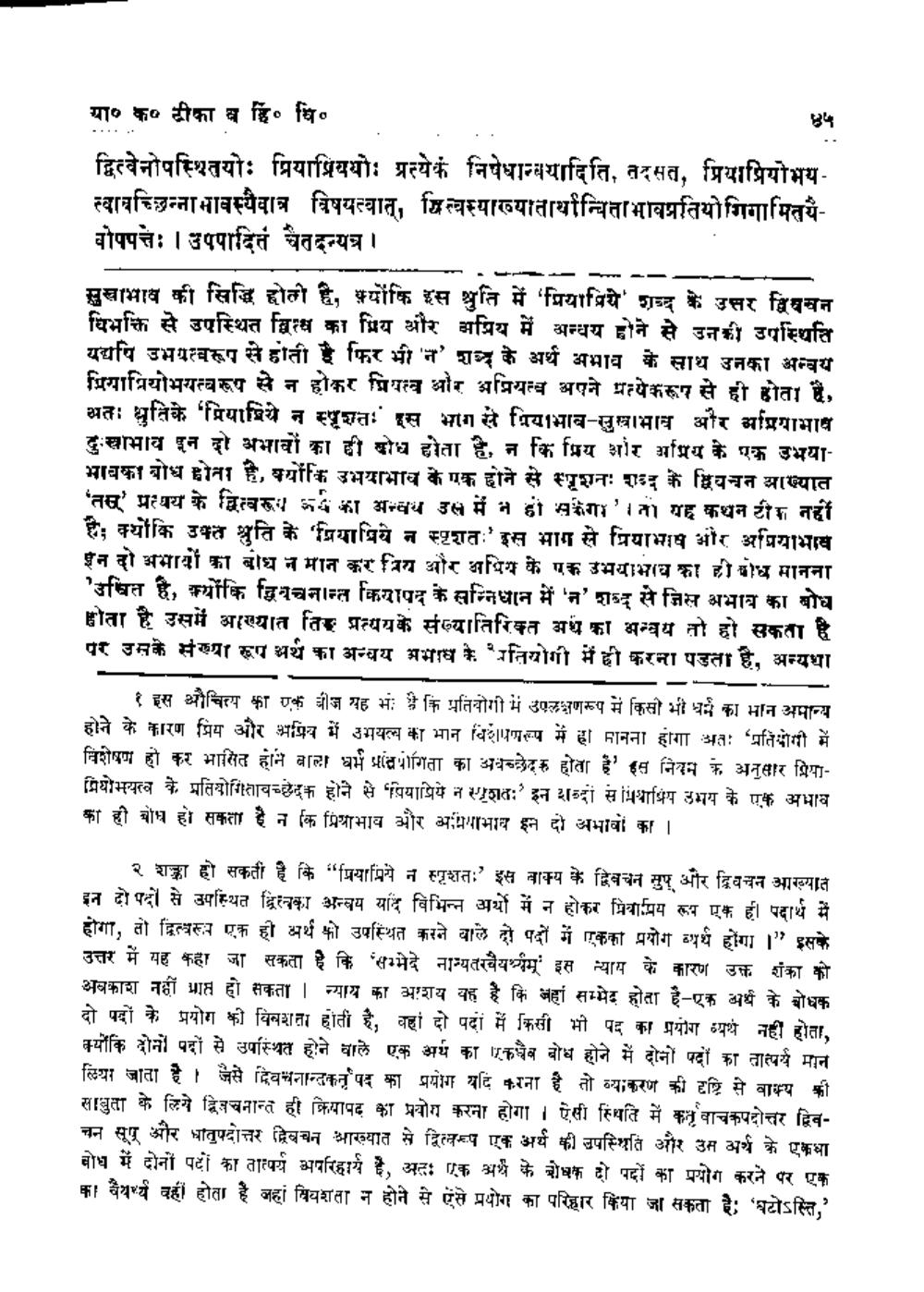________________
या० का टीका व हिं० वि० द्वित्वेनोपस्थितयोः प्रियाप्रिययोः प्रत्येकं निषेधान्बयादिति, तदसत, प्रियाप्रियोभयस्वावच्छिन्नामावस्यैवात्र विषयत्वात्, हित्वस्याख्यातार्यान्विताभावप्रतियोगिगामितयवोपपत्तः । उपपादित चैतदन्यत्र ।।
सुखाभाव की सिद्धि होती है, क्योंकि इस श्रुति में 'प्रियाप्रिये' शब्द के उत्तर द्विवचन विभक्ति से उपस्थित विश्व का प्रिय और अप्रिय में अन्धय होने से उनकी उपस्थिति यद्यपि उभयत्वरूप से होती है फिर भी 'न' शब्द के अर्थ अभाव के साथ उनका अन्वय प्रियाप्रियोभयत्व रूप से न होकर नियत्व और अप्रियत्व अपने प्रत्येकरूप से ही होता है, अतः धुतिके 'प्रियाप्रिये न स्पृशतः इस भाग से दियाभाव-मुखाभाव और प्रियाभाव दुःखाभाव इन दो अभावों का ही बोध होता है, न कि प्रिय और अप्रिय के एक उभयाभावका बोध होता है, क्योंकि उभयाभाव के एक होने से स्पृशनः शब्द के द्विवचन आख्यात 'तस्' प्रत्यय के विस्वरूप भई का अन्वय उल में न हो सकेगा।ना यह कथन टीक नहीं है; क्योंकि उक्त श्रुति के "प्रियाप्रिये न स्पृशतः' इस भाग से प्रियाभाष और अप्रियाभाव इन दो अमायों का बोध न मान कर त्रिय और अपिय के एक उभयाभाव का ही बोध मानना 'उधित है, क्योंकि द्विवचनान्त कियापद के सन्निधान में 'न' शब्द से जिस अभाव का बोध होता है उसमें आख्यात तिा प्रत्यय के संख्यातिरिक्त अर्थ का अन्वय तो हो सकता है पर उसके संख्या रूप अर्थ का अन्वय अभाव के प्रतियोगी में ही करना पड़ता है, अन्यथा
इस औचित्य का एक बीज यह भ है कि प्रतियोगी में उपलक्षणरूप में किसी भी धर्म का भान अमान्य होने के कारण प्रिय और अप्रिय में उपयल्य का भान विशेषणरूप में हा मानना होगा अतः 'प्रतियोगी में विशेषण हो कर भासित होने वाला धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है' इस निगम के अनुसार प्रियामियोभन्यत्व के प्रतियोगितावच्छेदक होने से पियाप्रिये नस्पृशतः' इन शब्दों से विधायि उभय के एक अभाव का ही बोध हो सकता है न कि प्रियाभाव और अमियाभाव इन दो अभावों का ।
२ शक्का हो सकती है कि “प्रियाप्रिये न स्पृशतः' इस वाक्य के द्विवचन सुए और द्विवचन आख्यात इन दो पदो से उपस्थित द्विलका अन्वय यदि विभिन्न अर्थो में न होकर प्रियाप्रिय रूप एक ह। पदार्थ में होगा, तो द्वित्वरूप एक ही अर्थ को उपस्थित करने वाले दो पदों में एकका प्रयोग व्यर्थ होगा ।" इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सम्भेदे नान्यतरवैयर्थ्यम् इस न्याय के कारण उक्त शंका को अवकाश नहीं प्राप्त हो सकता । न्याय का अाशय यह है कि जहां सम्मेद होता है-एक अर्थ के बोधक दो पदों के प्रयोग की विवशता होती है, वहां दो पदों में किसी भी पद का प्रयोग व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि दोनों पदों से उपस्थित होने वाले एक अर्थ का एकचैव बोध होने में दोनों पदों का तात्पर्य मान लिया जाता है। जैसे द्विवचनान्तक पद का प्रयोग यदि करना है तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य की साबुता के लिये द्विवचनान्त ही क्रियापद का प्रयोग करना होगा । ऐसी स्थिति में कतृ वाचकपदोत्तर द्विवचन सूपू और धातुपदोत्तर द्विवचन आख्यात से द्वित्वम्प एक अर्थ की उपस्थिति और उम अर्थ के एकमा बोध में दोनों पदों का तात्पर्य अपरिहार्य है, अतः एक अर्थ के बोधक दो पदों का प्रयोग करने पर एक का वैवयं वहीं होता है जहां विवशता न होने से ऐसे प्रयोग का परिहार किया जा सकता है; 'घटोऽस्ति,'