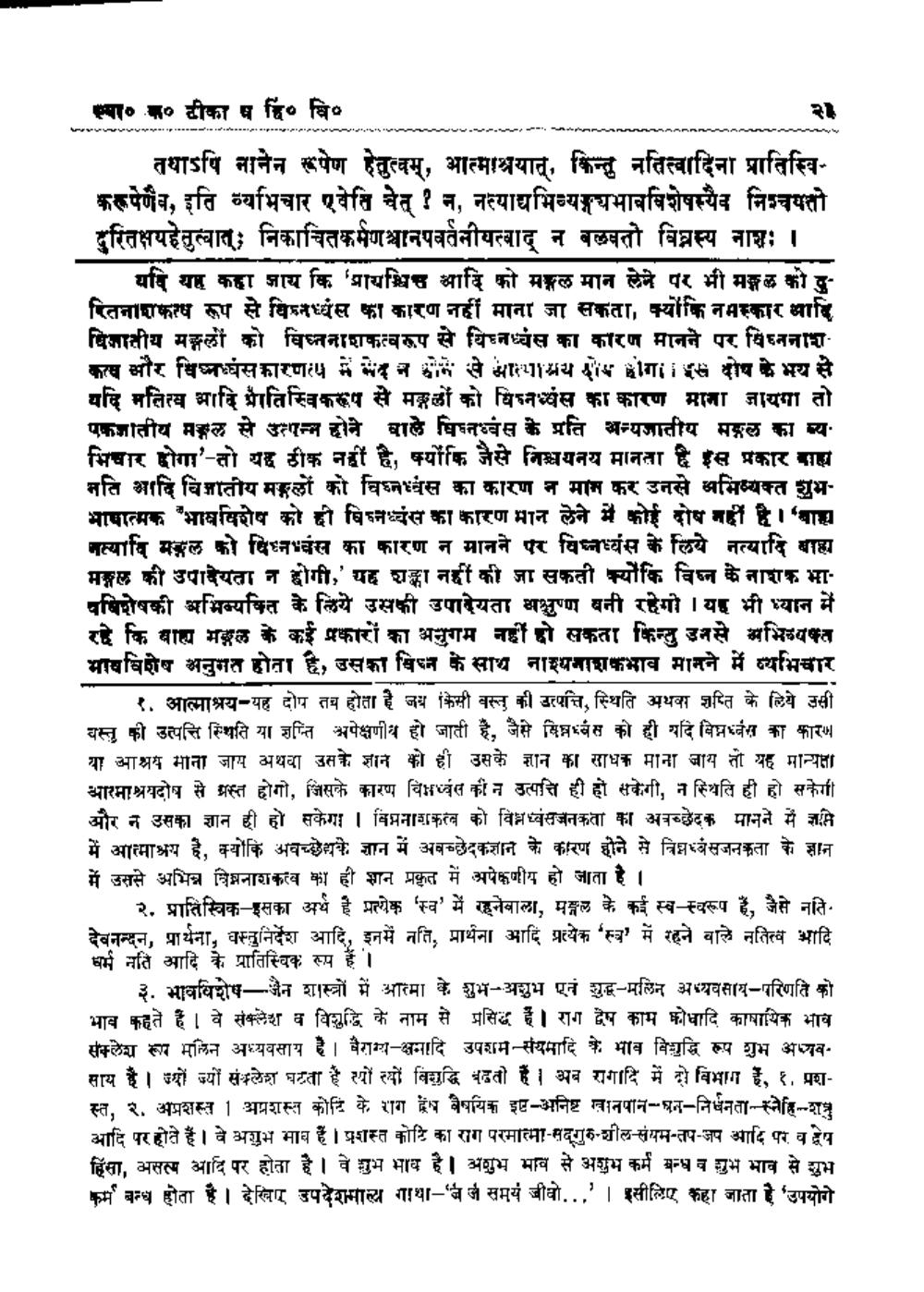________________
स्वा० स० टीका प हिं० वि०
__ तथाऽपि नानेन रूपेण हेतुत्वम्, आत्माश्रयान्, किन्तु नतित्वादिना प्रातिस्विकरूपेणैव, इति व्यभिचार एवेति चेत् ? न, नत्याघभिव्ययभावविशेषस्यैव निश्चयतो दुरितक्षयहेतुत्वात् निकाचितकर्मणश्वानपवर्तनीयत्वाद् न बलवतो विघ्नस्य नाशः ।।
यदि यह कहा जाय कि 'प्रायश्चित्त आदि को मङ्गल मान लेने पर भी माल को दु. रितनाशकाष रूप से विनध्धंस का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि नमस्कार आदि विजातीय मङ्गलों को विघ्ननाशकत्वरूप से विघ्नध्वंस का कारण मानने पर विघ्ननाश करव और विघ्नध्वंसकारणस्य मेदन में से आत्मानयोगास दोष के भय से यदि मतित्व आदि प्रातिस्विकरूप से मङ्गलों को विश्नध्वंस का कारण माना जायगा तो पकजातीय मङ्गल से उत्पन्न होने वाले विनध्वंस के प्रति अन्यजातीय महल का व्य. भिचार होगा'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे निश्चयनय मानता है इस प्रकार बाह्य मति आदि विजातीय मङ्गलों को चिनिध्वस का कारण न मान कर उनसे अभिव्यक्त शुभभाषात्मक भावविशेष को ही विनध्वंस का कारण मान लेने में कोई दोष नहीं है। बाह्य मस्यावि मङ्गल को विनवंस का कारण न मानने पर विघ्नध्यंस के लिये नत्यादि बाह्य मजल की उपादेयता न होगी, यह शङ्का नहीं की जा सकती क्योंकि विघ्न के नाशक भा. पषिशेषकी अभिव्यक्ति के लिये उसकी उपादेयता अक्षुण्ण बनी रहेगी । यह भी ध्यान में रहे कि बाय मङ्गल के कई प्रकारों का अनुगम नहीं हो सकता किन्तु उनसे अभिव्यक्त भावविशेष अनुगत होता है, उसका विधन के साथ नाश्यनाशकभाव मानने में व्यभिचार
१. आत्माश्रय-यह दोप तब होता है जब किसी वस्तु की उत्पत्ति, स्थिति अथका ज्ञप्ति के लिये उसी वस्तु की उत्पत्ति स्थिति या जप्ति अपेक्षणीय हो जाती है, जैसे विघ्नध्वंस को ही यदि विघ्नवस का कारण या आश्रय माना जाय अथवा उसके ज्ञान को ही उसके ज्ञान का साधक माना जाय तो यह मान्यता आरमाश्रयदोष से ग्रस्त होगी, जिसके कारण विध्वंस की न उत्पत्ति ही हो सकेगी, न स्थिति ही हो सकेगी और न उसका ज्ञान ही हो सकेगा । विपनाशकत्व को विनध्वंसजनकता का अवच्छेदक मानने में ज्ञप्ति में आत्माश्रय है, क्योंकि अवच्छेद्यके ज्ञान में अवच्छेदकज्ञान के कारण होने से विघ्नध्वंसजनकता के ज्ञान में उससे अभिन्न विघ्ननाशकत्व का ही शान प्रकृत में अपेकणीय हो जाता है।
२. प्रातिस्विक-इसका अर्थ है प्रत्येक 'स्व' में रहनेवाला, माल के कई स्व-स्वरूप है, जैसे नति. देवनन्दन, प्रार्थना, वस्तुनिर्देश आदि, इनमें नति, प्रार्थना आदि प्रत्येक 'स्व' में रहने वाले नतित्व आदि धर्म नति आदि के प्रातिस्विक रूप हैं ।
३. भावविशेष-जैन शास्त्रों में आत्मा के शुभ-अशुभ एवं शुद्ध-मलिन अध्यवसाय-परिणति को भाव कहते हैं । वे संक्लेश व विशुद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। राग द्वेष काम क्रोधादि काषायिक भाव सक्लेश रूप मलिन अध्यवसाय है। बैराग्य-समादि उपशम-संयमादि के भाव विशुद्धि रूप शुभ अव. साय है। ज्यों ज्यों संश्लेश घटता है स्यों खो विशुद्धि बढ़ती हैं। अब रागादि में दो विभाग है, ६, प्रशस्त, २. अप्रशस्त 1 अप्रशस्त कोटि के राग द्वेष वैषयिक इट-अनिष्ट खानपान-घन-निर्धनता-स्नेह-शत्र आदि पर होते हैं। वे अशुभ भाव हैं । प्रशस्त कोटि का राग परमात्मा-सद्गुरु-शील-संयम-तप-जप आदि पर व द्वेष हिंसा, असल्प आदि पर होता है । वे शुभ भाव है। अशुभ भाव से अशुभ कर्म बन्ध व शुभ भाव से शुभ कर्म बन्ध होता है। देखिए उपदेशमाल्य गाथा-"जज समय जीवो...' | इसीलिए कहा जाता है 'उपयोगे