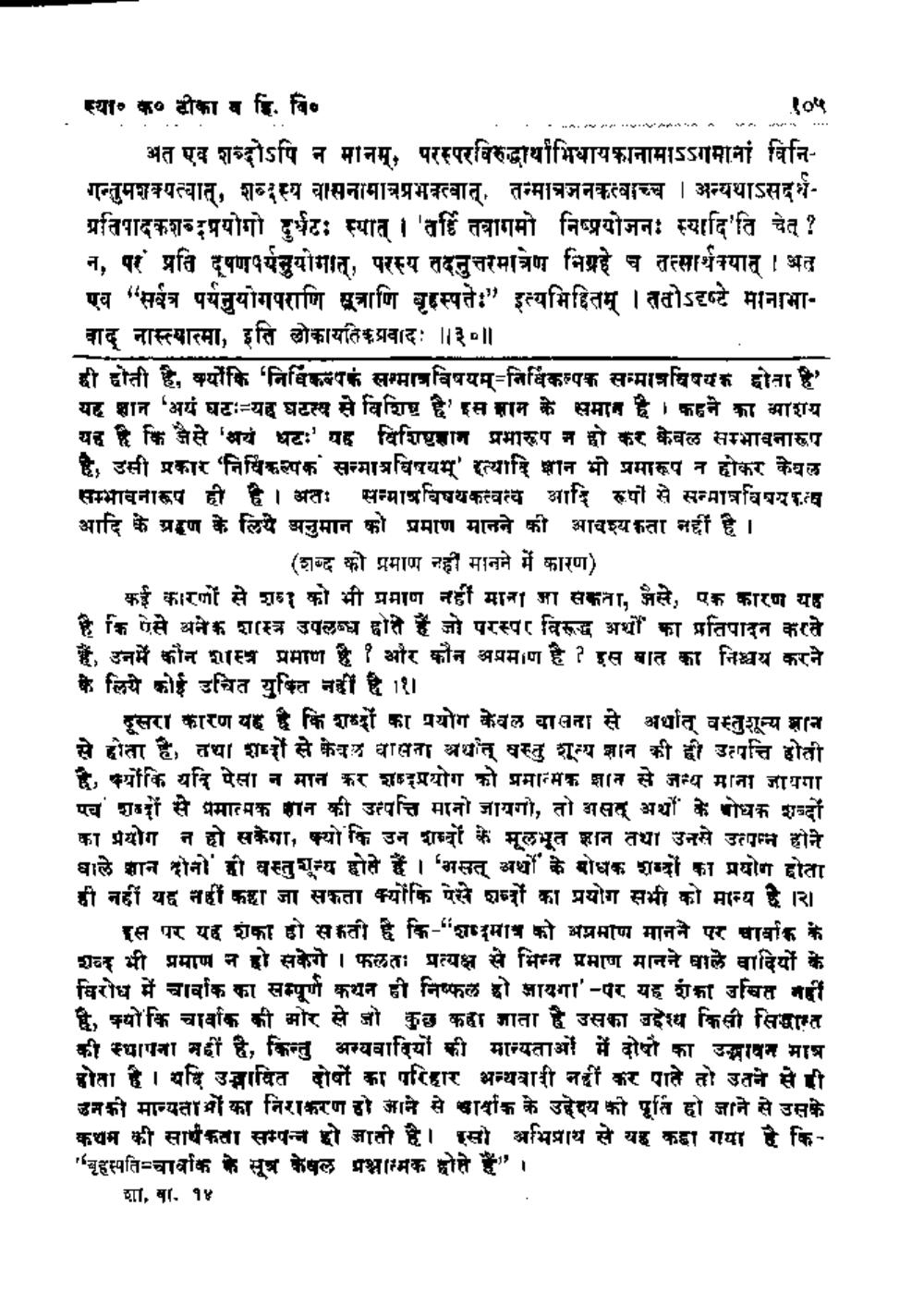________________
.
...
.....MAA
.AA
P
.
स्था का टीका व हि. वि०
१०५ अत एव शब्दोऽपि न मानम्, परस्परविरुद्धार्याभिधायफानामाऽऽगमानां विनिगन्तुमशक्यत्वात्, शब्दस्य वासनामात्रप्रभवत्वात्, तन्मात्रजनकत्वाच्च । अन्यथाऽसदर्थप्रतिपादकशब्दप्रयोगो दुर्धट: स्यात् । 'त ितवागमो निष्प्रयोजनः स्यादिति चेत् ? न, परं प्रति दूषणपर्यनुयोगात्, परस्य तदनुत्तरमात्रेण निग्रहे च तत्सार्थक्यात् । अत एव "सर्वत्र पर्यनुयोगपराणि पूत्राणि बृहस्पतेः" इत्यभिहितम् । ततोऽदृष्टे मानाभावाद् नास्त्यात्मा, इति लोकायतिकवादः ॥३०॥ ही होती है, क्योंकि निर्विकल्प सम्माविषयम्-निर्विकल्पक सम्मानविषयक होता है। यह शान 'अयं घटा यह घटस्य से विशिष्ट है' इस शाम के समान है। कहने का माशय यह है कि जैसे 'अयं घटः' यह विशिष्यज्ञान प्रमारूप न हो कर केवल सम्भावनारूप है, उसी प्रकार निर्विकल्पक सन्मानविषयम्' इत्यादि शान भी प्रमारूप न होकर केवल सम्भावनारूप ही है। अतः सन्माविषयकत्वत्व आदि रूपो से सन्मात्रविषयत्व आदि के ग्रहण के लिये अनुमान को प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है ।
(शब्द को प्रमाण नहीं मानने में कारण) कई कारणों से शभा को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता, जैसे, एक कारण यह है कि ऐसे अनेक शास्त्र उपलब्ध होते है जो परस्पर विरूद्ध अर्थों का प्रतिपादन करते हैं, उनमें कौन शास्त्र प्रमाण है ? और कौन अप्रमाण है ? इस बात का निश्चय करने के लिये कोई उचित युक्ति नहीं है ।
दूसरा कारण यह है कि शब्दों का प्रयोग केवल वासना से अर्थात् वस्तुशून्य ज्ञान से होता है, तथा शहों से केवल वासना अर्थात् वस्तु शून्य ज्ञान की ही उत्पत्ति होती है, क्योंकि यदि ऐसा न मान कर शब्दप्रयोग को प्रमान्मक ज्ञान से जन्य माना जायगा पच शब्दों से प्रमात्मक शान की उत्पत्ति मानो जायगो, तो असत् अर्थों के बोधक शब्दों का प्रयोग न हो सकेगा, क्योंकि उन शम्बों के मूलभूत ज्ञान तथा उनसे उत्पन्न होने वाले शान दोनों ही वस्तुशुन्य होते हैं । 'असत् अर्थो के योधक शब्दों का प्रयोग होता ही नहीं यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग सभी को मान्य है।
इस पर यह शंका हो सकती है कि-"शादमात्र को अप्रमाण मानने पर चार्वाक के शब्द भी प्रमाण न हो सकेगे । फलता प्रत्यक्ष से भिन्न प्रमाण मानने वाले वादियों के विरोध में चार्वाक का सम्पूर्ण कथन ही निष्फल हो जायगा' -पर यह शंका उचित नहीं है, क्योंकि चार्वाक की मोर से जो कुछ कहा जाता है उसका उद्देश्य किसी सिद्धान्त की स्थापना नहीं है, किन्तु अग्यवादियों की मान्यताओं में दोषो का उझावन मात्र होता है। यदि उसावित दोषों का परिहार अन्यवादी नहीं कर पाते तो उतने से दी उनकी मान्यताओं का निराकरण हो आने से बाकि के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने से उसके कथम की सार्थकता सम्पन्न हो जाती है। इसो अभिप्राय से यह कहा गया है कि"बृहस्पति-चार्वाक के सूत्र केवल प्रश्नामक होते हैं"।
शा, बा. १४