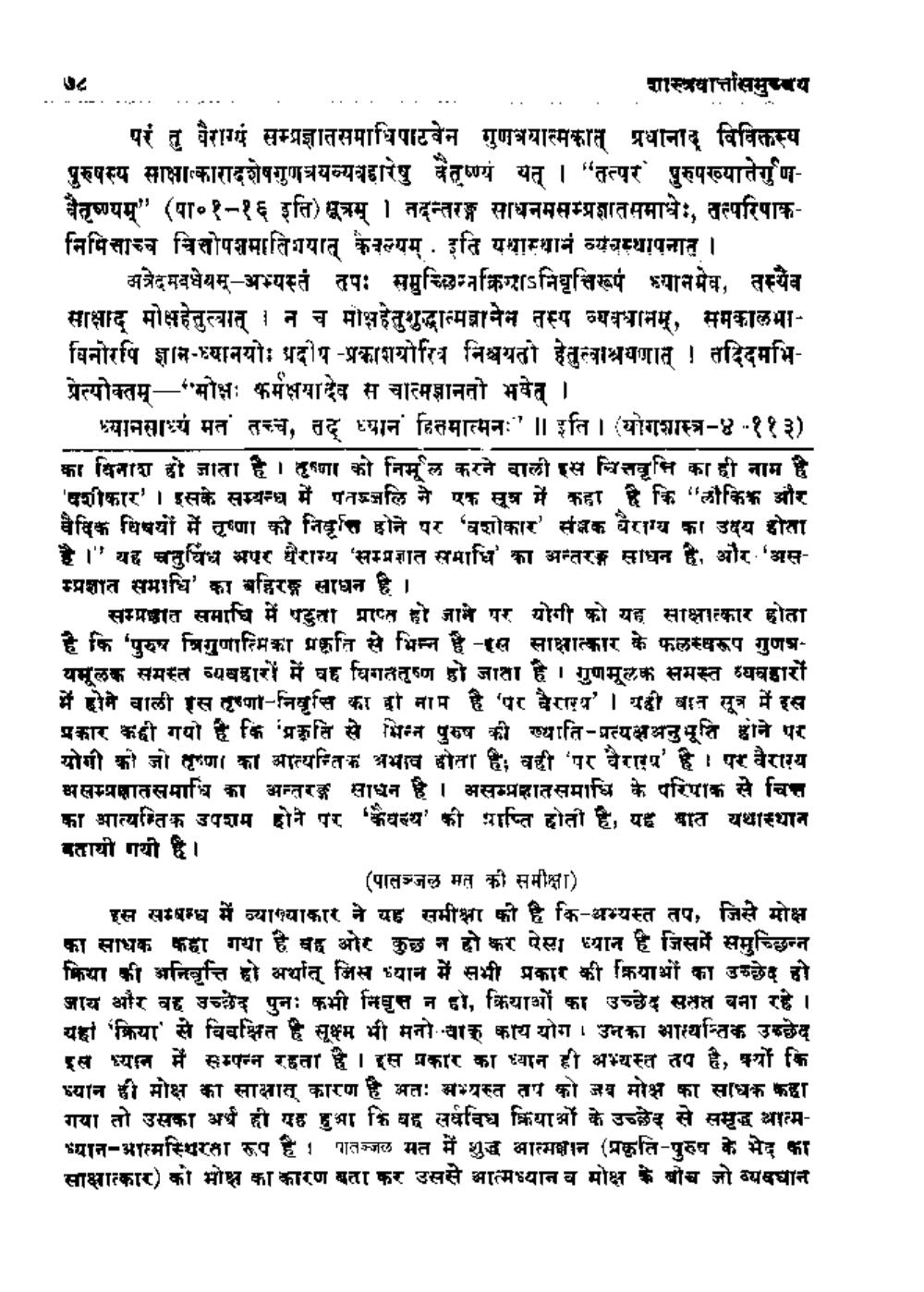________________
शास्त्रवासिमुच्चय परं तु वैराग्यं सम्प्रज्ञातसमाधिपाटवेन गुणत्रयात्मकात् प्रधानाद विविक्तस्य पुरुषस्य साक्षात्कारादशेषगुणत्रयन्यवहारेषु वैतृष्ण्यं यत् । “तत्पर पुरुपख्यातेर्गुणचैतृष्ण्यम्" (पा.१-१६ इति) सूत्रम् । तदन्तरङ्ग साधनमसम्प्रज्ञातसमाधेः, तत्परिपाकनिमिसाच्च चित्तोपशमातिशयात् कैवल्यम् . इति यथास्थानं व्यवस्थापनात ।
अत्रेदमवधेयम्-अभ्यस्तं तपः समुस्टिम्नक्रियानिवृत्तिरूपं ध्यानमेव, तस्यैव साक्षाद् मोक्षहेतुत्वात् । न च मोक्षहेतुशुद्धात्मनानेन तस्य व्यवधानम्, समकालमाविनोरपि ज्ञान-ध्यानयोः प्रदीप -प्रकाशयोरिव निश्चयतो हेतुत्वाश्रयणात् । तदिदमभिप्रेत्योक्तम्-'मोक्षः कर्मक्षया देव स चात्मज्ञानतो भवेत् ।
ध्यानसाध्यं मत तच्च, तद् ध्यान हितमात्मनः' || इति । योगशास्त्र-४.११३) का विनाश हो जाता है। हमणा को निर्मूल करने वाली इस चित्तवृमि का ही नाम है 'पशीकार' । इसके सम्बन्ध में पतम्जलि ने एक सूत्र में कहा है कि "लौकिक और वैविक विषयों में तृष्णा को निवृत्ति होने पर 'वशोकार' संक्षक घेराग्य का उदय होता है।" यह चतुर्विध अपर घेराम्य 'सम्प्रज्ञात समाधि' का अन्तरङ्ग साधन है, और 'असप्रशात समाधि' का बहिरङ्ग साधन है।
सम्प्रहात समाधि में पटुता प्राप्त हो जाने पर योगी को यह साक्षात्कार होता है कि 'पुरुष त्रिगुणात्मिका प्रकृति से भिन्न है -स साक्षात्कार के फलस्वरूप गुणत्रयमूलक समस्त व्यवहारों में घह विगततरुण हो जाता है । गुणमूलक समस्त व्यवहारों में होने वाली सहरणा-निर्वास का वो नाम है पर वैराग्य । यही बान सत्र में इस प्रकार कही गयो है कि प्रकृति से भिन्न पुरुष की ख्याति-प्रत्यक्षअनुभूति होने पर यांगा का जा कृष्णा का आत्यन्तिक अभाव होता है; वही 'पर वैरारप' है। पर वैराग्य घसम्प्रहातसमाधि का अन्तरङ्ग साधन है। असम्माहातसमाधि के परिपाक से चित्त का आत्यन्तिक उपशम होने पर 'कैवल्य' की प्राप्ति होती है, यह बात यथास्थान बतायी गयी है।
(पातञ्जल मत की समीक्षा) इस सम्बन्ध में व्यागयाकार ने यह समीक्षा की है कि-अभ्यस्त तप, जिसे मोक्ष का साधक कहा गया है वह ओर कुछ न हो कर ऐसा ध्यान है जिसमें समुच्छिन्न क्रिया की अनिवृत्ति हो अर्थात् जिस ध्यान में सभी प्रकार की क्रियाओं का उच्छेद हो जाय और वह उच्छेद पुनः कभी निवृस न हो, क्रियाओं का उच्छेद सतत बना रहे । यहा क्रिया' से विवक्षित है सूक्ष्म भी मनो वाक काय योग । उनका मास्यन्तिक उच्छेद इस ध्यान में सम्पन्न रहता है । इस प्रकार का ध्यान ही अभ्यस्त तप है, क्यों कि ध्यान ही मोक्ष का साक्षात् कारण है अतः अभ्यस्त तप को जब मोक्ष का साधक कहा गया तो उसका अर्थ ही यह हुआ कि यह लविध क्रियाओं के उच्छेद से समृद्ध आत्मध्यान-आस्मस्थिरता रूप है। पातञ्जल मत में शुद्ध आत्मज्ञान (प्रकृति-पुरुष के भेद का साक्षात्कार) को मोक्ष का कारण बता कर उससे आत्मध्यान व मोक्ष के बीच जो व्यवधान