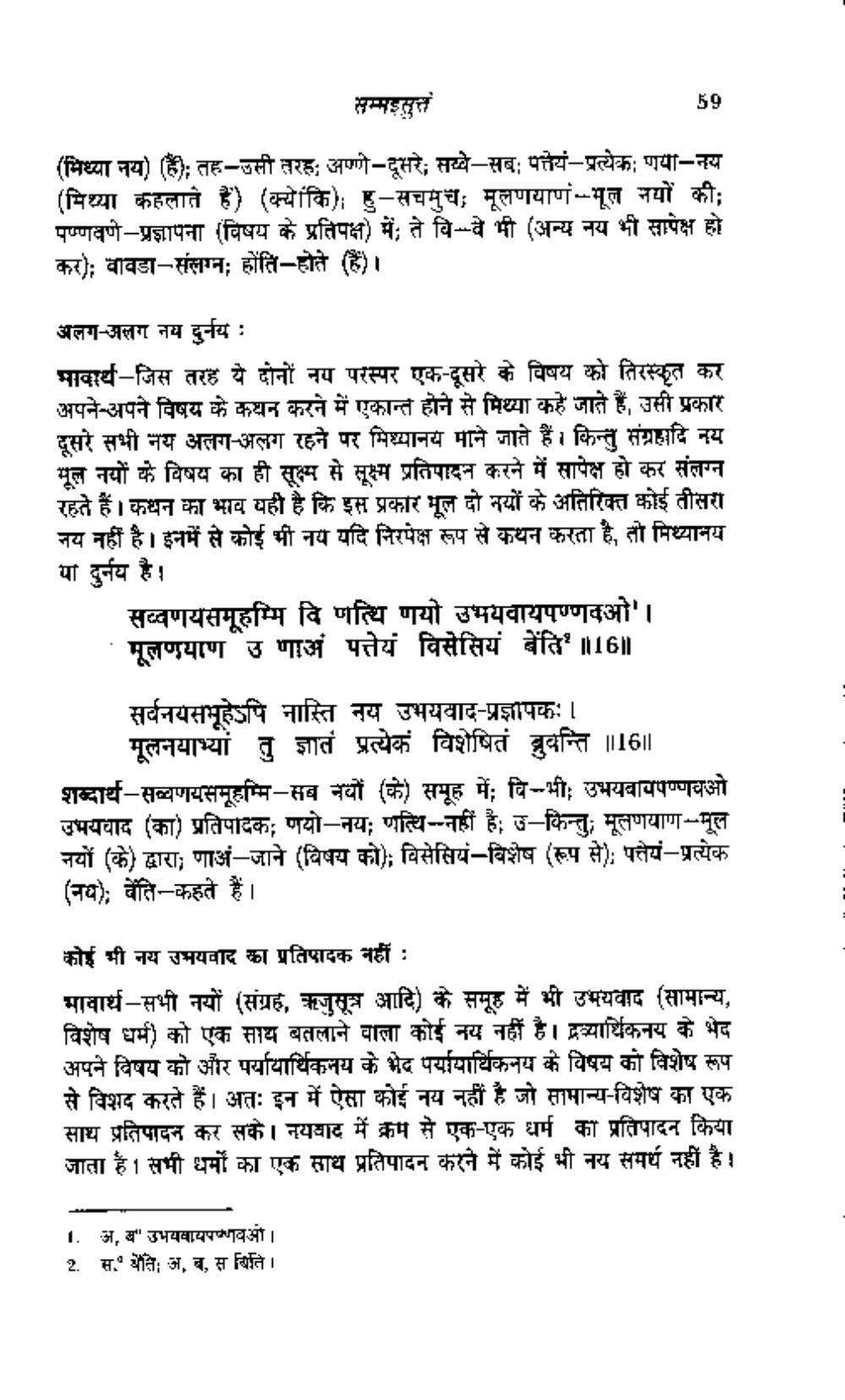________________
सम्मइसुतं
59
(मिथ्या नय) (है), तह-उसी तरह; अणणे-दूसरे, सय्ये-सब; पत्तेयं-प्रत्येक गया-नय (मिथ्या कहलाते हैं) (क्योंकि); हु-सचमुच; मूलणयाणं-मूल नयों की; पण्णवणे-प्रज्ञापना (विषय के प्रतिपक्ष) में; ते वि-वे भी (अन्य नय भी सापेक्ष हो कर); वावडा-संलग्न होति-होते (है)।
अलग-अलग नय दुर्नय : भावार्थ-जिस तरह ये दोनों नय परस्पर एक-दूसरे के विषय को तिरस्कृत कर अपने-अपने विषय के कथन करने में एकान्त होने से मिथ्या कहे जाते हैं, उसी प्रकार दूसरे सभी नय अलग-अलग रहने पर मिथ्यानय माने जाते हैं। किन्तु संग्रहादि नय मूल नयों के विषय का ही सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रतिपादन करने में सापेक्ष हो कर संलग्न रहते हैं। कथन का भाव यही है कि इस प्रकार मूल दो नयों के अतिरिक्त कोई तीसरा नय नहीं है। इनमें से कोई भी नय यदि निरपेक्ष रूप से कथन करता है, तो मिथ्यानय या दुर्नय है।
सवणयसमूहम्मि वि णस्थि णयो उभयवायपण्णवओ'। मूलणयाण उ णाअं पत्तेयं विसेसियं बेंति ॥16॥
सर्वनयसभहेऽपि नास्ति नय उभयवाद-प्रज्ञापकः ।
मूलनयाभ्यां तु ज्ञातं प्रत्येक विशेषितं ब्रुवन्ति ॥16|| शब्दार्थ-सव्यणयसमूहम्मि-सब नवों (के) समूह में; वि-भी; उभयवापपण्णवओ उभयवाद (का) प्रतिपादक; णयो-नय; णत्यि-नहीं है; उ-किन्तु; मूलणयाण-मूल नयों (के) द्वारा; णाअं-जाने (विषय को); विसेसियं-विशेष (रूप से); पत्तेयं-प्रत्येक (नय); वेति-कहते हैं।
कोई भी नय उभयवाद का प्रतिपादक नहीं : भावार्थ-सभी नयों (संग्रह, ऋजुसूत्र आदि) के समूह में भी उपयवाद (सामान्य, विशेष धर्म) को एक साथ बतलाने वाला कोई नय नहीं है। द्रव्यार्थिकनय के भेद अपने विषय को और पर्यायार्थिकनय के भेद पर्यायार्थिकनय के विषय को विशेष रूप से विशद करते हैं। अतः इन में ऐसा कोई नय नहीं है जो सामान्य-विशेष का एक साथ प्रतिपादन कर सके। नयवाद में क्रम से एक-एक धर्म का प्रतिपादन किया जाता हैं। सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन करने में कोई भी नय समर्थ नहीं है।
1. अ, ब" उभयवायपष्णवओ। 2. स.' यतिः अ, ब, स विति।