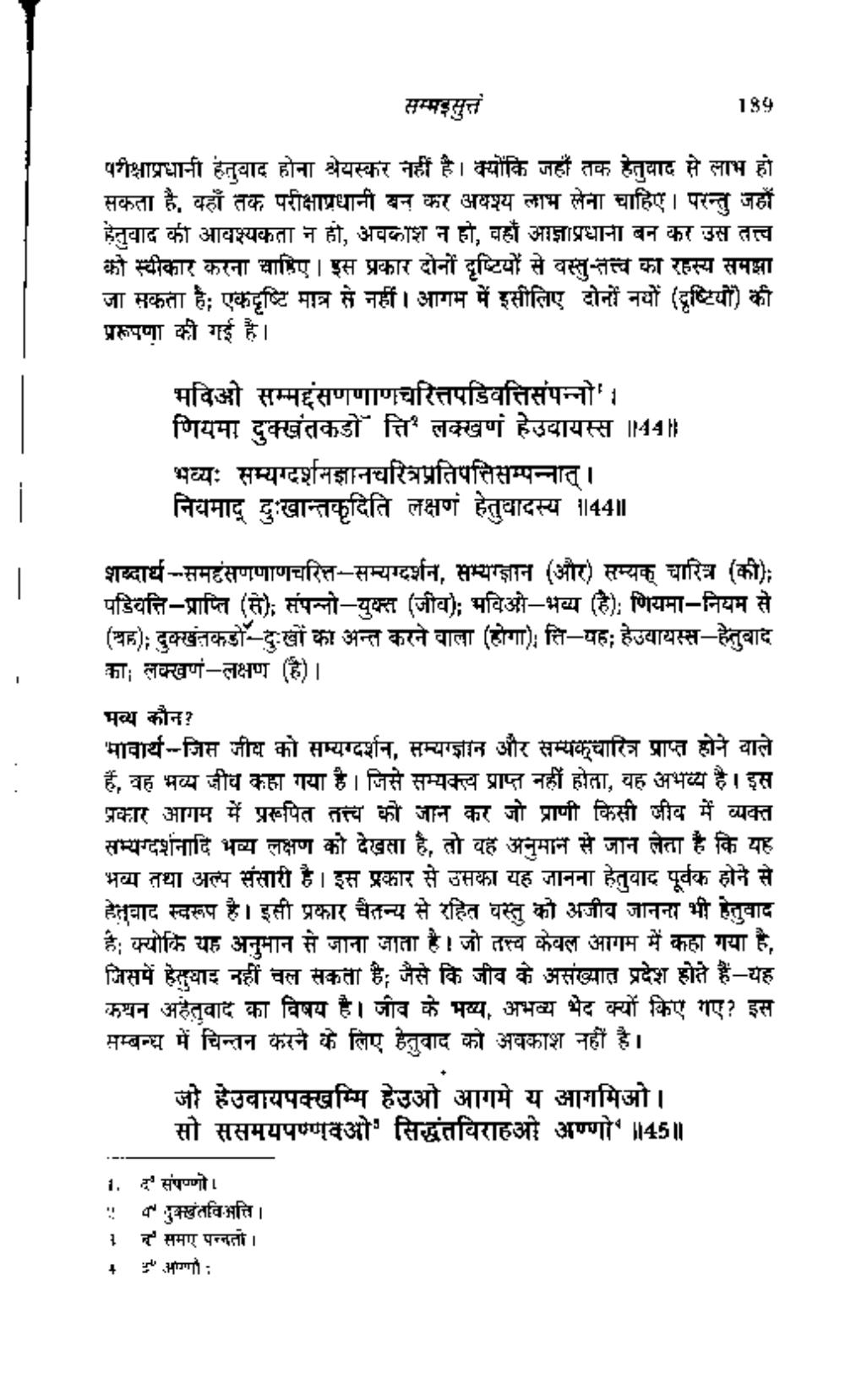________________
सम्मइसुतं
184
परीक्षाप्रधानी हेतुवाद होना श्रेयस्कर नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हेतुयाद से लाभ हो सकता है, वहाँ तक परीक्षाप्रधानी बन कर अवश्य लाभ लेना चाहिए। परन्तु जहाँ हेतुवाद की आवश्यकता न हो, अवकाश न हो, वहाँ आज्ञाप्रधाना बन कर उस तत्त्व को स्वीकार करना चाहिए । इस प्रकार दोनों दृष्टियों से वस्तु-तत्त्व का रहस्य समझा जा सकता है; एकदृष्टि मात्र से नहीं। आगम में इसीलिए दोनों नयों (दृष्टियों) की प्ररूपणा की गई है।
मविओ सम्मइंसणणाणचरित्तपडिवत्तिसंपन्नो' । णियमा दुक्खंतकडों त्ति लक्खणं हेउवायस्स 1440 भव्यः सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्रप्रतिपत्तिसम्पन्नात। नियमाद् दुःखान्तकृदिति लक्षणं हेतुवादस्य ||44॥
शब्दार्थ-समहसणणाणचरित्त-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान (और) सम्यक चारित्र (की); पडिवत्ति-प्राप्ति (से); संपन्नो-युक्स (जीव); भविओ-भव्य (है); णियमा-नियम से (वह); दुक्खंतकड़ों-दुःखों का अन्त करने वाला (होगा); ति–यह; हेउयायस्स-हेतुबाद का लक्खणं-लक्षण (है)। भव्य कौन? भावार्थ-जिस जीव को सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र प्राप्त होने वाले हैं, वह भव्य जीव कहा गया है। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता, वह अभव्य है। इस प्रकार आगम में प्ररूपित तत्त्व को जान कर जो प्राणी किसी जीव में व्यक्त सम्यग्दर्शनादि भव्य लक्षण को देखता है, तो वह अनुमान से जान लेता है कि यह भव्य तथा अल्प संसारी है। इस प्रकार से उसका यह जानना हेतुबाद पूर्वक होने से हेतुवाद स्वरूप है। इसी प्रकार चैतन्य से रहित वस्तु को अजीव जानना भी हेतुवाद है; क्योकि यह अनुमान से जाना जाता है। जो तत्त्व केवल आगम में कहा गया है, जिसमें हेस्याद नहीं चल सकता है। जैसे कि जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं-यह कथन अहेतुवाद का विषय है। जीव के भव्य, अभव्य भेद क्यों किए गए? इस सम्बन्ध में चिन्तन करने के लिए हेतुवाद को अवकाश नहीं है।
जो हेउवायपक्खम्मि हेउओ आगमे य आगमिओ। सो ससमयपण्णवओ' सिद्धंतविराहओ अण्णो' 145॥
1. द' संपण्णो । :: मुक्खंतवि अत्ति।
न' समए पन्नतो। है आग्णा :