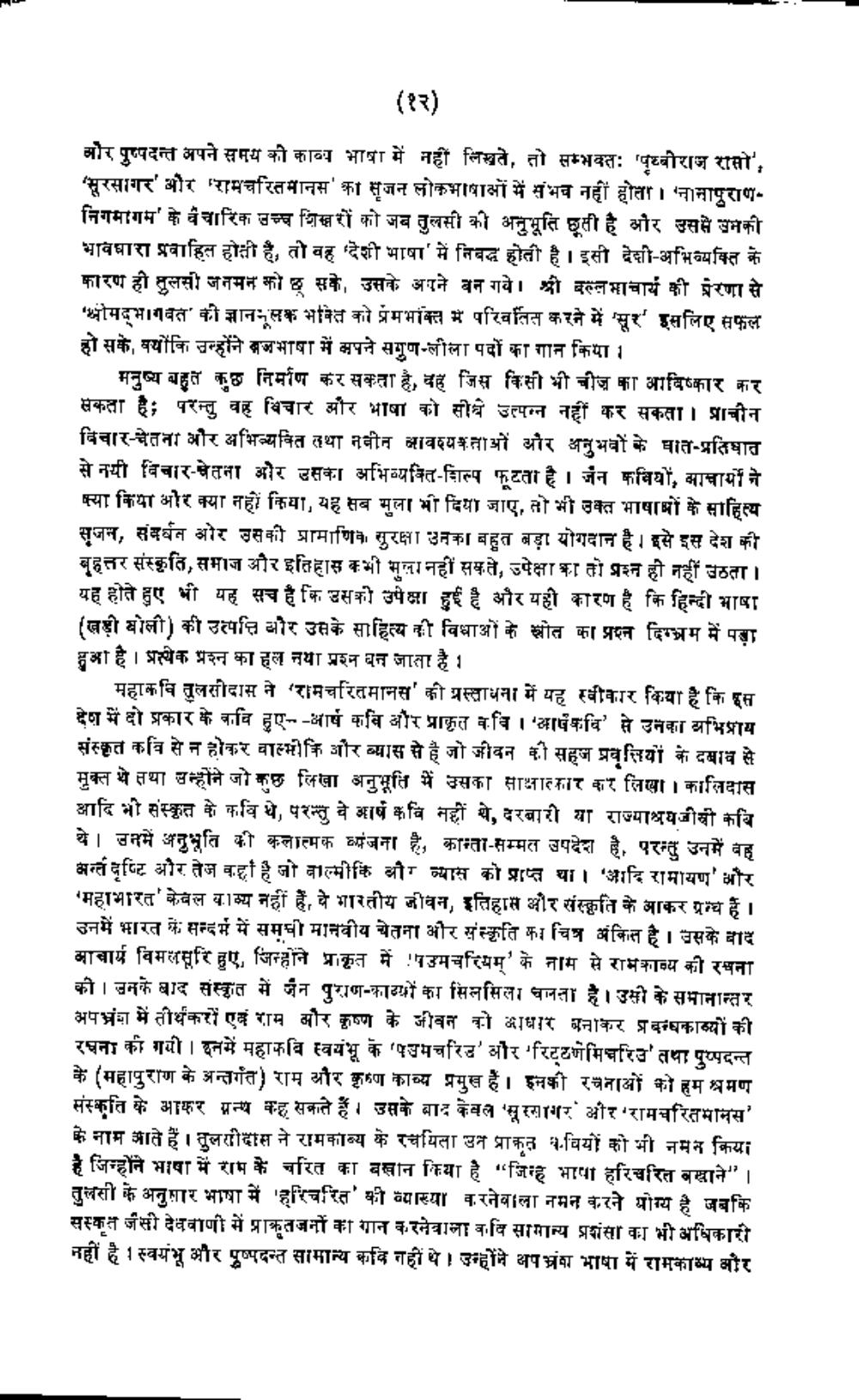________________
और पुष्पदन्त अपने समय की काव्य भाषा में नहीं लिखते, तो सम्भवत: 'पृथ्वीराज रासो', 'सूरसागर' और 'रामचरितमानस' का सृजन लोकभाषाओं में संभव नहीं होता। नानापुराणनिगमागम' के वैचारिक उच्च शिनरों को जब तुलसी की अनुभूति छूती है और उससे उनकी भावधारा प्रवाहित होती है, तो वह 'देशी भाषा में निबद्ध होती है । इसी देशी-अभिव्यक्ति के कारण ही तुलसी जनमन को छु सके, उसके अपने बन गये। श्री बल्लभाचार्य की प्रेरणा से 'श्रीमद्भागवत' की ज्ञानमूलक भक्ति को प्रेम भक्ति में परिवर्तित करने में 'सूर' इसलिए सफल हो सके, क्योंकि उन्होंने अजभाषा में अपने सगुण-लीला पदों का गान किया ।
मनुष्य बहुत कुछ निर्माण कर सकता है, वह जिस किसी भी चीज का आविष्कार कर सकता है। परन्तु वह विचार और भाषा को सीधे उत्पन्न नहीं कर सकता। प्राचीन विचार-चेतना और अभिव्यक्ति तथा नवीन आवश्यकताओं और अनुभवों के घात-प्रतिधात से नयी विचार-चेतना और उसका अभिव्यक्ति-शिल्प फटता है । जन कवियों, आचार्यों ने क्या किया और क्या नहीं किया, यह सब मुला भी दिया जाए, तो भी उक्त भाषात्रों के साहित्य सृजन, संवर्धन और उसकी प्रामाणिक सुरक्षा उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसे इस देश की बृहत्तर संस्कृति, समाज और इतिहास कभी भुला नहीं सकते, उपेक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह होते हुए भी यह सच है कि उसकी उपेक्षा हुई है और यही कारण है कि हिन्दी भाषा (खड़ी बोली) की उत्पत्ति और उसके साहित्य की विधाओं के स्रोत का प्रश्न दिग्भ्रम में पड़ा हुआ है । प्रत्येक प्रश्न का हल नया प्रश्न बन जाता है । ___ महाकवि तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' की प्रस्तावना में यह स्वीकार किया है कि इस देश में दो प्रकार के बाद हुए---आर्ष कवि और प्राकृत कवि । 'आकवि' से उनका अभिप्राय संस्कृत कवि से न होकर वाल्मीकि और ब्यास से है जो जीवन को सहज प्रवृत्तियों के दबाव से मुक्त थे तथा उन्होंने जो कुछ लिखा अनुभूति में उसका साक्षात्कार कर लिया। कालिदास आदि भी संस्कृत के कवि थे, परन्तु वे आर्ष कवि नहीं थे, दरबारी या राज्याश्रयजीबी कवि थे। उनमें अनुभूति की कलात्मक व्यंजना है, कान्ता-सम्मत उपदेश है, परन्तु उनमें वह अन्तं दृष्टि और तेज वही है जो वाल्मीकि और व्यास को प्राप्त था। 'आदि रामायण' और 'महाभारत' केवल याव्य नहीं हैं, वे भारतीय जीवन, इतिहास और संस्कृति के आकर ग्रन्थ हैं। उनमें भारत के सन्दर्भ में समधी मानवीय चेतना और संस्कृति का चित्र अंकित है। उसके बाद आवार्य विमलमूरि हुए, जिन्होंने प्राकृत में 'पउमरियम्' के नाम से रामकाव्य की रचना की। उनके बाद संस्कृति में जैन पुराण-काव्यों का सिलसिला चलता है। उसी के समानान्तर अपभ्रंश में तीर्थंकरों एवं राम और कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर प्रबन्धकाव्यों की रचना की गयी । इनमें महाकवि स्वयंभू के 'एउमचरिउ' और 'रिट्टमिचरित' तथा पुष्पदन्त के (महापुराण के अन्तर्गत) राम और कृष्ण काव्य प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं को हम श्रमण संस्कृति के आकर ग्रन्थ कह सकते हैं। उसके बाद केवल 'सूरसागर और 'रामचरितमानस' के नाम आते हैं । तुलसीदास ने रामकाव्य के रचयिता उन प्राकृत ३.वियों को भी नमन क्रिया है जिन्होंने भाषा में राम के चरित का बखान किया है “जिन्ह भाषा हरिचरित बखाने" | तुलसी के अनुसार भाषा में 'हरिचरित' की व्याख्या करनेवाला नमन करने योग्य है जबकि सस्कृत जैसी देववाणी में प्राकृतजनों का गान करनेवाला बवि सामान्य प्रशंसा का भी अधिकारी नहीं है । स्वयंभू और पुष्पदन्त सामान्य कवि नहीं थे। उन्होंने अपभ्रंका भाषा में रामकाव्य और