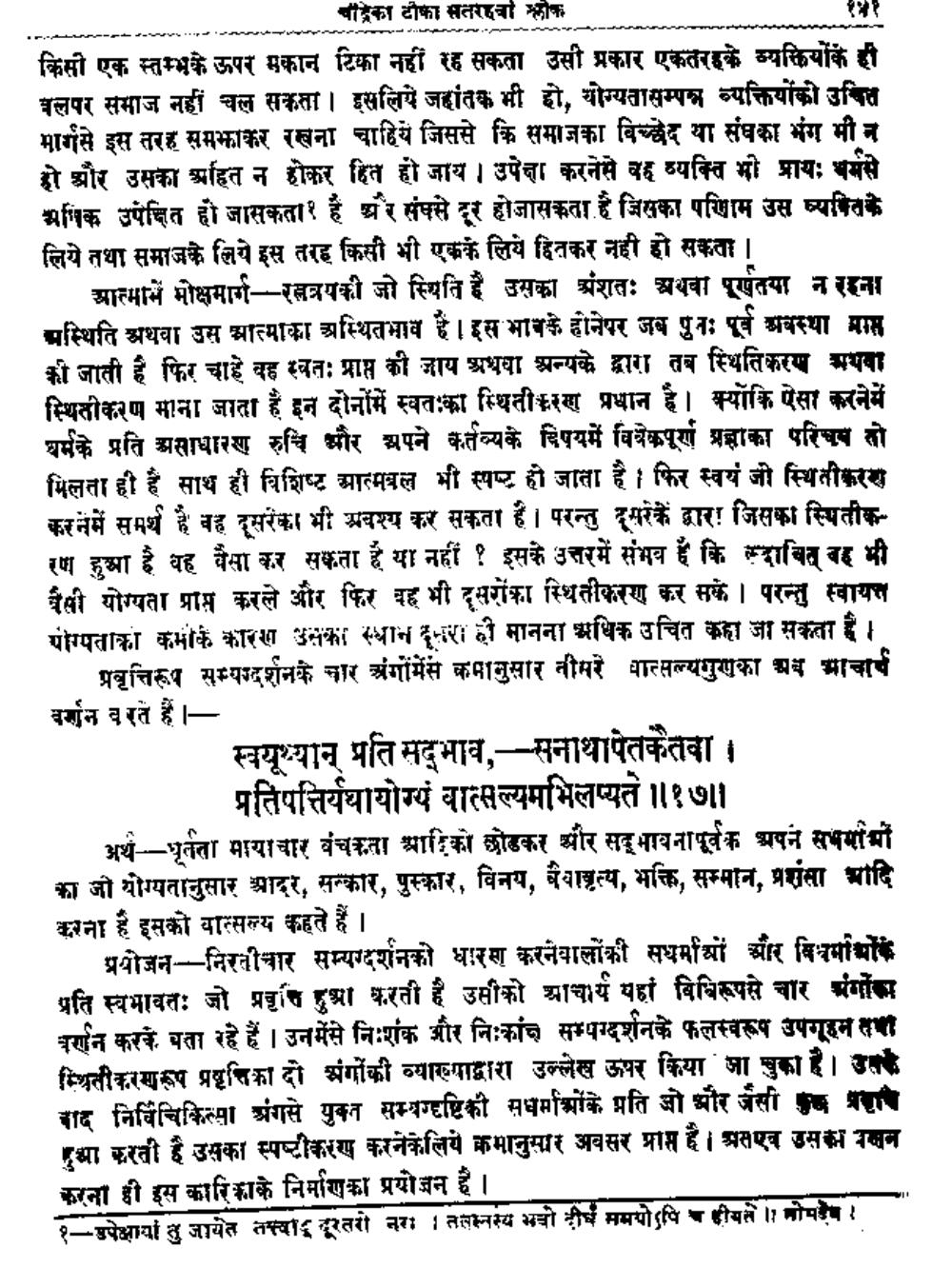________________
बौद्रिका टीका सतरवा श्लोक किसी एक स्तम्भके ऊपर मकान टिका नहीं रह सकता उसी प्रकार एकतरहके व्यक्तियोंके ही वलपर समाज नहीं चल सकता। इसलिये जहांतक भी हो, योग्यतासम्पन्न व्यक्तियोंको उचित मार्गसे इस तरह समझाकर रखना चाहिये जिससे कि समाजका विच्छेद या संघका भंग भीन हो और उसका अहित न होकर हित हो जाय । उपेक्षा करनेसे वह व्यक्ति भी प्रायः धर्मसे अपिक उपेक्षित हो जासकता है पर संपसे दूर होजासकता है जिसका पणिाम उस व्यक्ति के लिये तथा समाजके लिये इस तरह किसी भी एकके लिये हितकर नही हो सकता।
आत्मामें मोक्षमार्ग-रलत्रयकी जो स्थिति है उसका अंशतः अथवा पूर्णतया न रहना प्रस्थिति अथवा उस आत्माका अस्थितभाव हैं । इस भावके होनेपर जब पुनः पूर्व अवस्था मास की जाती है फिर चाहे वह स्वतः प्राप्त की जाय अथवा अन्यके द्वारा तब स्थितिकरण अथवा स्थितीकरण माना जाता है इन दोनों में स्वतःका स्थितीकरण प्रधान है। क्योंकि ऐसा करने में धर्मके प्रति असाधारण रुचि और अपने कर्तव्यके विषयमें विवेकपूर्ण प्रज्ञाका परिषष तो मिलता ही है साथ ही विशिष्ट आत्मबल भी स्पष्ट हो जाता है। फिर स्वयं जो स्थितीकरण करने में समर्थ है वह दूसरेका भी अवश्य कर सकता है। परन्तु दूसरे के द्वारा जिसका स्पितीकरण हुआ है वह वैसा कर सकता है या नहीं ? इसके उत्तर में संभव है कि सदाचित् वह भी वैसी योग्यता प्राप्त करले और फिर वह भी दूसरोंका स्थितीकरण कर सके। परन्तु स्वायत योग्यताका कमांक कारण उसका स्थान द्वारा ही मानना अधिक उचित कहा जा सकता है।
प्रवृत्तिरूप सम्यग्दर्शनके चार अंगोंमेंस क्रमानुसार नीमरे वात्सल्यगुणका अब प्राचार्य वर्णन वरत हैं।
स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव, सनाथापेतकैतवा ।
प्रतिपत्तियथायोग्यं वात्सल्यमभिलप्यते ॥१७॥ अर्थ-धूर्तता मायाचार वंचकता आदिको छोडकर और सद्भावनापूर्वक अपने सपनीमों का जो योग्यतानुसार आदर, सन्कार, पुस्कार, विनय, वैवात्य, भक्ति, सम्मान, प्रशंसा आदि करना है इसको वात्सल्य कहते हैं।
प्रयोजन-निरतीचार सम्यग्दर्शनको धारण करनेवालोंकी सधर्माओं और विधाभोंक प्रति स्वभावतः जो प्रवृत्ति हुआ करती है उसीको प्राचार्य यहां विधिरूपसे चार अंगों वर्णन करके बता रहे हैं । उनमेंसे निःशंक और निःकांश सम्पग्दर्शनके फलस्वरूप उपग्रहमा मिथतीकरणरूप प्रवृत्तिका दो अंगोंकी व्याख्याद्वारा उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसके बाद निर्विचिकित्सा अंगसे युक्त सम्यग्दृष्टिको सधर्मानोंके प्रति जो और जैसी एक प्रक
आ करती है उसका स्पष्टीकरण करनेकेलिये क्रमानुसार अवसर प्राप्त है। अतएव उस वक्षन करना ही इस कारिकाके निर्माणका प्रयोजन है। १-उपेक्षायां तु जायेत तत्वाप दूरतरो नरा । तलनस्य भवो दीर्थ ममयोऽपि च हीयते ॥ मोपड़े।