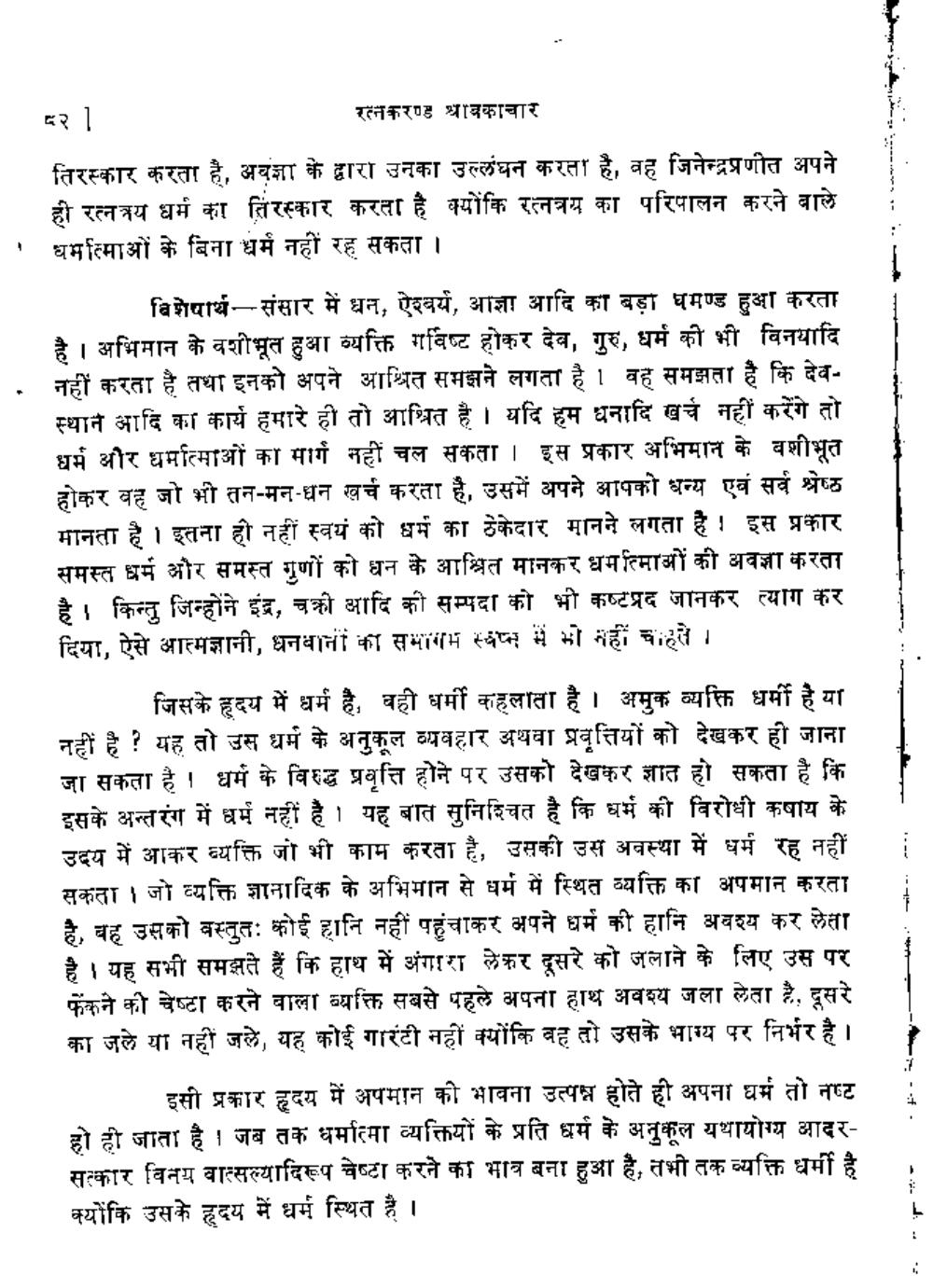________________
"
·
रत्नकरण्ड श्रावकाचार
५२ ]
तिरस्कार करता है, अवज्ञा के द्वारा उनका उल्लंघन करता है, वह जिनेन्द्रप्रणीत अपने ही रत्नत्रय धर्म का तिरस्कार करता है क्योंकि रत्नत्रय का परिपालन करने वाले धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रह सकता ।
विशेषार्थ - संसार में धन, ऐश्वर्य, आज्ञा आदि का बड़ा घमण्ड हुआ करता है । अभिमान के वशीभूत हुआ व्यक्ति गर्विष्ट होकर देव, गुरु, धर्म की भी विनयादि
नहीं करता है तथा इनको अपने आश्रित समझने लगता है । वह समझता है कि देव - स्थान आदि का कार्य हमारे ही तो आश्रित है । यदि हम धनादि खर्च नहीं करेंगे तो धर्म और धर्मात्माओं का मार्ग नहीं चल सकता। इस प्रकार अभिमान के वशीभूत होकर वह जो भी तन-मन-धन खर्च करता है, उसमें अपने आपको धन्य एवं सर्व श्रेष्ठ मानता है । इतना ही नहीं स्वयं को धर्म का ठेकेदार मानने लगता है । इस प्रकार समस्त धर्म और समस्त गुणों को धन के आश्रित मानकर धर्मात्माओं की अवज्ञा करता है । किन्तु जिन्होंने इंद्र, चक्री आदि की सम्पदा को भी कष्टप्रद जानकर त्याग कर दिया, ऐसे आत्मज्ञानी, धनवानों का समागम स्वप्न में भी नहीं चाहते ।
जिसके हृदय में धर्म है, वही धर्मी कहलाता है । अमुक व्यक्ति धर्मी है या नहीं है ? यह तो उस धर्म के अनुकूल व्यवहार अथवा प्रवृत्तियों को देखकर ही जाना जा सकता है । धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति होने पर उसको देखकर ज्ञात हो सकता है कि इसके अन्तरंग में धर्म नहीं है । यह बात सुनिश्चित है कि धर्म की विरोधी कषाय के उदय में आकर व्यक्ति जो भी काम करता है, उसकी उस अवस्था में धर्म रह नहीं सकता । जो व्यक्ति ज्ञानादिक के अभिमान से धर्म में स्थित व्यक्ति का अपमान करता है, वह उसको वस्तुतः कोई हानि नहीं पहुंचाकर अपने धर्म की हानि अवश्य कर लेता है । यह सभी समझते हैं कि हाथ में अंगारा लेकर दूसरे को जलाने के लिए उस पर फेंकने की चेष्टा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपना हाथ अवश्य जला लेता है. दूसरे का जले या नहीं जले, यह कोई गारंटी नहीं क्योंकि वह तो उसके भाग्य पर निर्भर है ।
इसी प्रकार हृदय में अपमान की भावना उत्पन्न होते ही अपना धर्म तो नष्ट हो ही जाता है । जब तक धर्मात्मा व्यक्तियों के प्रति धर्म के अनुकूल यथायोग्य आदरसत्कार विनय वात्सल्यादिरूप चेष्टा करने का भाव बना हुआ है, तभी तक व्यक्ति धर्मी है क्योंकि उसके हृदय में धर्म स्थित है ।
·
+