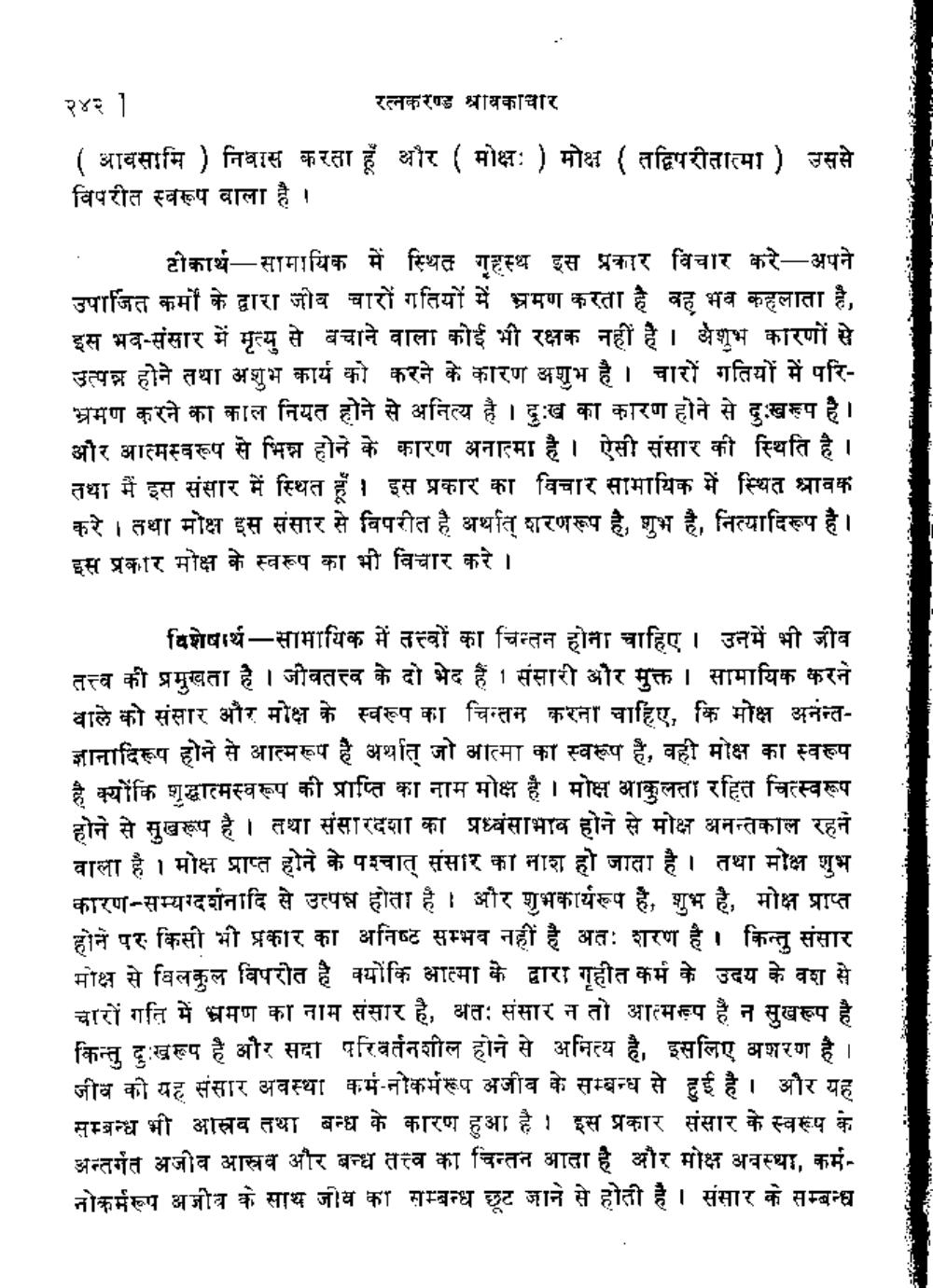________________
२४२ ]
रत्नकरण्ड श्रावकाचार
( आवसामि ) निवास करता हूँ और ( मोक्षः ) मोक्ष ( तद्विपरीतात्मा ) उससे विपरीत स्वरूप वाला है ।
टीकार्थ - सामायिक में स्थित गृहस्थ इस प्रकार विचार करे – अपने उपार्जित कर्मों के द्वारा जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है वह भव कहलाता है, इस भव-संसार में मृत्यु से बचाने वाला कोई भी रक्षक नहीं हैं । अशुभ कारणों से उत्पन्न होने तथा अशुभ कार्य को करने के कारण अशुभ है। चारों गतियों में परि'भ्रमण करने का काल नियत होने से अनित्य है । दुःख का कारण होने से दुःखरूप है । और आत्मस्वरूप से भिन्न होने के कारण अनात्मा है । ऐसी संसार की स्थिति है । तथा मैं इस संसार में स्थित हूँ । इस प्रकार का विचार सामायिक में स्थित श्रावक करे । तथा मोक्ष इस संसार से विपरीत है अर्थात् शरणरूप है, शुभ है, नित्यादिरूप है। इस प्रकार मोक्ष के स्वरूप का भी विचार करे ।
विशेषार्थ - सामायिक में तत्त्वों का चिन्तन होना चाहिए। उनमें भी जीव तत्त्व की प्रमुखता है । जीवतत्त्व के दो भेद हैं । संसारी और मुक्त । सामायिक करने वाले को संसार और मोक्ष के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए, कि मोक्ष अनंन्तज्ञानादिरूप होने से आत्मरूप है अर्थात् जो आत्मा का स्वरूप है, वही मोक्ष का स्वरूप है क्योंकि शुद्धात्मस्वरूप की प्राप्ति का नाम मोक्ष है । मोक्ष आकुलता रहित चित्स्वरूप होने से सुखरूप है । तथा संसारदशा का प्रध्वंसाभाव होने से मोक्ष अनन्तकाल रहने वाला है । मोक्ष प्राप्त होने के पश्चात् संसार का नाश हो जाता है। तथा मोक्ष शुभ कारण - सम्यग्दर्शनादि से उत्पन्न होता है । और शुभकार्यरूप है, शुभ है, मोक्ष प्राप्त होने पर किसी भी प्रकार का अनिष्ट सम्भव नहीं है अतः शरण है । किन्तु संसार मोक्ष से बिलकुल विपरीत है क्योंकि आत्मा के द्वारा गृहीत कर्म के उदय के वश से चारों गति में भ्रमण का नाम संसार है, अतः संसार न तो आत्मरूप है न सुखरूप है किन्तु दुःखरूप है और सदा परिवर्तनशील होने से अनित्य है, इसलिए अशरण है । जीव को यह संसार अवस्था कर्म- नौकर्मरूप अजीव के सम्बन्ध से हुई है । और यह सम्बन्ध भी आस्रव तथा बन्ध के कारण हुआ है । इस प्रकार संसार के स्वरूप के अन्तर्गत अजीव आस्रव और बन्ध तत्त्व का चिन्तन आता है और मोक्ष अवस्था, कर्मनोकर्मरूप अजीव के साथ जीव का सम्बन्ध छूट जाने से होती है । संसार के सम्बन्ध