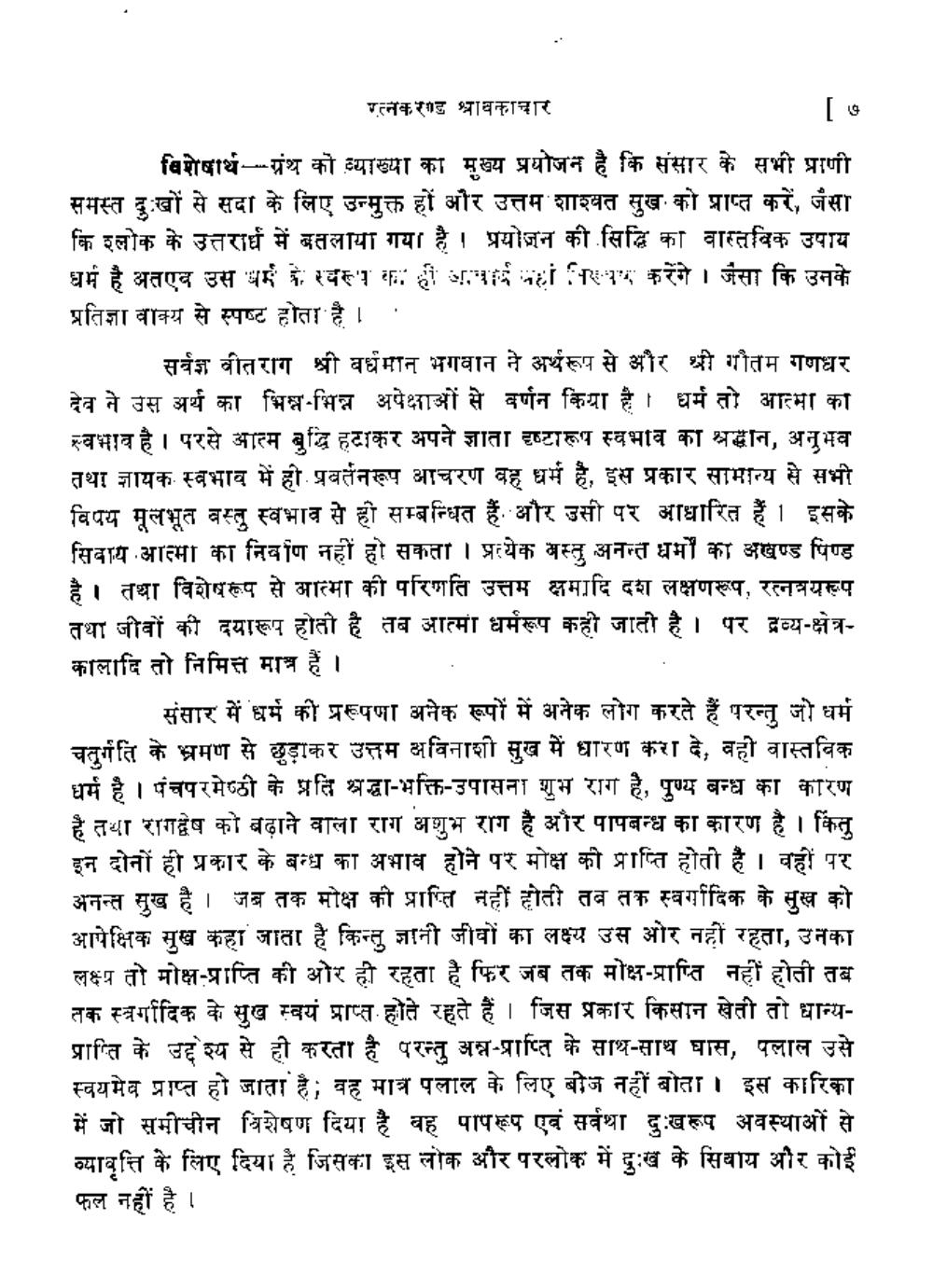________________
रत्नकरगढ श्रावकाचार
[७
विशेषार्थ----ग्रंथ को व्याख्या का मुख्य प्रयोजन है कि संसार के सभी प्राणी समस्त दुःखों से सदा के लिए उन्मुक्त हों और उत्तम शाश्वत सुख को प्राप्त करें, जैसा कि श्लोक के उत्तरार्ध में बतलाया गया है। प्रयोजन की सिद्धि का वास्तविक उपाय धर्म है अतएव उस धर्म के स्वरूप काही काही नियम करेंगे । जैसा कि उनके प्रतिज्ञा वाक्य से स्पष्ट होता है। .
सर्वज्ञ वीतराग श्री बर्धमान भगवान ने अर्थरूप से और श्री गौतम गणधर देव ने उस अर्थ का भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से वर्णन किया है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है । परसे आत्म बुद्धि हटाकर अपने ज्ञाता दृष्टारूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव तथा ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तनरूप आचरण वह धर्म है, इस प्रकार सामान्य से सभी विपय मूलभूत वस्तु स्वभाव से ही सम्बन्धित हैं और उसी पर आधारित हैं । इसके सिवाय आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता । प्रत्येक बस्तु अनन्त धर्मों का अखण्ड पिण्ड है। तथा विशेषरूप से आत्मा की परिणति उत्तम क्षमादि दश लक्षणरूप, रत्नत्रयरूप तथा जीवों की दयारूप होती है तब आत्मा धर्मरूप कही जाती है। पर द्रव्य-क्षेत्रकालादि तो निमित्त मात्र हैं।
संसार में धर्म की प्ररूपणा अनेक रूपों में अनेक लोग करते हैं परन्तु जो धर्म चतुर्गति के भ्रमण से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धारण करा दे, वही वास्तविक धर्म है । पंचपरमेष्ठी के प्रति श्रद्धा-भक्ति-उपासना शुभ राग है, पुण्य बन्ध का कारण है तथा रागद्वेष को बढ़ाने वाला राग अशुभ राग है और पापबन्ध का कारण है। किंतु इन दोनों ही प्रकार के बन्ध का अभाव होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है । वहीं पर अनन्त सुख है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक स्वर्गादिक के सुख को आपेक्षिक सुख कहा जाता है किन्तु ज्ञानी जीवों का लक्ष्य उस ओर नहीं रहता, उनका लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति की ओर ही रहता है फिर जब तक मोक्ष-प्राप्ति नहीं होती तब तक स्वर्गादिक के सुख स्वयं प्राप्त होते रहते हैं । जिस प्रकार किसान खेती तो धान्यप्राप्ति के उद्देश्य से ही करता है परन्तु अन्न-प्राप्ति के साथ-साथ घास, पलाल उसे स्वयमेव प्राप्त हो जाता है; वह मात्र पलाल के लिए बीज नहीं बोता। इस कारिका में जो समीचीन विशेषण दिया है वह पापरूप एवं सर्वथा दुःखरूप अवस्थाओं से व्यावृत्ति के लिए दिया है जिसका इस लोक और परलोक में दुःख के सिवाय और कोई फल नहीं है ।