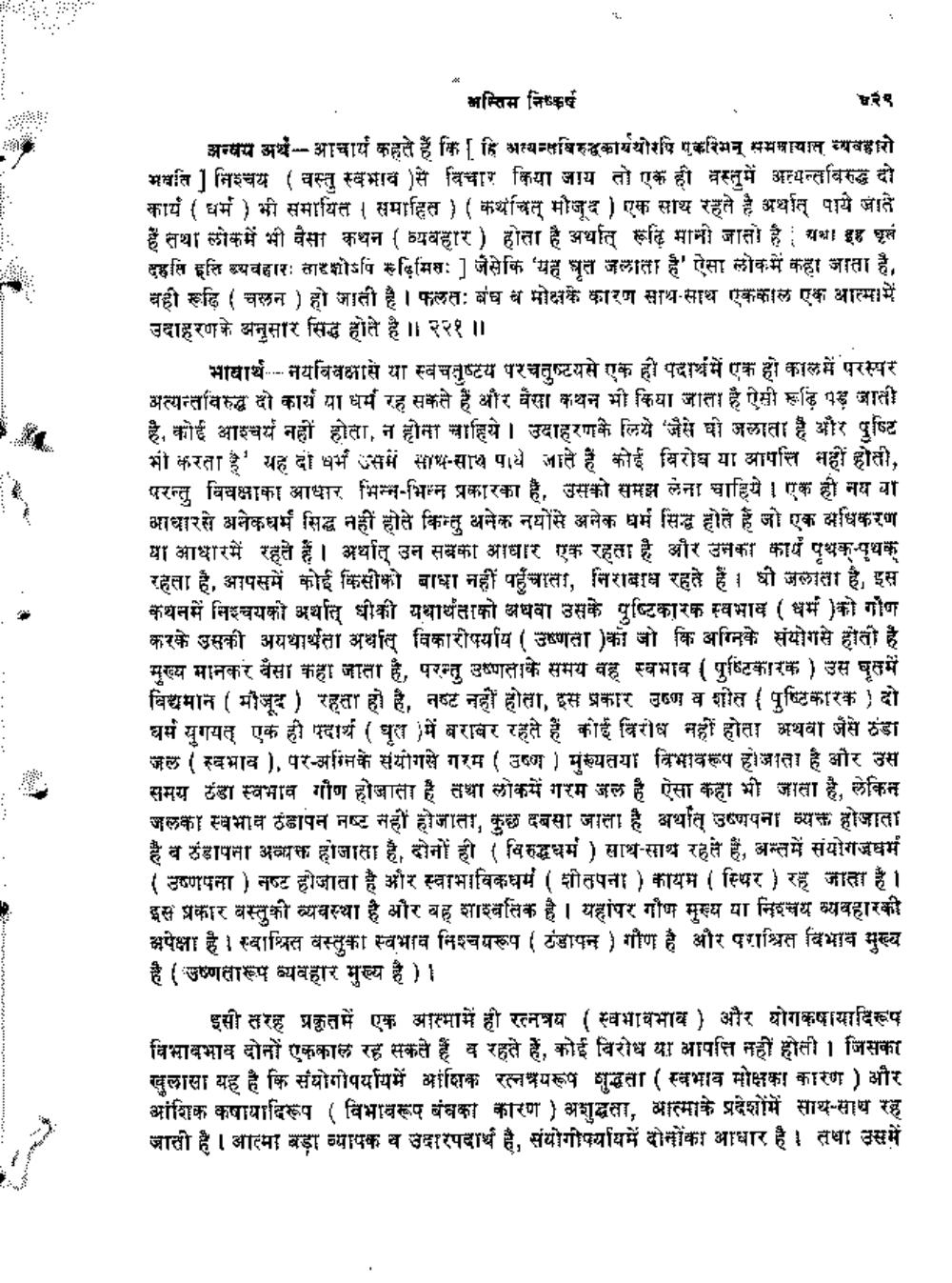________________
अन्तिम निष्कर्ष अन्वय अर्थ-- आचार्य कहते हैं कि [हि अत्यन्सविरुद्ध कार्ययोरपि परिमन् समन्त्रायात व्यवहारो भवति ] निश्चय ( वस्तु स्वभाव से विचार किया जाय तो एक ही वस्तुमें अत्यन्तविरुद्ध दो कार्य ( धर्म ) भी समायित्त । समाहित ) ( कचित् मौजूद ) एक साथ रहते है अर्थात् पाये जाते है तथा लोकमें भी वैसा कथन ( व्यवहार ) होता है अर्थात् रूदि मानी जातो है बचा इष्ट वृत्त दहप्ति इति व्यवहारः तारशोऽपि दिमित: ] जेसेकि 'यह घृत जलाता है' ऐसा लोक में कहा जाता है, वही रूढ़ि ( चलन ) हो जाती है । फलत: बंध च मोक्षके कारण साथ-साथ एककाल एक आत्मामें उदाहरण के अनुसार सिद्ध होते है ।। २२१॥
भावार्थ.--नयविवक्षासे या स्वचतुष्टय परचतुष्टयसे एक ही पदार्थ में एक हो काल में परस्पर अत्यन्तविरुद्ध दो कार्य या धर्म रह सकते हैं और वैसा कथन भी किया जाता है ऐसी हदि पड़ जाती है, कोई आश्चर्य नहीं होता, न होना चाहिये । उदाहरण के लिये 'जैसे घी जलाता है और पुष्टि भी करता है' यह दो धर्भ उसमें साथ-साथ पाये जाते हैं कोई विरोध या आपत्ति नहीं होती, परन्तु विषक्षाका आधार भिन्न-भिन्न प्रकारका है, उसको समझ लेना चाहिये । एक ही नय या आधारसे अनेकधर्म सिद्ध नहीं होते किन्तु अनेक नथोंसे अनेक धर्म सिद्ध होते हैं जो एक अधिकरण या आधारमें रहते हैं। अर्थात् उन सबका आधार एक रहता है और उनका कार्य पृथक्-पृथक रहता है, आपसमें कोई किसीको बाधा नहीं पहुंचाता, निराबाध रहते हैं। घी जलाता है, इस कथनमें निश्चयको अर्थात् धीकी यथार्थताको अधवा उसके पुष्टिकारक स्वभाव ( धर्म )को गौण करके उसकी अयथार्थता अर्थात् विकारीपर्याय ( उता )को जो कि अग्निके संयोगसे होती है मुख्य मानकर वैसा कहा जाता है, परन्तु उष्णताके समय वह स्वभाव ( पुष्टिकारक ) उस घृतमें विद्यमान ( मौजूद ) रहता हो है, नष्ट नहीं होता, इस प्रकार उष्ण व शीत { पुष्टिकारक ) दो धर्म युगयत् एक ही पदार्थ (घृत में बरावर रहते हैं कोई विरोध नहीं होता अथवा जैसे ठंडा जल ( स्वभाव ), पर-अग्निके संयोगसे गरम ( उष्ण ) मुख्यतया विभावरूप होजाता है और उस समय ठंडा स्वभाव गौण होजाता है तथा लोकमें गरम जल है ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन जलका स्वभाव ठंडापन नष्ट नहीं होजाता, कुछ दबसा जाता है अर्थात् उष्णपना व्यक्त होजाता है व ठंडापना अव्यक्त होजाता है, दोनों ही ( विरुद्धधर्म ) साथ-साथ रहते हैं, अन्त में संयोगजधर्म ( उष्णपना ) नष्ट होजाता है और स्वाभाविकधर्म ( शीतपना) कायम ( स्थिर ) रह जाता है। इस प्रकार वस्तुको व्यवस्था है और वह शाश्चतिक है। यहांपर गौण मुख्य या निश्चय व्यवहारकी अपेक्षा है । स्वाश्रित वस्तुका स्वभाव निश्चयरूप ( ठंडापन ) गौण है और पराश्रित विभाव मुख्य है ( उष्णतारूप व्यवहार मुख्य है)।
इसी तरह प्रकृतमें एक आस्मामें ही रत्नत्रय ( स्वभावभाव) और योगकषायादिरूप विभावभाव दोनों एककाल रह सकते हैं व रहते हैं, कोई विरोध या आपत्ति नहीं होती। जिसका खुलासा यह है कि संयोगोपर्यायमें आंशिक रत्नत्रयरूप शुद्धता ( स्वभाव मोक्षका कारण ) और आंशिक कषायादिरूप ( विभावरूप बंधका कारण ) अशुद्धता, आत्माके प्रदेशोंमें साथ-साथ रह जाती है । आत्मा बड़ा व्यापक व उदारपदार्थ है, संयोगीपर्यायमें दोनोंका आधार है । तथा उसमें