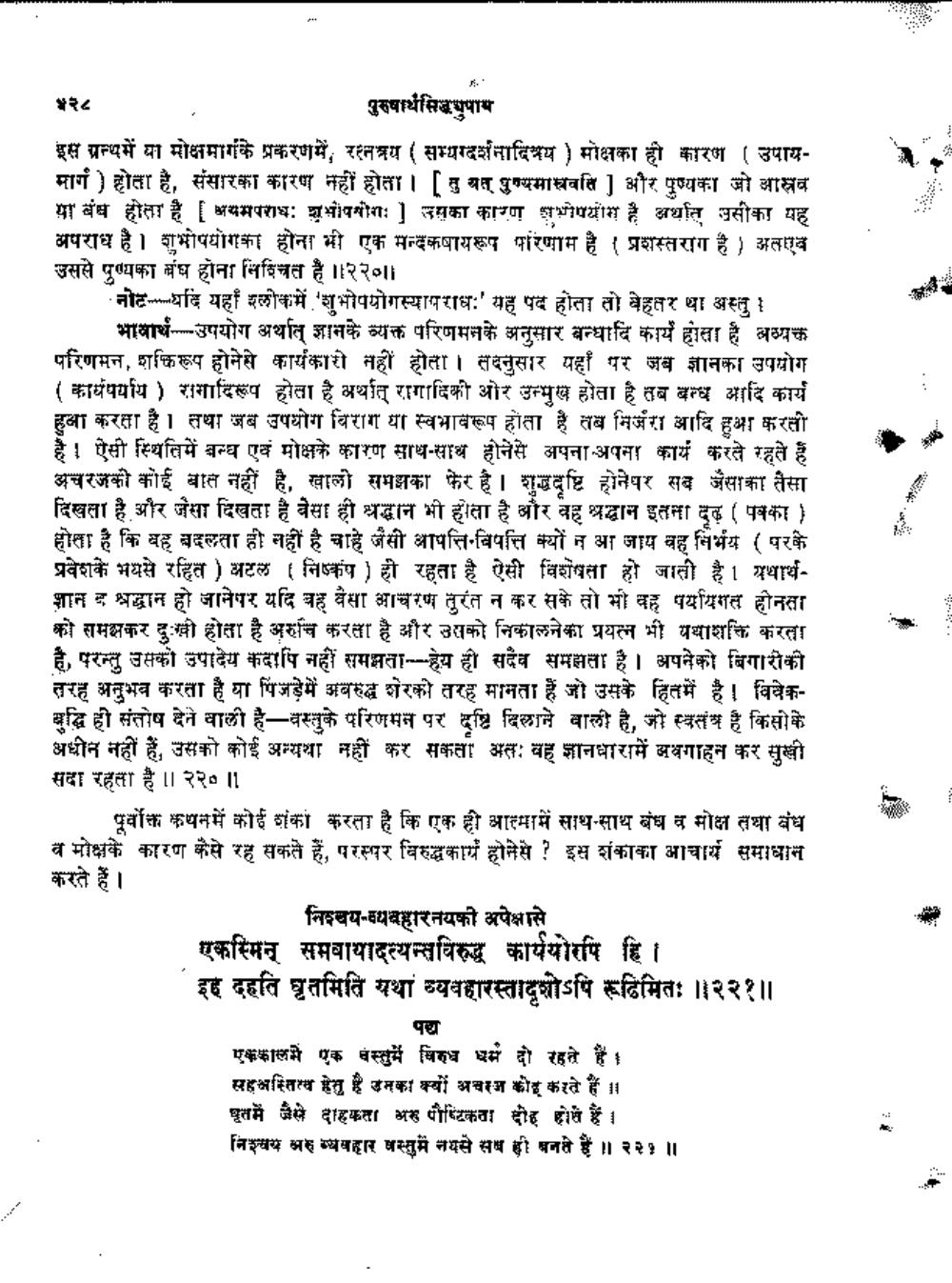________________
३२८
पुरुषार्थसिद्धधुपाय इस ग्रन्थमें या मोक्षमार्गके प्रकरणमें, रत्नत्रय ( सम्यग्दर्शनादिश्य ) मोक्षका ही कारण ( उपायमार्ग) होता है, संसारका कारण नहीं होता। [ तु यत् पुण्यमात्रवति ] और पुण्यका जो आस्रव या बंध होता है [ अयमपराध: शभापमोगः ] उसका कारण भोपयोग है अर्थात असीका यह अपराध है। शुभोपयोगका होना भी एक मन्दकषायरूप परिणाम है { प्रशस्तराग है । अतएव उससे पुण्यका बंध होना निश्चित है ।।२२०॥
नोट- यदि यहाँ श्लोको 'शुभोपयोगस्यागराधः' यह पद होता तो बेहतर था अस्तु ।
भावार्थ-उपयोग अर्थात् ज्ञानके व्यक्त परिणमनके अनुसार बन्धादि कार्य होता है अध्यक्त परिणमन, शक्तिरूप होनेसे कार्यकारी नहीं होता। तदनुसार यहाँ पर जब ज्ञानका उपयोग ( कार्यपर्याय ) रागादिरूप होता है अर्थात् रागादिकी ओर उन्मुख होता है तब बन्ध आदि कार्य हुआ करता है। तथा जब उपयोग विराग या स्वभावरूप होता है तब निर्जरा आदि हुआ करती है। ऐसी स्थितिमें बन्ध एवं मोक्षके कारण साथ-साथ होनेसे अपना अपना कार्य करते रहते हैं अचरजको कोई बात नहीं है, खाली समझका फेर है। शुद्धदृष्टि होनेपर सब जैसाका तैसा दिखता है और जैसा दिखता है वैसा ही श्रद्धान भी होता है और वह श्रद्धान इमादप
पक्का ) होता है कि वह बदलता ही नहीं है चाहे जैसी आपत्ति-विपत्ति क्यों न आ जाय वह निर्भय
(परके प्रवेशके भयसे रहित ) अटल (निष्कप) ही रहता है ऐसी विशेषता हो जाती है 1 यथार्थशानद श्रद्धान हो जानेपर यदि वह वैसा आचरण तुरंत न कर सके तो भी वह पर्यायगत होनसा को समझकर दुःखी होता है अरुचि करता है और उसको निकालनेका प्रयत्न भी यथाशक्ति करता है, परन्तु उसको उपादेय कदापि नहीं समझता--हेय ही सदैव समझता है। अपने को बिगारीकी तरह अनुभव करता है या पिंजड़ेमें अवरुद्ध शेरको तरह मानता हैं जो उसके हितमें है। विवेकबुद्धि ही संतोष देने वाली है-वस्तुके परिणमन पर दृष्टि दिलाने वाली है, जो स्वतंत्र हैं किसी के अधीन नहीं हैं, उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता अतः वह ज्ञानधासमें अवगाहन कर सुखी सदा रहता है ।। २२० ।।
पूर्वोक्त कथन में कोई शंका करता है कि एक ही आत्मामें साथ-साथ बंध व मोक्ष तथा बंध व मोक्षके कारण कैसे रह सकते हैं, परस्पर विरुद्धकार्य होनेसे ? इस शंकाका आचार्य समाधान करते हैं।
निश्चय-व्यवहारनयको अपेक्षासे एकस्मिन् समवायादत्यन्तविरुद्ध कार्ययोरपि हि । इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः ॥२२१।।
पद्य एककाल में एक वस्तु विरुध धर्म दो रहते है। सहअस्तित्व हेतु है उनका क्यों अचरज कोह करते हैं । धृत में जैसे दाहकता अरु पौष्टिकता दौह होते हैं। निश्चय अरु व्यवहार पस्सुमै नयसे सब ही बनते हैं॥२१॥