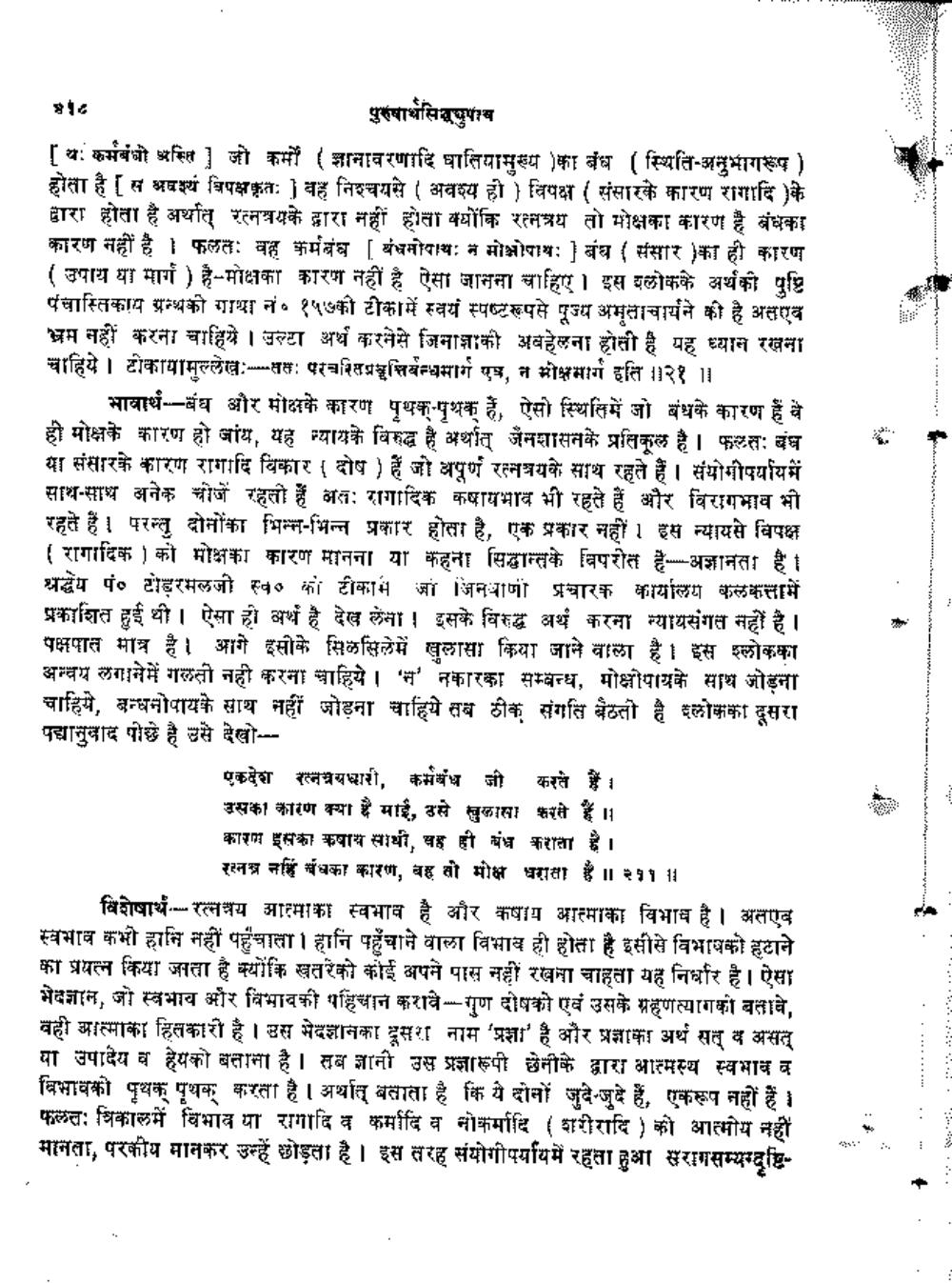________________
in-two
४१८
पुरुषार्थसिलघुपाय [यः कर्मबंधी अस्ति ] जो कर्मों ( ज्ञानावरणादि धातियामुख्य का बंध ( स्थिति-अनुभागरूप ) होता है [ स अवश्य विपक्षकृत: ] वह निश्चयसे । अवश्य ही विपक्ष ( संसारके कारण रागादि )के द्वारा होता है अर्थात् रत्नत्रयके द्वारा नहीं होता क्योंकि रत्नत्रय तो मोक्षका कारण है बंधका कारण नहीं है । फलतः वह कर्मबंध [ बंधमोपायः न मोनोपाथः ] बंध ( संसार का ही कारण ( उपाय या मार्ग) है-मोक्षका कारण नहीं है ऐसा जानना चाहिए। इस इलोकके अर्थकी पुष्टि पंचास्तिकाय ग्रन्थकी गाथा नं. १५७को टीकामें स्वयं स्पष्टरूपसे पूज्य अमृताचार्य ने की है अतएव भ्रम नहीं करना चाहिये । उल्टा अर्थ करनेसे जिनाज्ञाको अवहेलना होती है यह ध्यान रखना चाहिये। टीकायामुल्लेख :....-तत: परवरितप्रतिवन्धमार्ग एष, न मोक्षमार्ग इति ॥२१ ॥
भावार्थ-बंध और मोक्षके कारण पृथक्-पृथक हैं, ऐसी स्थितिमें जो बंधके कारण हैं वे ही मोक्षके कारण हो जाय, यह न्यायके विरुद्ध है अर्थात् जनशासनके प्रतिकूल है। फलतः बंध या संसारके कारण रागादि विकार { दोष ) हैं जो अपूर्ण रत्नत्रयके साथ रहते हैं । संयोगीपर्याय में साथ-साथ अनेक चीजें रहती हैं अतः रागादिक कषायभाव भी रहते हैं और विरागभाव भी रहते हैं। परन्तु दोनोंका भिन्न-भिन्न प्रकार होता है, एक प्रकार नहीं। इस न्यायसे विपक्ष { रागादिक ) को मोक्षका कारण मानना या कहना सिद्धान्तके विपरीत है...--अज्ञानता है। श्रद्धेय पं० टोडरमलजी स्व. को टीकाम जो जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्तामें प्रकाशित हुई थी। ऐसा ही अर्थ है देख लेगा। इसके विरुद्ध अर्थ करना न्यायसंगत नहीं है । पक्षपात मात्र है। आगे इसीके सिलसिले में खुलासा किया जाने वाला है। इस श्लोकका अन्वय लगाने में गलती नहीं करना चाहिये । 'न' नकारका सम्बन्ध, मोक्षोपायके साथ जोड़ना चाहिये, बन्धनोपायके साथ नहीं जोड़ना चाहिये सब ठीक संगति बैठती है इलोकका दूसरा पद्यानुवाद पोछे है उसे देखो---
एकदेश रत्ननमधारी, कर्मबंध जी करते हैं। उसका कारण क्या है माई, उसे खुलासा करते हैं । कारण इसका कषाय साधी, वह ही बंध कराता है।
रत्नन नहिं बंधका कारण, बह तो मोक्ष धरासा है ॥ २१ ॥ विशेषार्थ-- रत्नत्रय आत्माका स्वभाव है और कषाय आत्माका विभाष है। अतएव स्वभाव कभी हानि नहीं पहुंचाता हानि पहुँचाने वाला विभाव ही होता है इसीसे विभाषको हटाने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि खतरेको कोई अपने पास नहीं रखना चाहता यह निर्धार है। ऐसा भेदज्ञान, जो स्वभाव और विभावकी पहिचान करावे-गुण दोषको एवं उसके ग्रहणत्यागको बताचे, वही आत्माका हितकारी है । उस भेदज्ञानका दूसरा नाम 'प्रशा' है और प्रज्ञाका अर्थ सत् व असत् या उपादेय व हेयको बताना है । सब ज्ञानी उस प्रज्ञारूपी छेनीके द्वारा आत्मस्थ स्वभाव व विभावको पृथक् पृथक करता है । अर्थात् बताता है कि ये दोनों जुदे जुदे हैं, एकरूप नहीं हैं। फलतः त्रिकालमें विभाव या रागादि व कर्मादि व नोकर्मादि ( शरीरादि ) को आत्मीय नहीं मानता, परकीय मानकर उन्हें छोड़ता है। इस तरह संयोगीपर्यायमें रहता हुआ सरागसम्यग्दृष्टि