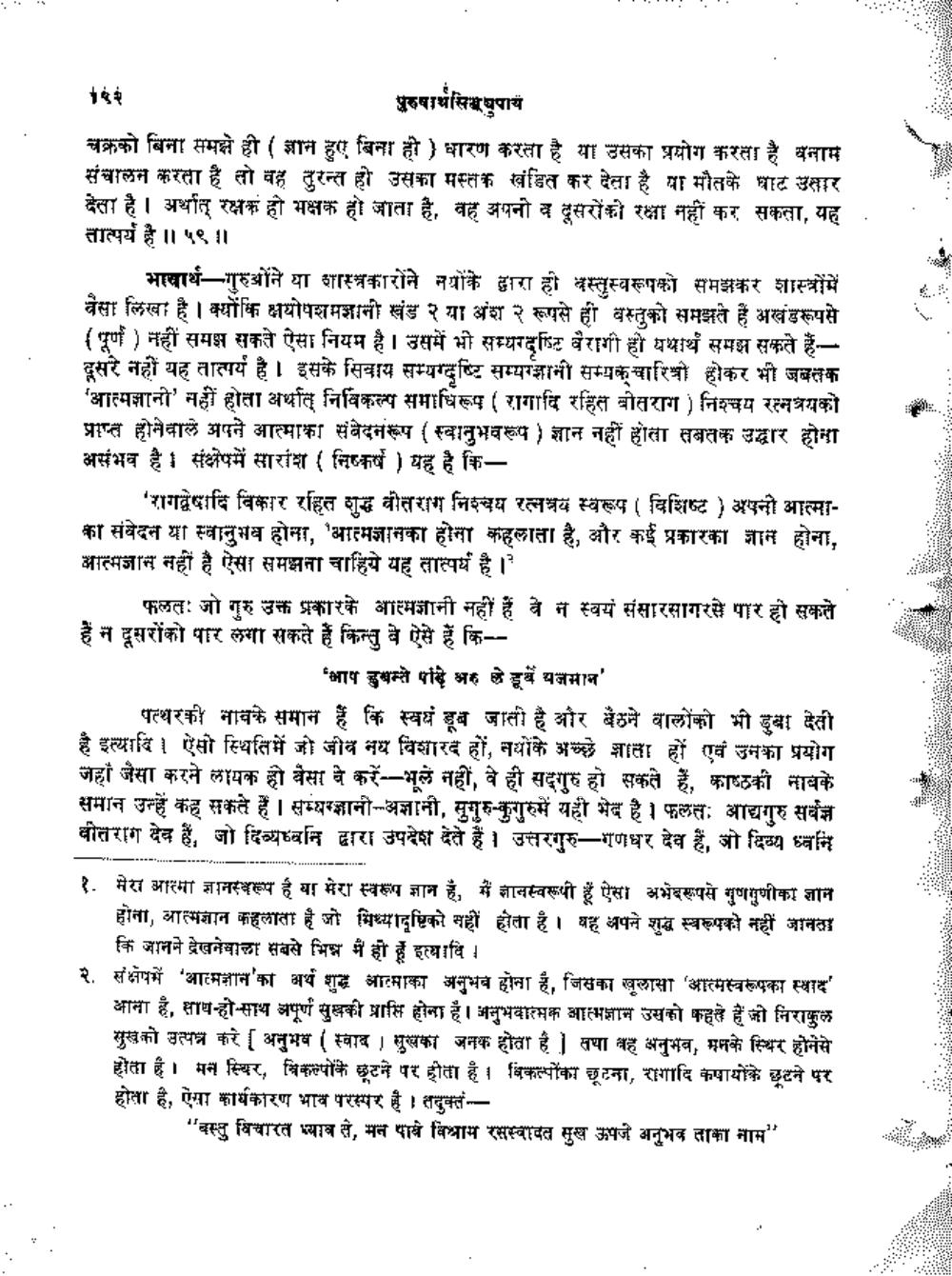________________
पुरुषार्थसिक्युपाय चक्रको बिना समझे ही ( ज्ञान हुए बिना हो ) धारण करता है या उसका प्रयोग करता है बनाम संचालन करता है तो वह तुरन्त हो उसका मस्तक खंडित कर देता है या मौतके घाट उतार देता है । अर्थात् रक्षक हो भक्षक हो जाता है, वह अपनी व दूसरोंको रक्षा नहीं कर सकता, यह तात्पर्य है ।। ५९ ॥
भावार्थ-गुरुओंने या शास्त्रकारोंने नयोंके द्वारा ही वस्तुस्वरूपको समझकर शास्त्रों में वैसा लिखा है। क्योंकि क्षयोपशमशानी खंड २ या अंश २ रूपसे ही बस्तुको समझते हैं अखंडरूपसे (पूर्ण) नहीं समझ सकते ऐसा नियम है। उसमें भी सम्यग्दष्टि वैरागी हो यथार्थ समझ सकते हैंदूसरे नहीं यह तात्पर्य है। इसके सिवाय सम्यग्दृष्टि सम्यग्ज्ञानी सम्यक् चारित्री होकर भी जबतक 'आत्मज्ञानी' नहीं होता अर्थात् निर्विकल्प समाधिरूप ( रागादि रहित बीतराग ) निश्चय रत्नत्रयको प्राप्त होनेवाले अपने आत्माका संबेदनरूप ( स्वानुभवरूप) ज्ञान नहीं होता सबतक उद्धार होना असंभव है। संक्षेपमें सारांश ( निष्कर्ष ) यह है कि
'रागद्वेषादि विकार रहित शुद्ध वीतराग निश्चय रत्नत्रय स्वरूप ( विशिष्ट ) अपनी आत्माका संवेदन या स्वानुभव होना, 'आत्मज्ञानका होना कहलाता है, और कई प्रकारका ज्ञान होना, आत्मज्ञान नहीं है ऐसा समझना चाहिये यह तात्पर्य है ।'
फलतः जो गुरु उक्त प्रकारके आत्मज्ञानी नहीं हैं वे न स्वयं संसारसागरसे पार हो सकते हैं न दूसरोंको पार लगा सकते हैं किन्तु वे ऐसे हैं कि--
'आप डुबन्ते पाड़े अरु ले डूबे यजमान' पत्थरकी नावके समान है कि स्वयं डूब जाती है और बैठने वालोंको भी डुबा देती है इत्यादि। ऐसो स्थितिमें जो जीव नय विशारद हों, नयोंके अच्छे ज्ञाता हों एवं उनका प्रयोग जहाँ जैसा करने लायक हो वैसा वे करें--भूले नहीं, वे ही सद्गुरू हो सकते हैं, काष्ठकी नाबके समान उन्हें कह सकते हैं । सम्यग्ज्ञानी--अज्ञानी, सुगुरु-कुगुरुमें यही भेद है। फलतः आद्यगुरु सर्वज्ञ वीतराग देव हैं, जो दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। उत्तरगुरु-गणधर देव हैं, जो दिव्य ध्वनि
१. मेरा आत्मा ज्ञानस्वरूप है या मेरा स्वरूप ज्ञान है, मैं ज्ञानस्वरूपी हूँ ऐसा अभेवरूपसे गुणगुणीका ज्ञान
होना, आत्मज्ञान कहलाता है जो मिथ्याष्टिको नहीं होता है। वह अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता
कि जानने देखनेवाला सबसे भिन्न में हो हूँ इत्यादि । २. संक्षेपमें 'आत्मज्ञान'का अर्थ शुद्ध आत्माका अनुभव होना है, जिसका खुलासा 'आत्मस्वरूपका स्वाद'
आना है, साथ हो-साथ अपूर्ण सुखकी प्राप्ति होना है। अनुभवात्मक आत्मज्ञान उसको कहते हैं जो निराकुल सुखको उत्पन्न करे [ अनुभव ( स्वाद । सुखका जनक होता है | सथा वह अनुभव, मनके स्थिर होनेसे होता है। मन स्थिर, विकल्पोंके छुटने पर होता है । विकल्पोंका छूटना, रागादि कषायोंके छूटने पर होता है, ऐसा कार्यकारण भाव परस्पर है । तदुक्तं--
"वस्तु विचारत भ्याव ते, मन पावे विश्राम रसस्वादत सुख ऊपजे अनुभव ताका नाम"