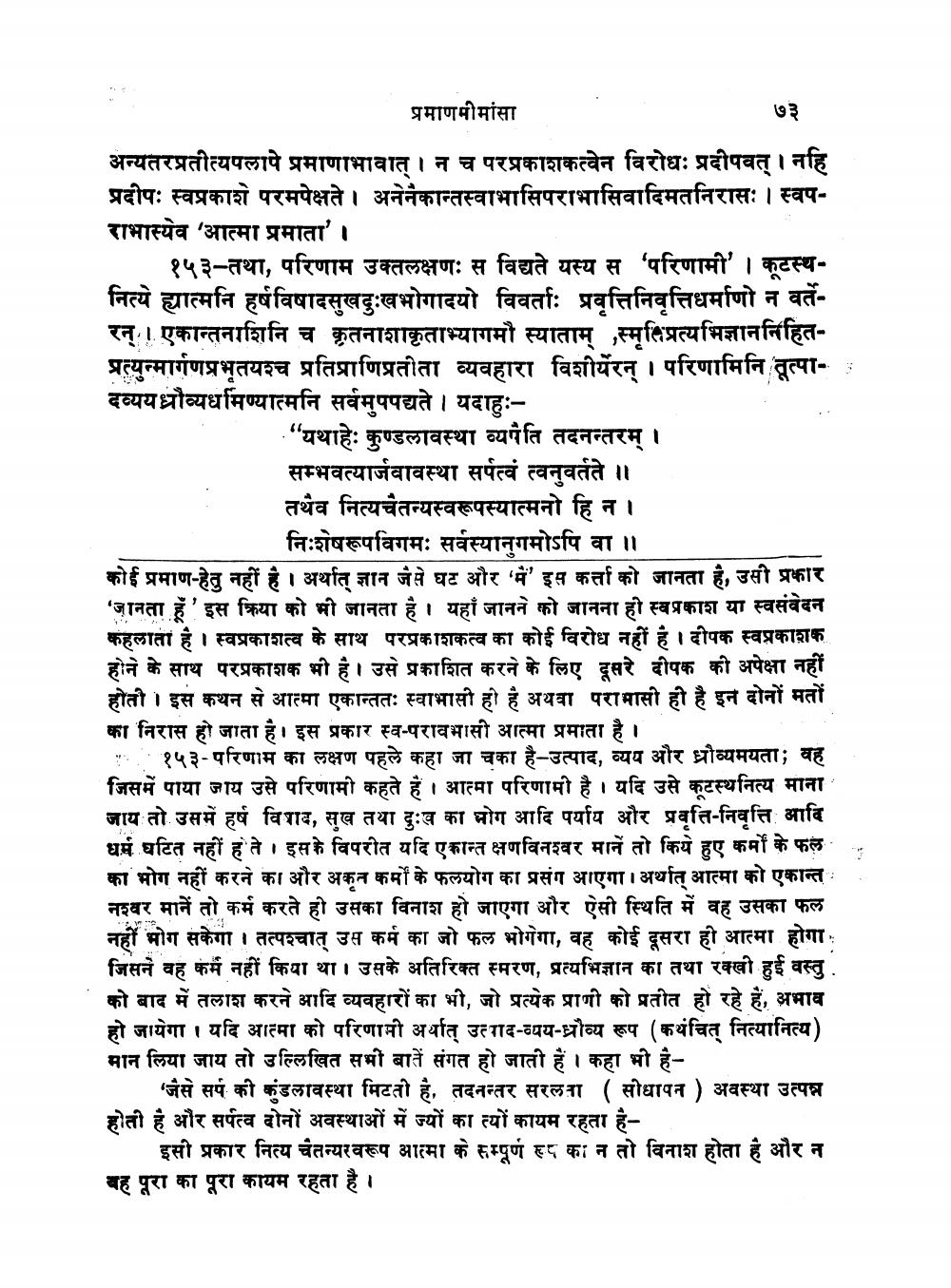________________
प्रमाणमीमांसा
अन्यतरप्रतीत्यपलापे प्रमाणाभावात् । न च परप्रकाशकत्वेन विरोधः प्रदीपवत् । नहि प्रदीपः स्वप्रकाशे परमपेक्षते। अनेनैकान्तस्वाभासिपराभासिवादिमतनिरासः । स्वपराभास्येव 'आत्मा प्रमाता'।
१५३-तथा, परिणाम उक्तलक्षणः स विद्यते यस्य स 'परिणामी' । कूटस्थनित्ये ह्यात्मनि हर्षविषादसुखदुःखभोगादयो विवर्ताः प्रवृत्तिनिवृत्तिधर्माणो न वर्तेरन् । एकान्तनाशिनि च कृतनाशाकृताभ्यागमौ स्याताम् ,स्मृतिप्रत्यभिज्ञाननिहितप्रत्युन्मार्गणप्रभृतयश्च प्रतिप्राणिप्रतीता व्यवहारा विशीरन् । परिणामिनि तूत्पा-: दव्ययध्रौव्यर्धामण्यात्मनि सर्वमुपपद्यते । यदाहुः
. “यथाहेः कुण्डलावस्था व्यपैति तदनन्तरम् ।
सम्भवत्यार्जवावस्था सर्पत्वं त्वनुवर्तते ॥ तथैव नित्यचैतन्यस्वरूपस्यात्मनो हि न ।
निःशेषरूपविगमः सर्वस्यानुगमोऽपि वा ॥ कोई प्रमाण-हेतु नहीं है । अर्थात् ज्ञान जैसे घट और 'मैं' इस कर्ता को जानता है, उसी प्रकार 'जानता हूँ' इस क्रिया को भी जानता है। यहाँ जानने को जानना ही स्वप्रकाश या स्वसंवेदन कहलाता है। स्वप्रकाशत्व के साथ परप्रकाशकत्व का कोई विरोध नहीं है । दीपक स्वप्रकाशक होने के साथ परप्रकाशक भी है। उसे प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीपक की अपेक्षा नहीं होती। इस कथन से आत्मा एकान्ततः स्वाभासी हो है अथवा परामासी ही है इन दोनों मतों का निरास हो जाता है। इस प्रकार स्व-परावभासी आत्मा प्रमाता है।
१५३- परिणाम का लक्षण पहले कहा जा चका है-उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यमयता; वह जिसमें पाया जाय उसे परिणामी कहते हैं । आत्मा परिणामी है । यदि उसे कूटस्थनित्य माना जाय तो उसमें हर्ष विशद, सुख तथा दुःख का भोग आदि पर्याय और प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि धर्म घटित नहीं होते। इसके विपरीत यदि एकान्त क्षणविनश्वर माने तो किये हुए कर्मों के फल का भोग नहीं करने का और अकृत कर्मों के फलयोग का प्रसंग आएगा। अर्थात् आत्मा को एकान्त नश्वर मानें तो कर्म करते हो उसका विनाश हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वह उसका फल नहीं भोग सकेगा। तत्पश्चात् उस कर्म का जो फल भोगेगा, वह कोई दूसरा ही आत्मा होगा: जिसने वह कर्म नहीं किया था। उसके अतिरिक्त स्मरण, प्रत्यभिज्ञान का तथा रक्खी हुई वस्तु . को बाद में तलाश करने आदि व्यवहारों का भी, जो प्रत्येक प्राणी को प्रतीत हो रहे हैं, अभाव हो जायेगा । यदि आत्मा को परिणामी अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप (कथंचित् नित्यानित्य) मान लिया जाय तो उल्लिखित सभी बातें संगत हो जाती हैं। कहा भी है_ 'जैसे सर्प की कुंडलावस्था मिटती है, तदनन्तर सरलता ( सीधापन ) अवस्था उत्पन्न होती है और सर्पत्व दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों कायम रहता है
इसी प्रकार नित्य चैतन्यरवरूप आत्मा के सम्पूर्ण रूप का न तो विनाश होता है और न वह पूरा का पूरा कायम रहता है ।