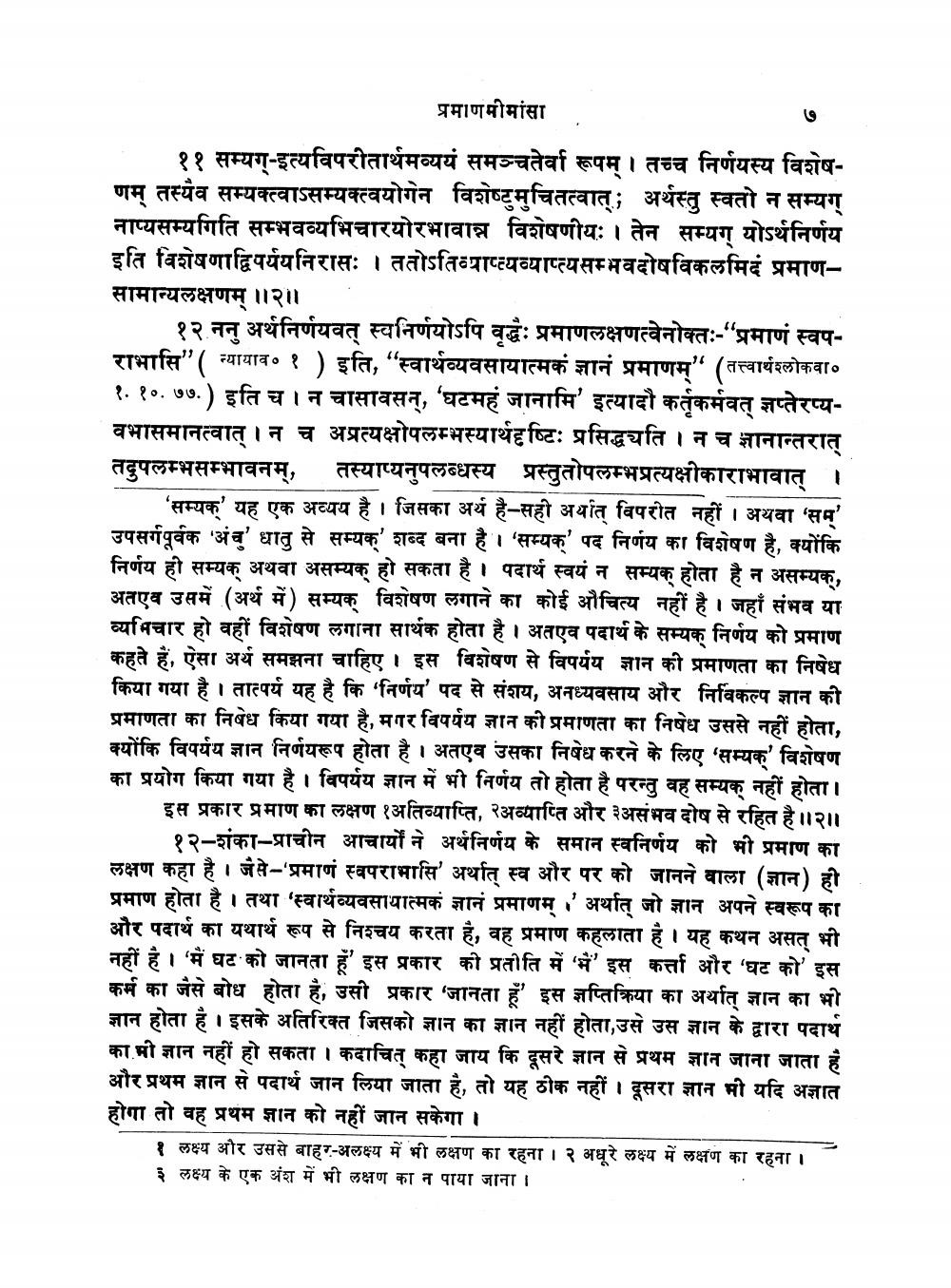________________
प्रमाणमीमांसा
७
११ सम्यग् - इत्यविपरीतार्थमव्ययं समञ्चतेर्वा रूपम् । तच्च निर्णयस्य विशेषणम् तस्यैव सम्यक्त्वाऽसम्यक्त्वयोगेन विशेष्टुमुचितत्वात् ; अर्थस्तु स्वतो न सम्यग् नाप्यसम्यगिति सम्भवव्यभिचारयोरभावान्न विशेषणीयः । तेन सम्यग् योऽर्थनिर्णय इति विशेषणाद्विपर्यय निरासः । ततोऽतिव्याप्त्यव्याप्त्यसम्भवदोषविकलमिदं प्रमाणसामान्यलक्षणम् ॥२॥
१२ ननु अर्थनिर्णयवत् स्वनिर्णयोऽपि वृद्धेः प्रमाणलक्षणत्वेनोक्तः- “प्रमाणं स्वपराभासि " ( न्यायाव ० १ ) इति, “स्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्" ( तत्त्वार्थश्लोकवा० १. १०. ७७ ) इति च । न चासावसन्, 'घटमहं जानामि' इत्यादौ कर्तृकर्मवत् ज्ञप्तेरप्यवभासमानत्वात् । न च अप्रत्यक्षोपलम्भस्यार्थदृष्टिः प्रसिद्धयति । न च ज्ञानान्तरात् तदुपलम्भसम्भावनम्, तस्याप्यनुपलब्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रत्यक्षीकाराभावात् ।
'सम्यक्' यह एक अव्यय है । जिसका अर्थ है - सही अर्थात् विपरीत नहीं । अथवा 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'अं' धातु से सम्यक्' शब्द बना है । 'सम्यक्' पद निर्णय का विशेषण है, क्योंकि निर्णय ही सम्यक् अथवा असम्यक् हो सकता है । पदार्थ स्वयं न सम्यक् होता है न असम्यक्, अतएव उसमें ( अर्थ में) सम्यक् विशेषण लगाने का कोई औचित्य नहीं है । जहाँ संभव या व्यभिचार हो वहीं विशेषण लगाना सार्थक होता है । अतएव पदार्थ के सम्यक् निर्णय को प्रमाण कहते हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए । इस विशेषण से विपर्यय ज्ञान की प्रमाणता का निषेध किया गया है । तात्पर्य यह है कि 'निर्णय' पद से संशय, अनध्यवसाय और निर्विकल्प ज्ञान की प्रमाणता का निषेध किया गया है, मगर विपर्यय ज्ञान की प्रमाणता का निषेध उससे नहीं होता, क्योंकि विपर्यय ज्ञान निर्णयरूप होता है । अतएव उसका निषेध करने के लिए 'सम्यक्' विशेषण का प्रयोग किया गया है। विपर्यय ज्ञान में भी निर्णय तो होता है परन्तु वह सम्यक् नहीं होता । इस प्रकार प्रमाण का लक्षण १ अतिव्याप्ति २अव्याप्ति और ३ असंभव दोष से रहित है ॥२॥ १२ - शंका - प्राचीन आचार्यों ने अर्थनिर्णय के समान स्वनिर्णय को भी प्रमाण का लक्षण कहा है। जैसे- 'प्रमाणं स्वपराभासि' अर्थात् स्व और पर को जानने वाला (ज्ञान) ही प्रमाण होता है । तथा 'स्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् । अर्थात् जो ज्ञान अपने स्वरूप का और पदार्थ का यथार्थ रूप से निश्चय करता है, वह प्रमाण कहलाता है । यह कथन असत् भी नहीं है । 'मैं घट को जानता हूँ' इस प्रकार की प्रतीति में 'मैं' इस कर्त्ता और 'घट को इस कर्म का जैसे बोध होता है, उसी प्रकार 'जानता हूँ' इस ज्ञप्तिक्रिया का अर्थात् ज्ञान का भी ज्ञान होता है । इसके अतिरिक्त जिसको ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, उसे उस ज्ञान के द्वारा पदार्थ का भी ज्ञान नहीं हो सकता । कदाचित् कहा जाय कि दूसरे ज्ञान से प्रथम ज्ञान जाना जाता है और प्रथम ज्ञान से पदार्थ जान लिया जाता है, तो यह ठीक नहीं। दूसरा ज्ञान भी यदि अज्ञात होगा तो वह प्रथम ज्ञान को नहीं जान सकेगा ।
१ लक्ष्य और उससे बाहर अलक्ष्य में भी लक्षण का रहना । २ अधूरे लक्ष्य में लक्षण का रहना । ३ लक्ष्य के एक अंश में भी लक्षण का न पाया जाना ।