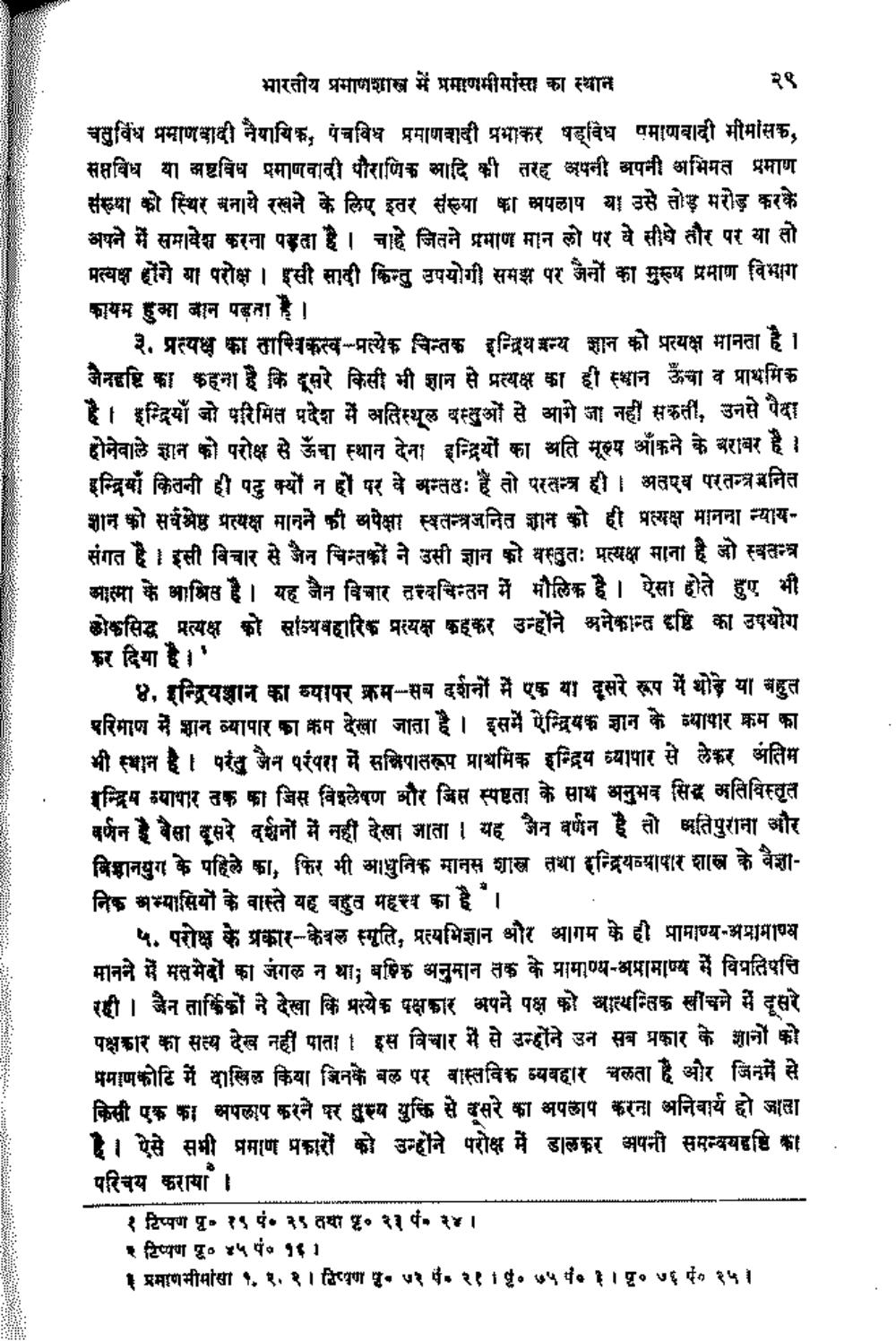________________
SHER
Mandalee
o minatilmm
a nsi
भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाणमीमांसा का स्थान चतुर्विध प्रमाणवादी नैयायिक, पंचविध प्रमाणवादी प्रभाकर षड्विध पमाणवादी मीमांसक, सप्तविध या अष्टविध प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी अपनी अभिमत प्रमाण संख्या को स्थिर बनाये रखने के लिए इतर संख्या का अपलाष या उसे तोड़ मरोड़ करके अपने में समावेश करना पड़ता है। चाहे जितने प्रमाण मान लो पर ये सीधे तौर पर या तो मत्यक्ष होंगे या परोक्ष । इसी सादी किन्तु उपयोगी समझ पर जैनों का मुख्य प्रमाण विभाग कायम हुमा जान पड़ता है।
३. प्रत्यक्ष का ताचिकत्व-प्रत्येक चिन्तक इन्द्रिय अन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है। अनदृष्टि का कहना है कि दूसरे किसी भी ज्ञान से प्रत्यक्ष का ही स्थान ऊँचा व प्राथमिक है। इन्द्रियाँ जो परिमित प्रदेश में अतिस्थूल वस्तुओं से आगे जा नहीं सकती, उनसे पैदा होनेवाले ज्ञान को परोक्ष से ऊँचा स्थान देना इन्द्रियों का अति मूल्य आँकने के बराबर है । इन्द्रियाँ कितनी ही पटु क्यों न हों पर वे अन्ततः है तो परतन्त्र ही। अतएव परतन्त्र अनित शान को सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष मानने की अपेक्षा स्वतन्त्रजनित ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना न्यायसंगत है। इसी विचार से जैन चिन्तकों ने उसी ज्ञान को वस्तुतः प्रत्यक्ष माना है जो स्वतन्त्र आत्मा के आश्रित है। यह जैन विचार तत्त्वचिन्तन में मौलिक है। ऐसा होते हुए भी छोकसिद्ध प्रत्यक्ष को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग कर दिया है।
१, इन्द्रियज्ञान का च्यापर क्रम-सब दर्शनों में एक या दूसरे रूप में थोड़े या बहुत परिमाण में शान व्यापार का कम देखा जाता है। इसमें ऐन्द्रियक ज्ञान के व्यापार क्रम का भी स्थान है। परंतु जैन परंपरा में सनिपातरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अंतिम इन्द्रिय व्यापार तक का जिस विश्लेषण और जिस स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध मतिविस्तृत वर्णन है वैसा दूसरे वचनों में नहीं देखा जाता । यह जैन वर्णन है तो अतिपुराना और विज्ञानयुग के पहिले का, फिर भी आधुनिक मानस शास्त्र तथा इन्द्रियव्यापार शास्त्र के वैज्ञानिक अभ्यासियों के वास्ते यह बहुत महत्त्व का है।
५. परोक्ष के प्रकार-केवल स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और आगम के ही प्रामाण्य-अप्रामाण्य मानने में मतभेदों का जंगल न था बक्षिक अनुमान तक के प्रामाण्य-अप्रामाण्य में विपतिपत्ति रही। जैन तार्किकों ने देखा कि प्रत्येक पक्षकार अपने पक्ष को प्रात्यन्तिक खींचने में दूसरे पक्षकार का सत्य देख नहीं पाता। इस विचार में से उन्होंने उन सब प्रकार के शानों को प्रमाणकोटि में दाखिल किया जिनके बल पर वास्तविक व्यवहार चलता है और जिनमें से किसी एक का अपलाप करने पर तुल्य युक्ति से दूसरे का अपलाप करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे सभी प्रमाण प्रकारों को उन्होंने परोक्ष में डालकर अपनी समन्वयदृष्टि का . परिचय कराया। १ टिप्पण पृ. १९५० २९ तथा पृ. २३६.२४ । शिप्पण पू० ४५पं. प्रमाणमीमांसा १.१.१ । विषण पु. ४२ पं. २१1० ४५० । पृ. ७६ पं० १५ ।
Ramdastishtatis
t
icat
ndianRaakhinditical