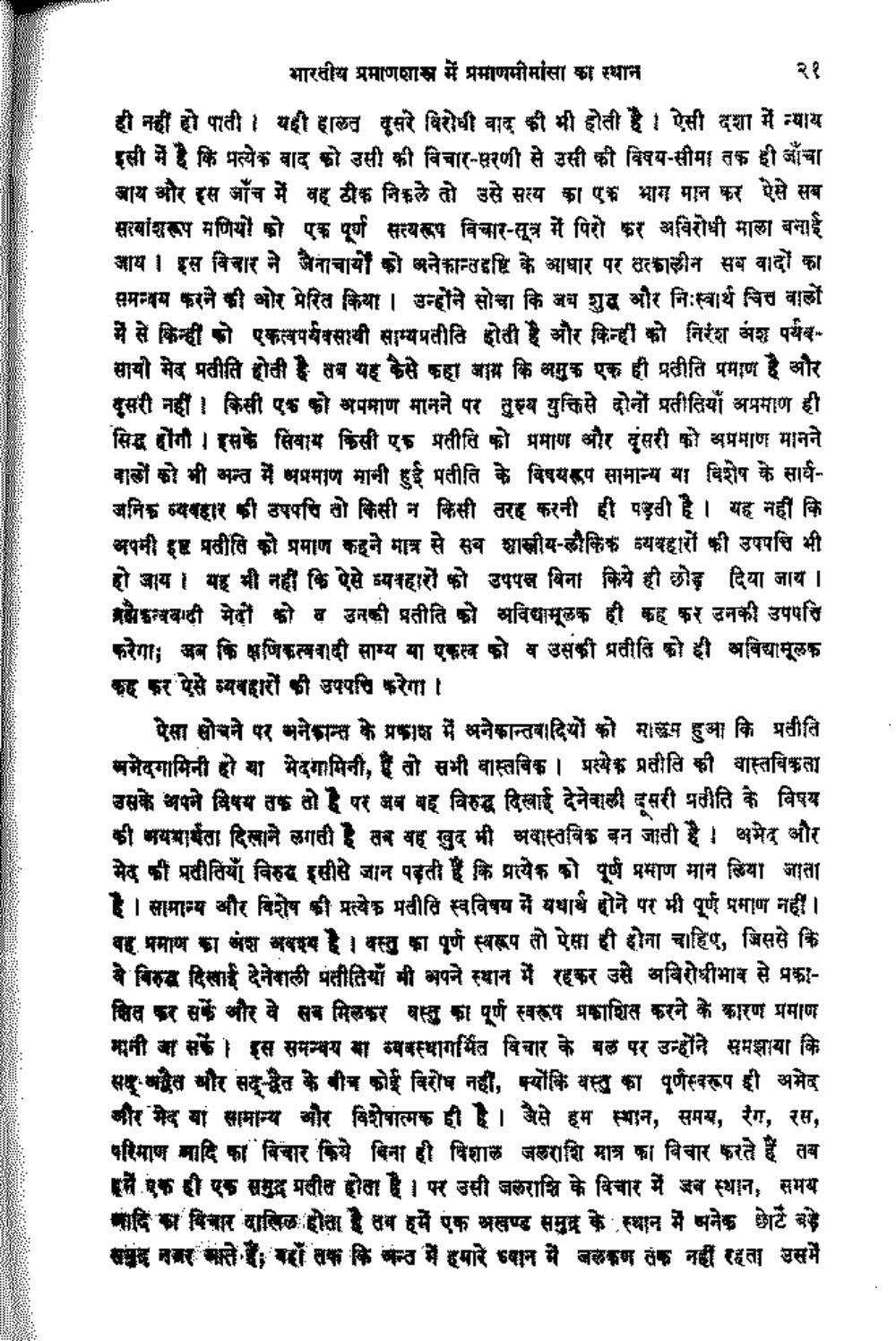________________
भारतीय प्रमाणशास्त्र में प्रमाणमीमांसा का स्थान
२१
ही नहीं हो पाती । यही हालत दूसरे विरोधी बाद की भी होती है। ऐसी दशा में न्याय इसी में है कि प्रत्येक वाद को उसी की विचारसरणी से उसी की विषय-सीमा तक ही जाँचा जय और इस आँच में वह ठीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मान कर ऐसे सब सरयांशरूप मणियों को एक पूर्ण सत्यरूप विचार सूत्र में पिरो कर अविरोधी माला बनाई जाय । इस विचार ने जैनाचार्यों को अनेकान्वष्टि के आधार पर तत्कालीन सब वादों का समन्वय करने की ओर प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि जब शुद्ध और निःस्वार्थ चिस वालों में से किन्हीं को एकत्वपर्यवसायी साम्यप्रतीति होती है और किन्हीं को निरंश अंश पर्यवसायी मेद प्रतीति होती है तब यह कैसे कहा जाय कि अमुक एक ही प्रतीति प्रमाण है और दूसरी नहीं किसी एक को अपमाण मानने पर तुझ्य युक्तिसे दोनों प्रतीतियाँ अप्रमाण ही सिद्ध होगी। इसके सिवाय किसी एक प्रतीति को प्रमाण और दूसरी को अप्रमाण मानने वालों को भी अन्त में प्रमाण मानी हुई प्रतीति के विषयरूप सामान्य या विशेष के सार्वafts व्यवहार की उपपत्ति तो किसी न किसी तरह करनी ही पड़ती है । यह नहीं कि अपनी इष्ट प्रतीति को प्रमाण कहने मात्र से सब शास्त्रीय लौकिक व्यवहारों की उपपत्ति भी हो जाय। यह भी नहीं कि ऐसे व्यवहारों को उपपत्र बिना किये ही छोड़ दिया जाय । मेदों को व उनकी प्रतीति को अविद्यामूलक ही कह कर उनकी उपपति करेगा जब कि क्षणिकत्ववादी साम्य या एकत्व को व उसकी प्रतीति को ही अविद्यामूलक कह कर ऐसे व्यवहारों की उपपति करेगा ।
ऐसा सोचने पर मनेकान्त के प्रकाश में अनेकान्तवादियों को मालूम हुआ कि प्रतीति ममेदगामिनी हो या भेदगामिनी, है तो सभी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता उसके अपने विषय तक तो है पर अब वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली दूसरी प्रतीति के विषय की ममता दिखाने लगती है तब यह खुद भी अवास्तविक बन जाती है। अमेद और मेद की प्रतीतियाँ विरुद्ध इसीसे जान पड़ती हैं कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है। सामान्य और विशेष की प्रत्येक मतीति स्वविषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नहीं । वह प्रमाण का अंश अवश्य है। वस्तु का पूर्ण स्वरूप तो ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि a fro दिखाई देनेवाली प्रतीतियाँ भी अपने स्थान में रहकर उसे अविरोधीभाव से प्रकाशिव कर सकें और वे सब मिलकर वस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण मानी जा सके। इस समभ्यय या व्यवस्थागर्मित विचार के बल पर उन्होंने समझाया कि स- द्वैत और सद्-द्वैत के बीच कोई विशेष नहीं, क्योंकि वस्तु का पूर्णस्वरूप ही अमे और मेद या सामान्य और विशेषात्मक दी है। जैसे हम स्थान, समय, रंग, रस, परिमाण नादि का विचार किये fear ft famाक जलराशि मात्र का विचार करते हैं तब एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है । पर उसी जलराशि के विचार में जब स्थान, समय नादि का विचार वालिल होता है तब हमें एक अखण्ड समुद्र के स्थान में अनेक छोटे बड़े नाते हैं यहाँ तक कि अन्त में हमारे sवान में जलकण तक नहीं रहता उसमें