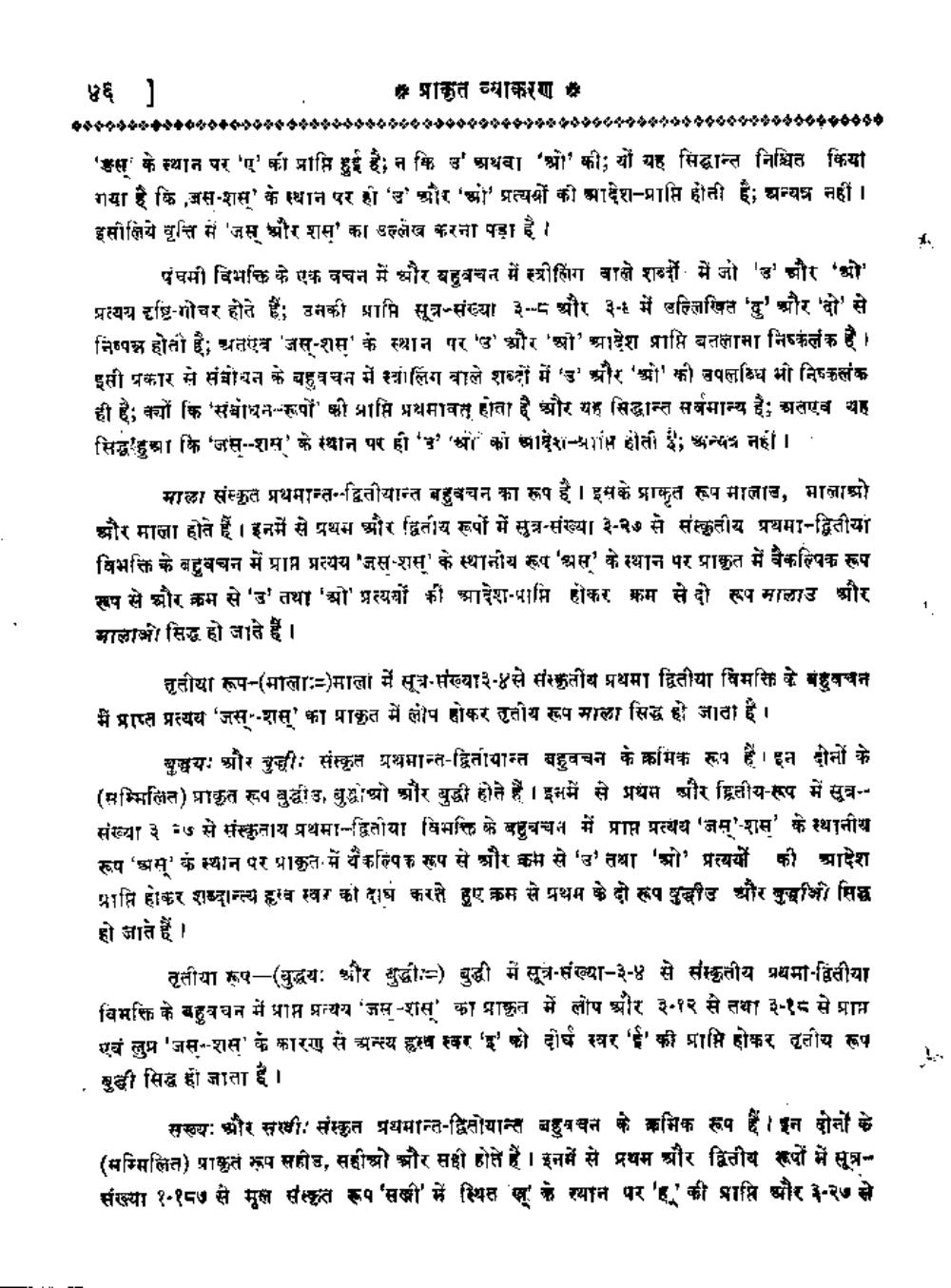________________
४६ ]
.प्राकृत व्याकरण
'स' के स्थान पर 'ए' की प्राप्ति हुई है न कि उ' अथवा 'श्री' की; यों यह सिद्धान्त निश्चित किया गया है कि ,जस-शस' के स्थान पर ही 'उ' और 'श्री' प्रत्ययों को आदेश-प्राप्ति होती है; अन्यत्र नहीं । इसीलिये वृत्ति में 'जम और शस' का उल्लेख करना पड़ा है।
पंचमी विभक्ति के एक वचन में और बहुवचन में स्त्रीलिंग वाले शब्दों में जो 'उ' और 'ओ' प्रत्यय दृष्टि-गोचर होते हैं; उनकी प्राप्ति सूत्र संख्या ३--- और ३-में उल्लिखित 'दु' और 'दो' से निष्पन्न होती है; अतएव 'जस्-शस' के स्थान पर 'उ' और 'ओ' आदेश प्राप्ति बतलामा निष्कलंक है। इसी प्रकार से संबोधन के बहुवचन में स्वालिंग वाले शब्दों में 'उ' और 'ओं' की उपलब्धि भी निष्कलंक ही है क्यों कि 'संबोधन रूपों' की प्राप्ति प्रथमावत होता है और यह सिद्धान्त सर्वमान्य है; अतएव यह सिद्धहुना कि 'जस--शम' के स्थान पर ही '' 'श्री को प्रादेश-प्रांत होती है; अन्यत्र नहीं। .
माला संस्कृत प्रथमान्त-द्वितीयान्त बहुवचन का रूप है । इसके प्राकृत रूप मालाज, मालामो और माला होते हैं । इनमें से प्रथम और द्वितीय रूपों में सुत्र-संख्या ३-२७ से संस्कृतीय प्रथमा-द्वितीया विभक्ति के बटुवचन में प्रान प्रत्यय 'जस-शस्' के स्थानीय रूप 'श्रम' के स्थान पर प्राकृत में वैकल्पिक रूप रूप से और कम से 'उ' तथा 'ओ' प्रत्ययों की आदेश-प्राप्ति होकर फ्रम से दो रूप मालाउ और मालाओ सिद्ध हो जाते हैं।
तृतीया रूप-(माला:-)माला में सूत्र संख्या३-४से संस्कृतीय प्रथमा द्वितीया विमति के बहुवचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस् -शस्' का प्राकृत में लोप होकर तृतीय रूप माला सिद्ध हो जाता है।
शुद्धयः और बुद्धी: संस्कृत प्रथमान्त-द्वितीयान्त बहुवचन के क्रमिक रूप है। इन दोनों के (सम्मिलित) प्राकृत रूप बुद्धीउ, बुद्धोश्रो और बुद्धी होते हैं । इनमें से प्रथम और द्वितीय-रूप में सूत्र-- संख्या ३ ७ से संस्कृताय प्रथमा-द्वितीया विभक्ति के बटुवचन में प्राप्त प्रत्यय 'जम्'-शस' के स्थानीय रूप 'श्रम' के स्थान पर प्राकृत में यकल्पिक रूप से और कम से 'उ' तथा 'ओ' प्रत्ययों की प्रादेश प्राप्ति होकर शब्दान्त्य हरव स्वर को दाध करते हुए क्रम से प्रथम के दो रूप पुछीउ और बुद्धीभी सिद्ध हो जाते हैं।
तृतीया रूप-(बुद्धयः और युद्धी:-) बुद्धी में सूत्र-संख्या-३-४ से संस्कृतीय प्रथमा-द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में प्राप्त प्रत्यय 'जस-शस्' का प्राकृत में लोप श्रीर ३.१२ से तथा ३-१८ से प्राप्त एवं लुप्र 'जस--शस' के कारण से अन्स्य ह्रस्व स्वर 'इ' को दीर्घ स्वर 'ई' की प्राप्ति होकर तृतीय रूप बुद्धी सिद्ध हो जाता है।
सख्यः और सरवी: संस्कृत प्रथमान्त-द्वितोयान्त बहुवचन के क्रमिक रूप हैं। इन दोनों के (मम्मिलित) प्राकृत रूप सहीउ, सहीअो और सही होते हैं । इनमें से प्रथम और वित्तीय रूपों में सूत्रसंख्या १.१८७ से मुल संस्कृत रूप 'सखी' में स्थित ' के रयान पर 'ह' की प्राप्ति और ३२७ से