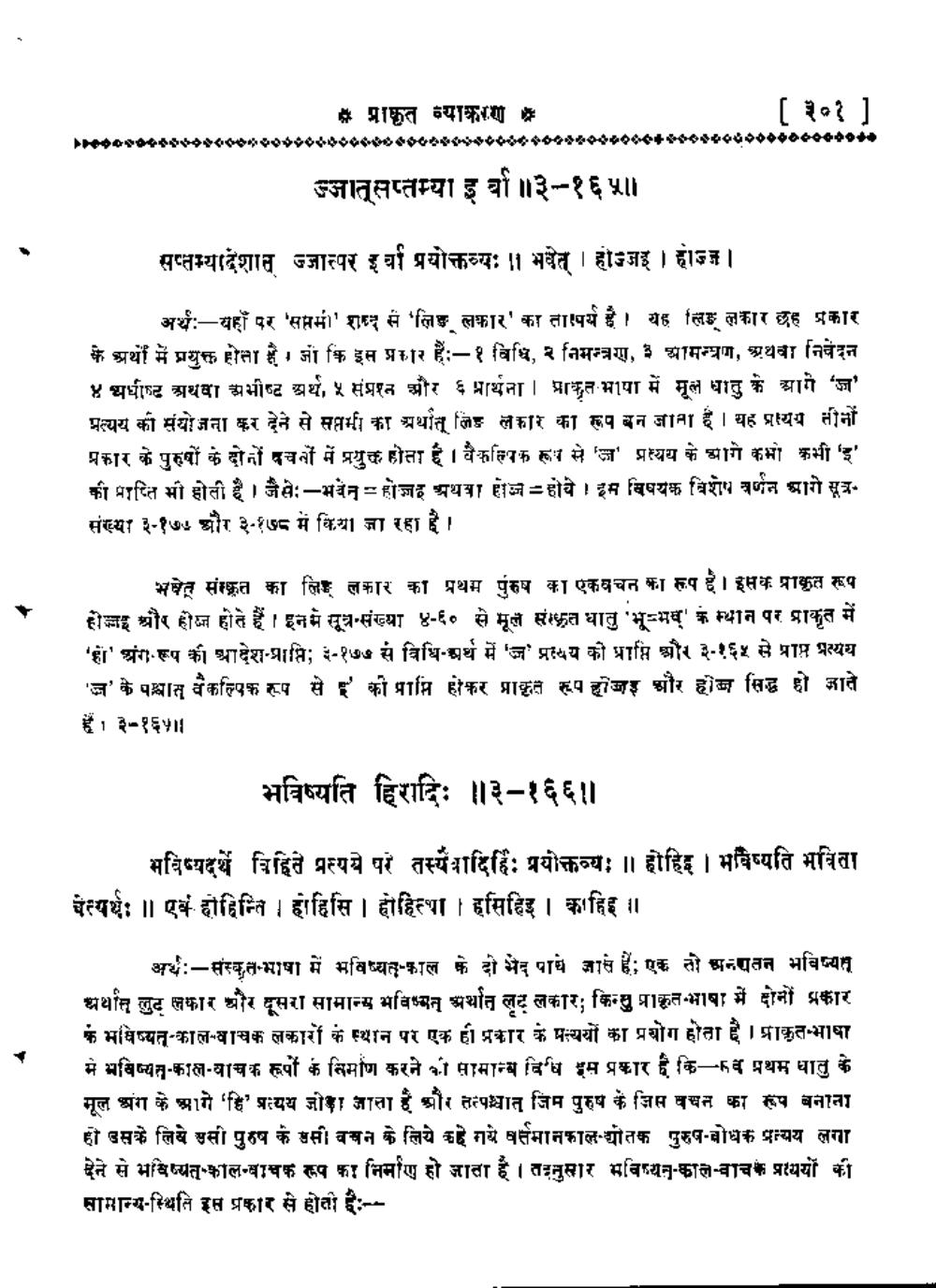________________
* प्राकृत व्याकरण * $60000000000066004
ज्जात्सप्तम्या इव ॥ ३--१६५ ॥
[ ३०१ ]
-
0000
सप्तभ्यादेशात् ज्जात्पर इर्घा प्रयोक्तव्यः || भवेत् । होज्जइ । होज्ज |
•
4
अर्थः- यहाँ पर 'सप्तमी' शब्द से 'लिङ लकार' का तापर्य है । यह लिङ् लकार छह प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होता है जो कि इस प्रकार हैं:- १ विधि, २ निमन्त्रण, ३ आमन्त्रण अथवा निवेदन ४ अर्धष्ट अथवा अभीष्ट अर्थ, ५ संप्रश्न और ६ प्रार्थना प्राकृत भाषा में मूल धातु के आगे 'ज' प्रत्यय की संयोजना कर देने से सप्तमी का अर्थात् लिङ लकार का रूप बन जाता है। यह प्रत्यय तीनों प्रकार के पुरुषों के दोनों वचनों में प्रयुक्त होता है। वैकल्पिक रूप से 'ज' प्रत्यय के आगे कभी कभी 'इ' की प्राप्ति भी होती हैं । जैसे:- भवेन होज अथवा होज होये । इस विषयक विशेष वर्णन आगे सूत्रसंख्या ३-१७७ और ३-१७८ में किया जा रहा है।
=
भषेत संस्कृत का लिङ्ग लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन का रूप है। इसक प्राकृत रूप हो और होन होते हैं। इनमें सूत्र संख्या ४-६० से मूल संस्कृत धातु 'भू भव्' के स्थान पर प्राकृत में 'हो' अंग-रूप की श्रादेश प्राप्ति; ३ १७७ से विधि अर्थ में 'ज' प्रत्यय की प्राप्ति और ३-१६५ से प्राप्त प्रत्यय 'ज' के पश्चात् वैकल्पिक रूप से ६ की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप होजई और होन सिद्ध हो जाते
हूँ । ३-१६५ ।।
भविष्यति हिरादिः ॥३ - १६६॥
भविष्यदर्थे चिह्निते प्रत्यये परं तस्यैवादिहिः प्रयोक्तव्यः || होहि । भविष्यति भविता त्यर्थः ॥ एवं होति । होहिसि । होहित्था | इसिहि । काहि ||
अर्थ :- संस्कृत भाषा में भविष्यत् काल के दो भेद पाये जाते हैं; एक तो अन्यतन भविष्यत् अर्थात लुट् लकार और दूसरा सामान्य भविष्यत् अर्थात लृट् लकार; किन्तु प्राकृत भाषा में दोनों प्रकार कं भविष्यत् काल वाचक लकारों के स्थान पर एक ही प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग होता है । प्राकृत भाषा
भविष्यकाल वाचक रूपों के निर्माण करने की सामान्य विधि इस प्रकार है कि प्रथम धातु के मूल अंग के आगे 'हि' प्रत्यय जोड़ा जाता है और तत्पश्चात् जिम पुरुष के जिस वचन का रूप बनाना हो उसके लिये उसी पुरुष के उसी वचन के लिये कहे गये वर्तमानकाल- द्योतक पुरुष बोधक प्रत्यय लगा देने से भविष्यत् काल वाचक रूप का निर्माण हो जाता है। तदनुसार भविष्यन काल वाचक प्रत्ययों की सामान्य स्थिति इस प्रकार से होती है:--