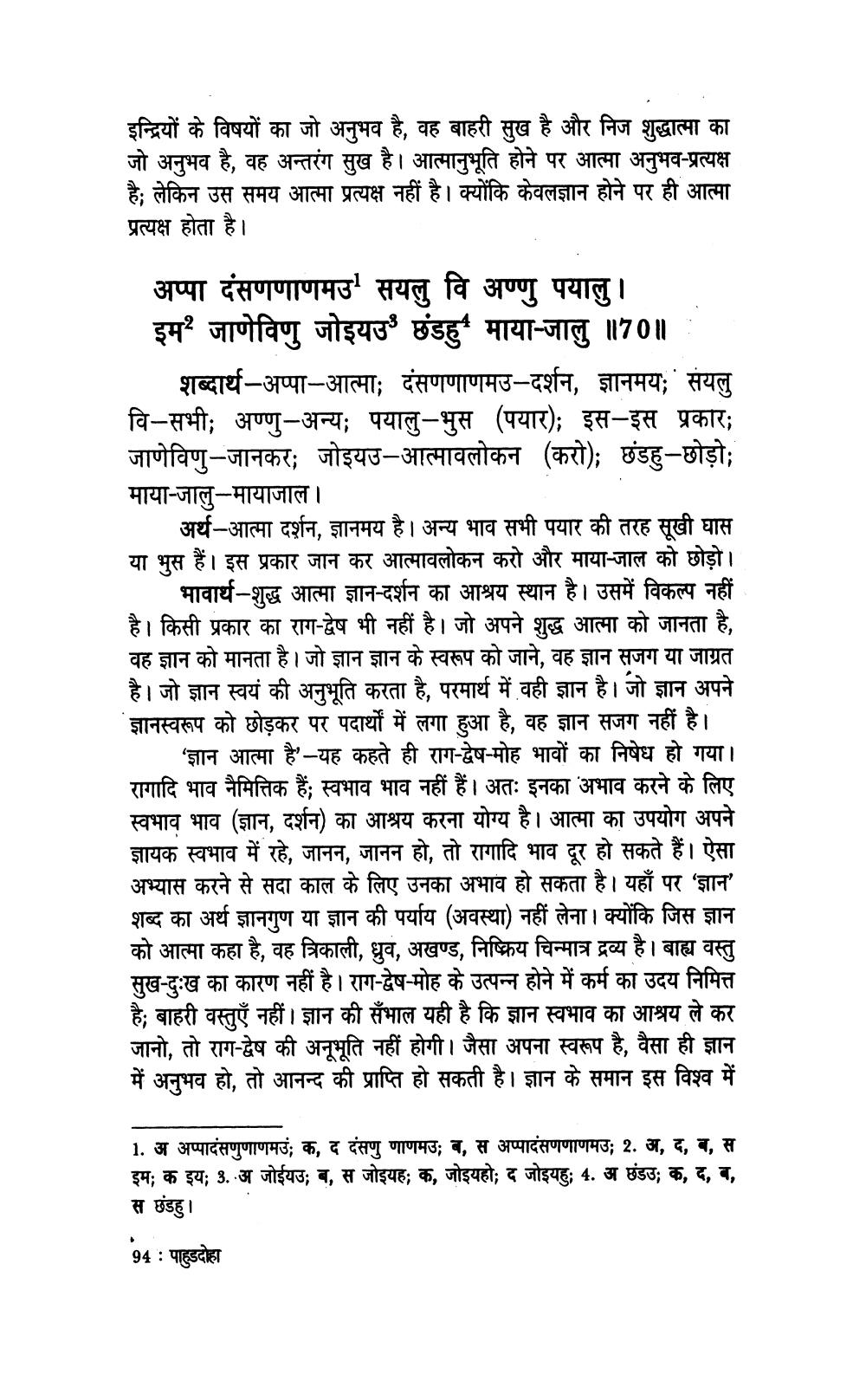________________
इन्द्रियों के विषयों का जो अनुभव है, वह बाहरी सुख है और निज शुद्धात्मा का जो अनुभव है, वह अन्तरंग सुख है। आत्मानुभूति होने पर आत्मा अनुभव-प्रत्यक्ष है; लेकिन उस समय आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। क्योंकि केवलज्ञान होने पर ही आत्मा प्रत्यक्ष होता है।
अप्पा दंसणणाणमउ सयलु वि अण्णु पयालु। इम जाणेविणु जोइयउ ठंडहु माया-जालु ॥70॥
शब्दार्थ-अप्पा-आत्मा; दंसणणाणमउ-दर्शन, ज्ञानमय; संयलु वि-सभी; अण्णु-अन्य; पयालु-भुस (पयार); इस-इस प्रकार; जाणेविणु-जानकर; जोइयउ-आत्मावलोकन (करो); छंडहु-छोड़ो; माया-जालु-मायाजाल। ___अर्थ-आत्मा दर्शन, ज्ञानमय है। अन्य भाव सभी पयार की तरह सूखी घास या भुस हैं। इस प्रकार जान कर आत्मावलोकन करो और माया-जाल को छोड़ो।
भावार्थ-शुद्ध आत्मा ज्ञान-दर्शन का आश्रय स्थान है। उसमें विकल्प नहीं है। किसी प्रकार का राग-द्वेष भी नहीं है। जो अपने शुद्ध आत्मा को जानता है, वह ज्ञान को मानता है। जो ज्ञान ज्ञान के स्वरूप को जाने, वह ज्ञान सजग या जाग्रत है। जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति करता है, परमार्थ में वही ज्ञान है। जो ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूप को छोड़कर पर पदार्थों में लगा हुआ है, वह ज्ञान सजग नहीं है।
___'ज्ञान आत्मा है'-यह कहते ही राग-द्वेष-मोह भावों का निषेध हो गया। रागादि भाव नैमित्तिक हैं; स्वभाव भाव नहीं हैं। अतः इनका अभाव करने के लिए स्वभाव भाव (ज्ञान, दर्शन) का आश्रय करना योग्य है। आत्मा का उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव में रहे, जानन, जानन हो, तो रागादि भाव दूर हो सकते हैं। ऐसा अभ्यास करने से सदा काल के लिए उनका अभाव हो सकता है। यहाँ पर 'ज्ञान' शब्द का अर्थ ज्ञानगुण या ज्ञान की पर्याय (अवस्था) नहीं लेना। क्योंकि जिस ज्ञान को आत्मा कहा है, वह त्रिकाली, ध्रुव, अखण्ड, निष्क्रिय चिन्मात्र द्रव्य है। बाह्य वस्तु सुख-दुःख का कारण नहीं है। राग-द्वेष-मोह के उत्पन्न होने में कर्म का उदय निमित्त है; बाहरी वस्तुएँ नहीं। ज्ञान की सँभाल यही है कि ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले कर जानो, तो राग-द्वेष की अनूभूति नहीं होगी। जैसा अपना स्वरूप है, वैसा ही ज्ञान में अनुभव हो, तो आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान के समान इस विश्व में
1. अ अप्पासणुणाणमउं; क, द दंसणु णाणमउ; ब, स अप्पादंसणणाणमउ; 2. अ, द, ब, स इम; क इय; 3. अ जोईयउ; ब, स जोइयह; क, जोइयहो; द जोइयहु; 4. अ छंडउ; क, द, ब, स छंडहु।
94 : पाहुडदोहा