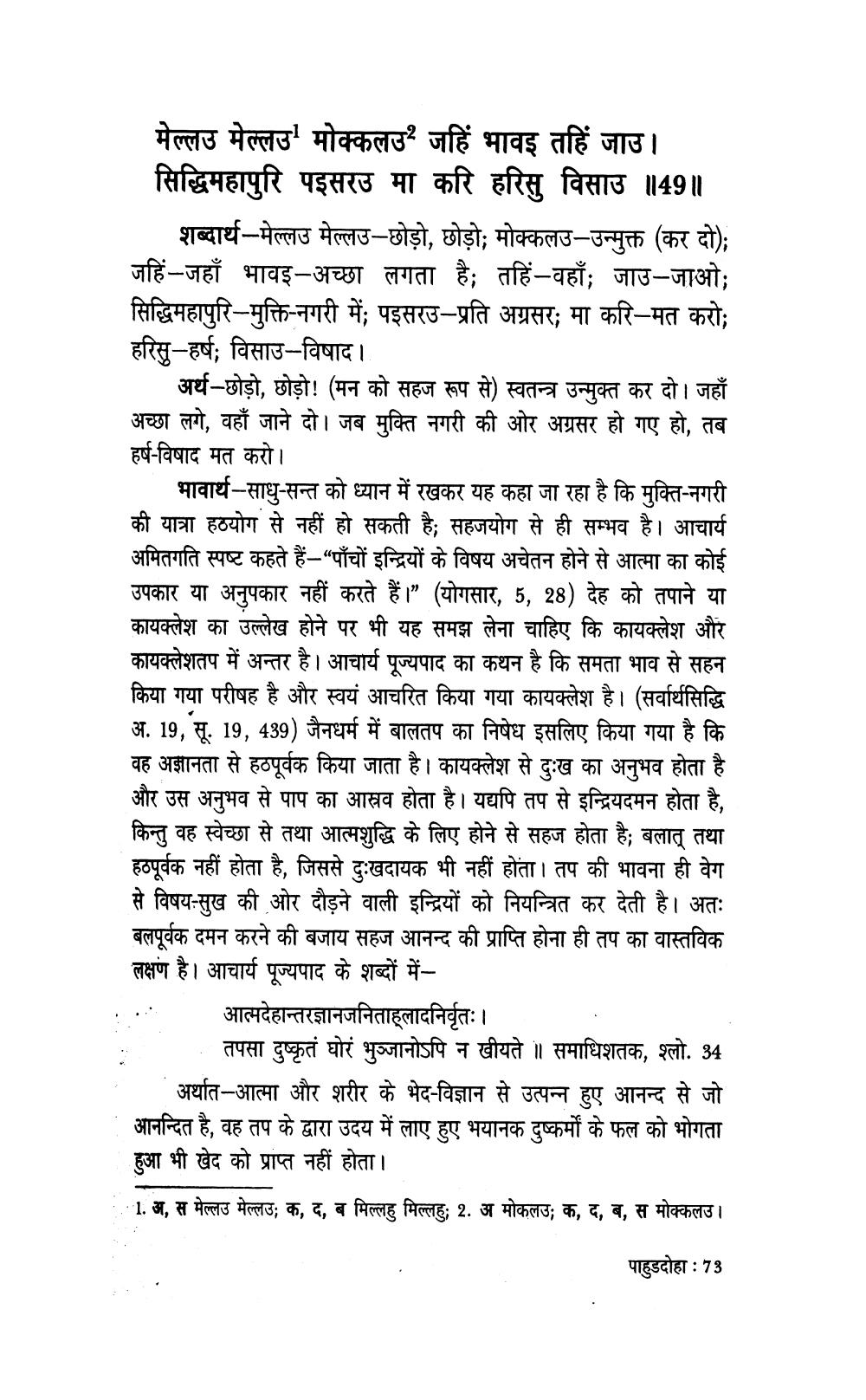________________
मेल्लउ मेल्लउ' मोक्कलउ जहिं भावइ तहिं जाउ। सिद्धिमहापुरि पइसरउ मा करि हरिसु विसाउ ॥49॥
शब्दार्थ-मेल्लउ मेल्लउ-छोड़ो, छोड़ो; मोक्कलउ-उन्मुक्त (कर दो); जहिं-जहाँ भावइ-अच्छा लगता है; तहिं-वहाँ; जाउ-जाओ; सिद्धिमहापुरि-मुक्ति-नगरी में; पइसरउ-प्रति अग्रसर; मा करि-मत करो; हरिसु-हर्ष; विसाउ-विषाद।
अर्थ-छोड़ो, छोड़ो! (मन को सहज रूप से) स्वतन्त्र उन्मुक्त कर दो। जहाँ अच्छा लगे, वहाँ जाने दो। जब मुक्ति नगरी की ओर अग्रसर हो गए हो, तब हर्ष-विषाद मत करो।
भावार्थ-साधु-सन्त को ध्यान में रखकर यह कहा जा रहा है कि मुक्ति-नगरी की यात्रा हठयोग से नहीं हो सकती है; सहजयोग से ही सम्भव है। आचार्य अमितगति स्पष्ट कहते हैं- “पाँचों इन्द्रियों के विषय अचेतन होने से आत्मा का कोई उपकार या अनुपकार नहीं करते हैं।” (योगसार, 5, 28) देह को तपाने या कायक्लेश का उल्लेख होने पर भी यह समझ लेना चाहिए कि कायक्लेश और कायक्लेशतप में अन्तर है। आचार्य पूज्यपाद का कथन है कि समता भाव से सहन किया गया परीषह है और स्वयं आचरित किया गया कायक्लेश है। (सर्वार्थसिद्धि अ. 19, सू. 19, 439) जैनधर्म में बालतप का निषेध इसलिए किया गया है कि वह अज्ञानता से हठपूर्वक किया जाता है। कायक्लेश से दुःख का अनुभव होता है
और उस अनुभव से पाप का आस्रव होता है। यद्यपि तप से इन्द्रियदमन होता है, किन्तु वह स्वेच्छा से तथा आत्मशुद्धि के लिए होने से सहज होता है; बलात् तथा हठपूर्वक नहीं होता है, जिससे दुःखदायक भी नहीं होता। तप की भावना ही वेग से विषय-सुख की ओर दौड़ने वाली इन्द्रियों को नियन्त्रित कर देती है। अतः बलपूर्वक दमन करने की बजाय सहज आनन्द की प्राप्ति होना ही तप का वास्तविक लक्षण है। आचार्य पूज्यपाद के शब्दों में
आत्मदेहान्तरज्ञानजनितालादनिर्वृतः।। - तपसा दुष्कृतं घोरं भुजानोऽपि न खीयते ॥ समाधिशतक, श्लो. 34 अर्थात-आत्मा और शरीर के भेद-विज्ञान से उत्पन्न हुए आनन्द से जो आनन्दित है, वह तप के द्वारा उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। - 1. अ, स मेल्लउ मेल्लउ; क, द, ब मिल्लहु मिल्लहु; 2. अ मोकलउ; क, द, ब, स मोक्कलउ।
पाहुडदोहा : 73