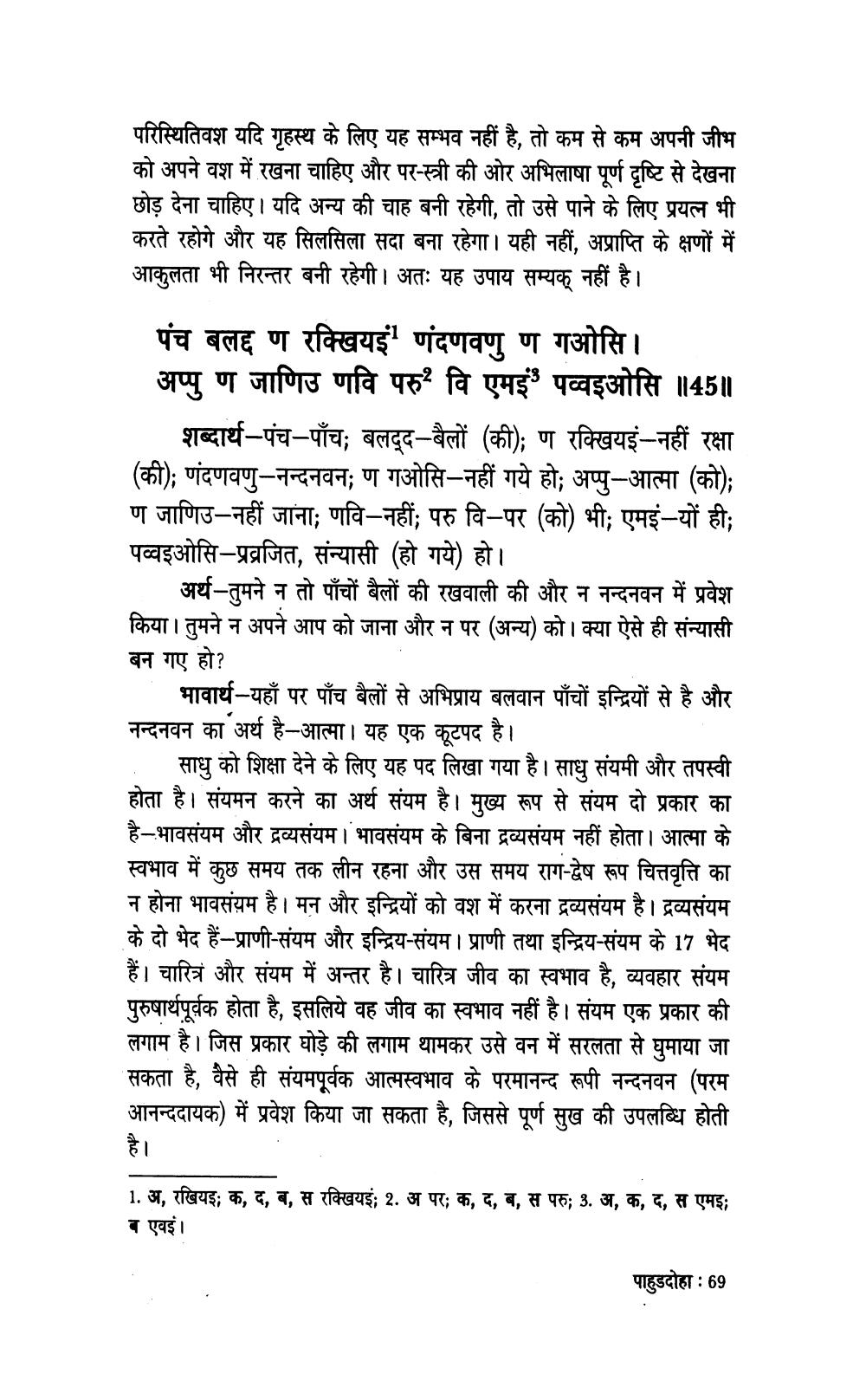________________
परिस्थितिवश यदि गृहस्थ के लिए यह सम्भव नहीं है, तो कम से कम अपनी जीभ को अपने वश में रखना चाहिए और पर-स्त्री की ओर अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखना छोड़ देना चाहिए। यदि अन्य की चाह बनी रहेगी, तो उसे पाने के लिए प्रयत्न भी करते रहोगे और यह सिलसिला सदा बना रहेगा। यही नहीं, अप्राप्ति के क्षणों में आकुलता भी निरन्तर बनी रहेगी। अतः यह उपाय सम्यक् नहीं है।
पंच बलद्द ण रक्खियई णंदणवणु ण गओसि। अप्पु ण जाणिउ णवि परु वि एमई पव्वइओसि ॥45॥
शब्दार्थ-पंच-पाँच; बलद-बैलों (की); ण रक्खियइं-नहीं रक्षा (की); णंदणवणु-नन्दनवन; ण गओसि-नहीं गये हो; अप्पु-आत्मा (को); ण जाणिउ-नहीं जाना; णवि-नहीं; परु वि-पर (को) भी; एमई-यों ही; पव्वइओसि-प्रव्रजित, संन्यासी (हो गये) हो।
अर्थ-तुमने न तो पाँचों बैलों की रखवाली की और न नन्दनवन में प्रवेश किया। तुमने न अपने आप को जाना और न पर (अन्य) को। क्या ऐसे ही संन्यासी बन गए हो?
भावार्थ-यहाँ पर पाँच बैलों से अभिप्राय बलवान पाँचों इन्द्रियों से है और नन्दनवन का अर्थ है-आत्मा। यह एक कूटपद है। . साधु को शिक्षा देने के लिए यह पद लिखा गया है। साधु संयमी और तपस्वी होता है। संयमन करने का अर्थ संयम है। मुख्य रूप से संयम दो प्रकार का है-भावसंयम और द्रव्यसंयम। भावसंयम के बिना द्रव्यसंयम नहीं होता। आत्मा के स्वभाव में कुछ समय तक लीन रहना और उस समय राग-द्वेष रूप चित्तवृत्ति का न होना भावसंयम है। मन और इन्द्रियों को वश में करना द्रव्यसंयम है। द्रव्यसंयम के दो भेद हैं-प्राणी-संयम और इन्द्रिय-संयम। प्राणी तथा इन्द्रिय-संयम के 17 भेद हैं। चारित्रं और संयम में अन्तर है। चारित्र जीव का स्वभाव है, व्यवहार संयम पुरुषार्थपूर्वक होता है, इसलिये वह जीव का स्वभाव नहीं है। संयम एक प्रकार की लगाम है। जिस प्रकार घोड़े की लगाम थामकर उसे वन में सरलता से घुमाया जा सकता है, वैसे ही संयमपूर्वक आत्मस्वभाव के परमानन्द रूपी नन्दनवन (परम आनन्ददायक) में प्रवेश किया जा सकता है, जिससे पूर्ण सुख की उपलब्धि होती
1. अ, रखियइ; क, द, ब, स रक्खियइं; 2. अ पर; क, द, ब, स परु; 3. अ, क, द, स एमइ; व एवई।
पाहुडदोहा : 69