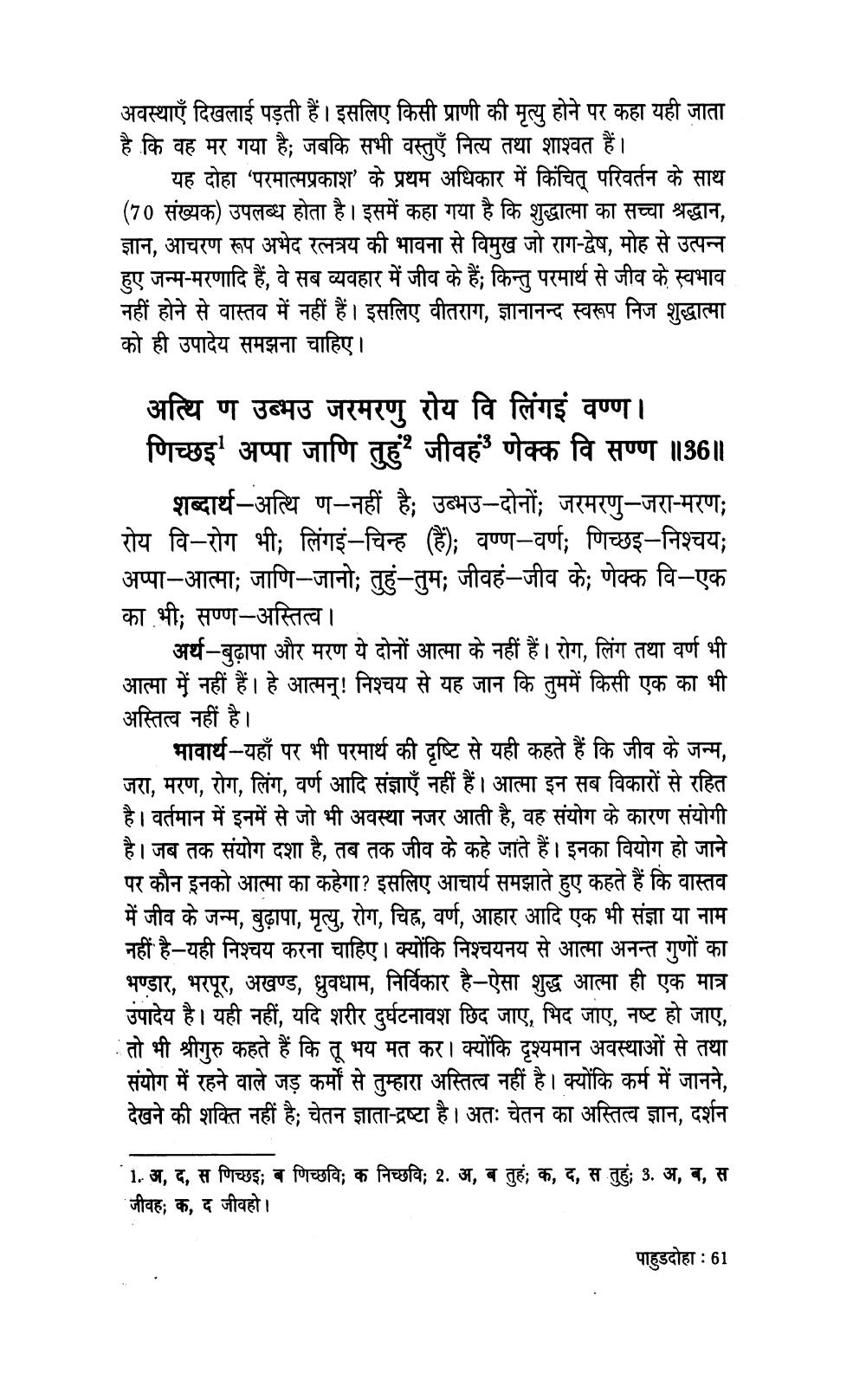________________
अवस्थाएँ दिखलाई पड़ती हैं। इसलिए किसी प्राणी की मृत्यु होने पर कहा यही जाता है कि वह मर गया है, जबकि सभी वस्तुएँ नित्य तथा शाश्वत हैं।
यह दोहा ‘परमात्मप्रकाश' के प्रथम अधिकार में किंचित् परिवर्तन के साथ (70 संख्यक) उपलब्ध होता है। इसमें कहा गया है कि शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण रूप अभेद रत्नत्रय की भावना से विमुख जो राग-द्वेष, मोह से उत्पन्न हुए जन्म-मरणादि हैं, वे सब व्यवहार में जीव के हैं; किन्तु परमार्थ से जीव के स्वभाव नहीं होने से वास्तव में नहीं हैं। इसलिए वीतराग, ज्ञानानन्द स्वरूप निज शुद्धात्मा को ही उपादेय समझना चाहिए।
अत्थि ण उब्भउ जरमरणु रोय वि लिंगई वण्ण। णिच्छइ' अप्पा जाणि तुहुँ' जीवह णेक्क वि सण्ण ॥36॥
शब्दार्थ-अस्थि ण-नहीं है; उब्भउ-दोनों; जरमरणु-जरा-मरण; रोय वि-रोग भी; लिंगई-चिन्ह हैं); वण्ण-वर्ण; णिच्छइ-निश्चय; अप्पा-आत्मा; जाणि-जानो; तुहुं-तुम; जीवहं-जीव के णेक्क वि-एक का भी; सण्ण-अस्तित्व।
अर्थ-बुढ़ापा और मरण ये दोनों आत्मा के नहीं हैं। रोग, लिंग तथा वर्ण भी आत्मा में नहीं हैं। हे आत्मन्! निश्चय से यह जान कि तुममें किसी एक का भी अस्तित्व नहीं है।
भावार्थ-यहाँ पर भी परमार्थ की दृष्टि से यही कहते हैं कि जीव के जन्म, जरा, मरण, रोग, लिंग, वर्ण आदि संज्ञाएँ नहीं हैं। आत्मा इन सब विकारों से रहित है। वर्तमान में इनमें से जो भी अवस्था नजर आती है, वह संयोग के कारण संयोगी है। जब तक संयोग दशा है, तब तक जीव के कहे जाते हैं। इनका वियोग हो जाने पर कौन इनको आत्मा का कहेगा? इसलिए आचार्य समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में जीव के जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, चिह्न, वर्ण, आहार आदि एक भी संज्ञा या नाम नहीं है-यही निश्चय करना चाहिए। क्योंकि निश्चयनय से आत्मा अनन्त गुणों का भण्डार, भरपूर, अखण्ड, ध्रुवधाम, निर्विकार है-ऐसा शुद्ध आत्मा ही एक मात्र उपादेय है। यही नहीं, यदि शरीर दुर्घटनावश छिद जाए, भिद जाए, नष्ट हो जाए, तो भी श्रीगुरु कहते हैं कि तू भय मत कर। क्योंकि दृश्यमान अवस्थाओं से तथा संयोग में रहने वाले जड़ कर्मों से तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। क्योंकि कर्म में जानने, देखने की शक्ति नहीं है; चेतन ज्ञाता-द्रष्टा है। अतः चेतन का अस्तित्व ज्ञान, दर्शन
1. अ, द, स णिच्छइ ब णिच्छवि; क निच्छवि; 2. अ, ब तुहं; क, द, स तुहूं; 3. अ, ब, स जीवह; क, द जीवहो।
पाहुडदोहा : 61