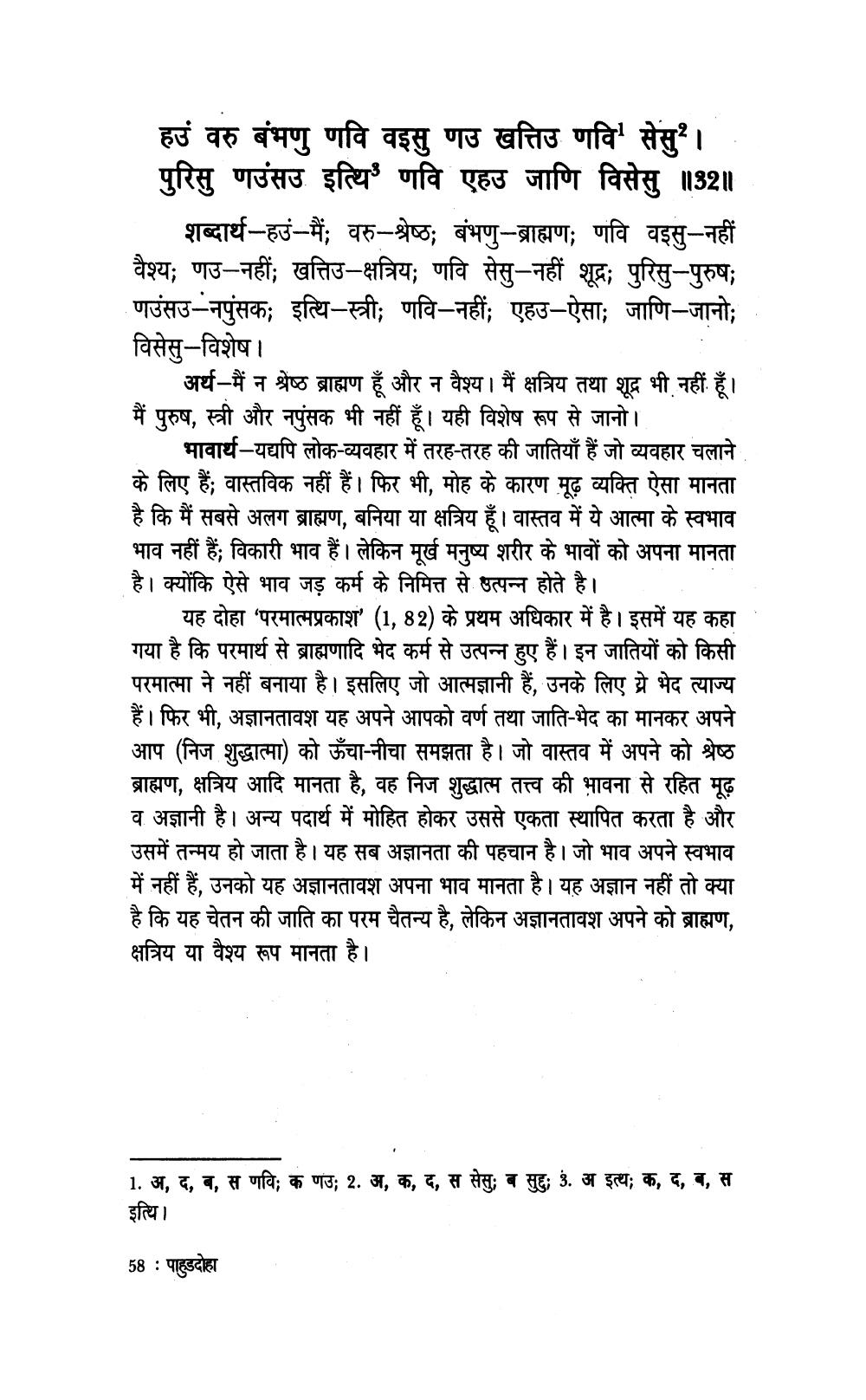________________
हउं वरु बंभणु णवि वइसु णउ खत्तिउ णवि' सेसु।
पुरिसु णउंसउ इत्थि णवि एहउ जाणि विसेसु ॥32॥ ___शब्दार्थ-हउं-मैं; वरु-श्रेष्ठ; बंभणु-ब्राह्मण; णवि वइसु-नहीं वैश्य; णउ-नहीं; खत्तिउ-क्षत्रिय; णवि सेसु-नहीं शूद्र; पुरिसु-पुरुष; णउंसउ-नपुंसक; इत्थि-स्त्री; णवि-नहीं; एहउ-ऐसा; जाणि-जानो; विसेसु-विशेष।
अर्थ-मैं न श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ और न वैश्य। मैं क्षत्रिय तथा शूद्र भी नहीं हूँ। मैं पुरुष, स्त्री और नपुंसक भी नहीं हूँ। यही विशेष रूप से जानो।
भावार्थ-यद्यपि लोक-व्यवहार में तरह-तरह की जातियाँ हैं जो व्यवहार चलाने के लिए हैं; वास्तविक नहीं हैं। फिर भी, मोह के कारण मूढ़ व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं सबसे अलग ब्राह्मण, बनिया या क्षत्रिय हैं। वास्तव में ये आत्मा के स्वभाव भाव नहीं हैं; विकारी भाव हैं। लेकिन मूर्ख मनुष्य शरीर के भावों को अपना मानता है। क्योंकि ऐसे भाव जड़ कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते है।
यह दोहा ‘परमात्मप्रकाश' (1, 82) के प्रथम अधिकार में है। इसमें यह कहा गया है कि परमार्थ से ब्राह्मणादि भेद कर्म से उत्पन्न हुए हैं। इन जातियों को किसी परमात्मा ने नहीं बनाया है। इसलिए जो आत्मज्ञानी हैं, उनके लिए ग्रे भेद त्याज्य हैं। फिर भी, अज्ञानतावश यह अपने आपको वर्ण तथा जाति-भेद का मानकर अपने आप (निज शुद्धात्मा) को ऊँचा-नीचा समझता है। जो वास्तव में अपने को श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मानता है, वह निज शुद्धात्म तत्त्व की भावना से रहित मूढ़ व अज्ञानी है। अन्य पदार्थ में मोहित होकर उससे एकता स्थापित करता है और उसमें तन्मय हो जाता है। यह सब अज्ञानता की पहचान है। जो भाव अपने स्वभाव में नहीं हैं, उनको यह अज्ञानतावश अपना भाव मानता है। यह अज्ञान नहीं तो क्या है कि यह चेतन की जाति का परम चैतन्य है, लेकिन अज्ञानतावश अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य रूप मानता है।
1. अ, द, ब, स णवि; क णउ; 2. अ, क, द, स सेसु; ब सुह; 3. अ इत्थ; क, द, ब, स इत्यि ।
58 : पाहुडदोहा