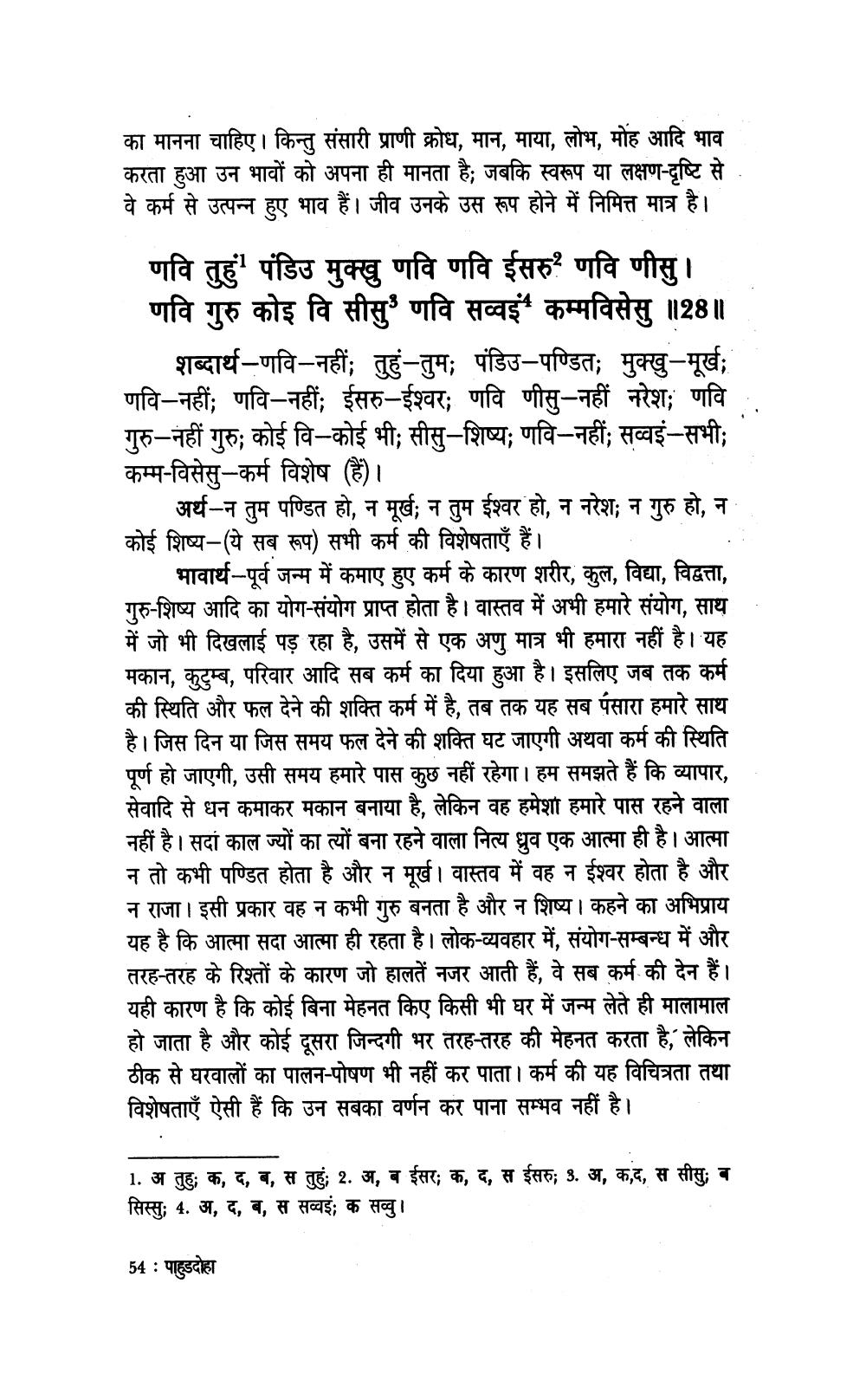________________
का मानना चाहिए। किन्तु संसारी प्राणी क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि भाव करता हुआ उन भावों को अपना ही मानता है; जबकि स्वरूप या लक्षण-दृष्टि से वे कर्म से उत्पन्न हुए भाव हैं। जीव उनके उस रूप होने में निमित्त मात्र है।
णवि तुहुँ' पंडिउ मुक्खु णवि णवि ईसरु णवि णीसु। णवि गुरु कोइ वि सीसु णवि सव्वई कम्मविसेसु ॥28॥
शब्दार्थ-णवि-नहीं; तुहुं-तुम; पंडिउ-पण्डित; मुक्खु-मूर्ख; णवि-नहीं; णवि-नहीं; ईसरु-ईश्वर; णवि णीसु-नहीं नरेश; णवि गुरु-नहीं गुरु; कोई वि-कोई भी; सीसु-शिष्य; णवि-नहीं; सव्वइं-सभी; कम्म-विसेसु-कर्म विशेष (हैं)।
अर्थ-न तुम पण्डित हो, न मूर्ख; न तुम ईश्वर हो, न नरेश; न गुरु हो, न कोई शिष्य-(ये सब रूप) सभी कर्म की विशेषताएँ हैं।
भावार्थ-पूर्व जन्म में कमाए हुए कर्म के कारण शरीर, कुल, विद्या, विद्वत्ता, गुरु-शिष्य आदि का योग-संयोग प्राप्त होता है। वास्तव में अभी हमारे संयोग, साथ में जो भी दिखलाई पड़ रहा है, उसमें से एक अणु मात्र भी हमारा नहीं है। यह मकान, कुटुम्ब, परिवार आदि सब कर्म का दिया हुआ है। इसलिए जब तक कर्म की स्थिति और फल देने की शक्ति कर्म में है, तब तक यह सब पंसारा हमारे साथ है। जिस दिन या जिस समय फल देने की शक्ति घट जाएगी अथवा कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाएगी, उसी समय हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम समझते हैं कि व्यापार, सेवादि से धन कमाकर मकान बनाया है, लेकिन वह हमेशा हमारे पास रहने वाला नहीं है। सदां काल ज्यों का त्यों बना रहने वाला नित्य ध्रुव एक आत्मा ही है। आत्मा न तो कभी पण्डित होता है और न मूर्ख। वास्तव में वह न ईश्वर होता है और न राजा। इसी प्रकार वह न कभी गुरु बनता है और न शिष्य। कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा सदा आत्मा ही रहता है। लोक-व्यवहार में, संयोग-सम्बन्ध में और तरह-तरह के रिश्तों के कारण जो हालतें नजर आती हैं, वे सब कर्म की देन हैं। यही कारण है कि कोई बिना मेहनत किए किसी भी घर में जन्म लेते ही मालामाल हो जाता है और कोई दूसरा जिन्दगी भर तरह-तरह की मेहनत करता है, लेकिन ठीक से घरवालों का पालन-पोषण भी नहीं कर पाता। कर्म की यह विचित्रता तथा विशेषताएँ ऐसी हैं कि उन सबका वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है।
1. अ तुहु; क, द, ब, स तुहुँ; 2. अ, ब ईसर; क, द, स ईसरु; 3. अ, क,द, स सीसु; व सिस्सु; 4. अ, द, ब, स सव्वइं; क सब्बु।
54 : पाहुडदोहा