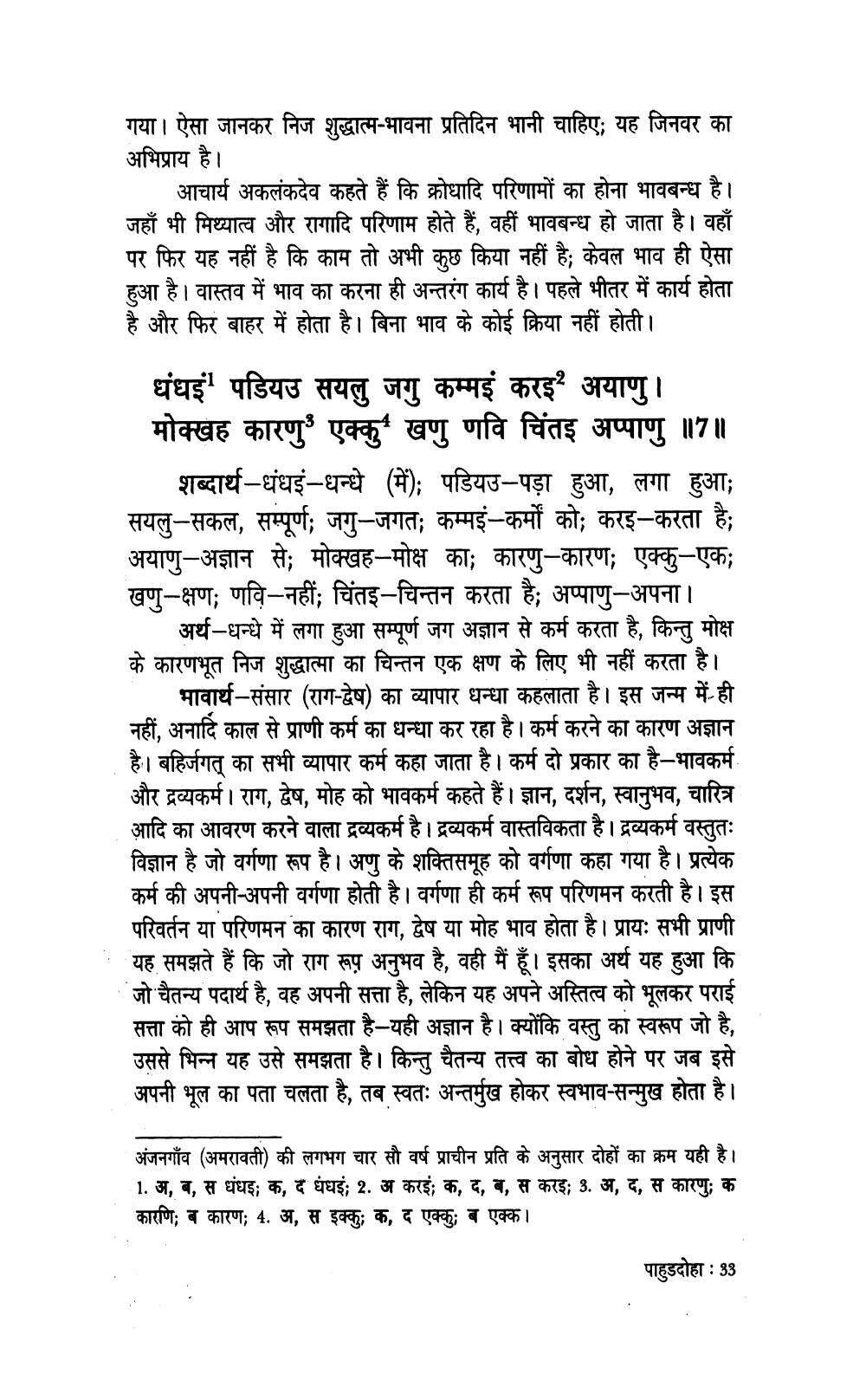________________
गया। ऐसा जानकर निज शुद्धात्म-भावना प्रतिदिन भानी चाहिए; यह जिनवर का अभिप्राय है।
आचार्य अकलंकदेव कहते हैं कि क्रोधादि परिणामों का होना भावबन्ध है। जहाँ भी मिथ्यात्व और रागादि परिणाम होते हैं, वहीं भावबन्ध हो जाता है। वहाँ पर फिर यह नहीं है कि काम तो अभी कुछ किया नहीं है; केवल भाव ही ऐसा हुआ है। वास्तव में भाव का करना ही अन्तरंग कार्य है। पहले भीतर में कार्य होता है और फिर बाहर में होता है। बिना भाव के कोई क्रिया नहीं होती।
धंधई पडियउ सयलु जगु कम्मई करइ अयाणु। मोक्खह कारणु एक्कु खणु णवि चिंतइ अप्पाणु ॥7॥
शब्दार्थ-धंधइं-धन्धे (में); पडियउ-पड़ा हुआ, लगा हुआ; सयलु-सकल, सम्पूर्ण; जगु-जगत; कम्मइं-कर्मों को; करइ-करता है; अयाणु-अज्ञान से; मोक्खह-मोक्ष का; कारणु-कारण; एक्कु-एक; खणु-क्षण; णवि-नहीं; चिंतइ-चिन्तन करता है; अप्पाणु-अपना।
___ अर्थ-धन्धे में लगा हुआ सम्पूर्ण जग अज्ञान से कर्म करता है, किन्तु मोक्ष के कारणभूत निज शुद्धात्मा का चिन्तन एक क्षण के लिए भी नहीं करता है।
भावार्थ-संसार (राग-द्वेष) का व्यापार धन्धा कहलाता है। इस जन्म में ही नहीं, अनादि काल से प्राणी कर्म का धन्धा कर रहा है। कर्म करने का कारण अज्ञान है। बहिर्जगत् का सभी व्यापार कर्म कहा जाता है। कर्म दो प्रकार का है-भावकर्म और द्रव्यकर्म। राग, द्वेष, मोह को भावकर्म कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, स्वानुभव, चारित्र आदि का आवरण करने वाला द्रव्यकर्म है। द्रव्यकर्म वास्तविकता है। द्रव्यकर्म वस्तुतः विज्ञान है जो वर्गणा रूप है। अणु के शक्तिसमूह को वर्गणा कहा गया है। प्रत्येक कर्म की अपनी-अपनी वर्गणा होती है। वर्गणा ही कर्म रूप परिणमन करती है। इस परिवर्तन या परिणमन का कारण राग, द्वेष या मोह भाव होता है। प्रायः सभी प्राणी यह समझते हैं कि जो राग रूप अनुभव है, वही मैं हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चैतन्य पदार्थ है, वह अपनी सत्ता है, लेकिन यह अपने अस्तित्व को भूलकर पराई सत्ता को ही आप रूप समझता है-यही अज्ञान है। क्योंकि वस्तु का स्वरूप जो है, उससे भिन्न यह उसे समझता है। किन्तु चैतन्य तत्त्व का बोध होने पर जब इसे अपनी भूल का पता चलता है, तब स्वतः अन्तर्मुख होकर स्वभाव-सन्मुख होता है।
अंजनगाँव (अमरावती) की लगभग चार सौ वर्ष प्राचीन प्रति के अनुसार दोहों का क्रम यही है। 1. अ, ब, स धंधइ; क, द धंधई; 2. अ करई; क, द, ब, स करइ; 3. अ, द, स कारणु; क कारणि; ब कारण; 4. अ, स इक्कु, क, द एक्कु; व एक्क।
पाहुडदोहा : 33