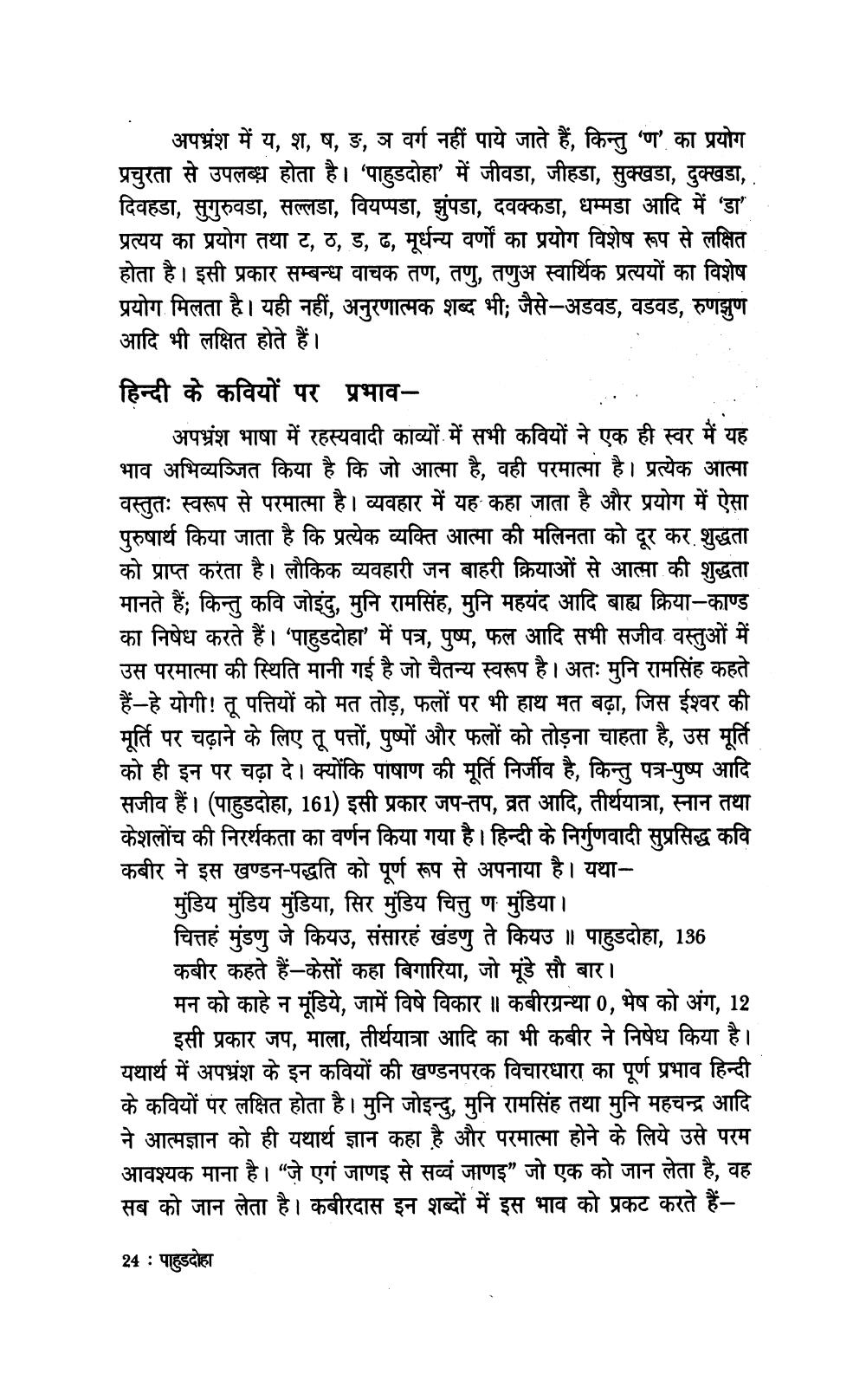________________
अपभ्रंश में य, श, ष, ङ, ञ वर्ग नहीं पाये जाते हैं, किन्तु 'ण' का प्रयोग प्रचुरता से उपलब्ध होता है। ‘पाहुडदोहा' में जीवडा, जीहडा, सुक्खडा, दुक्खडा, दिवहडा, सुगुरुवडा, सल्लडा, वियप्पडा, झुपडा, दवक्कडा, धम्मडा आदि में 'डा' प्रत्यय का प्रयोग तथा ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य वर्गों का प्रयोग विशेष रूप से लक्षित होता है। इसी प्रकार सम्बन्ध वाचक तण, तणु, तणुअ स्वार्थिक प्रत्ययों का विशेष प्रयोग मिलता है। यही नहीं, अनुरणात्मक शब्द भी; जैसे-अडवड, वडवड, रुणझुण आदि भी लक्षित होते हैं। हिन्दी के कवियों पर प्रभाव
अपभ्रंश भाषा में रहस्यवादी काव्यों में सभी कवियों ने एक ही स्वर में यह भाव अभिव्यञ्जित किया है कि जो आत्मा है, वही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा वस्तुतः स्वरूप से परमात्मा है। व्यवहार में यह कहा जाता है और प्रयोग में ऐसा पुरुषार्थ किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की मलिनता को दूर कर शुद्धता को प्राप्त करता है। लौकिक व्यवहारी जन बाहरी क्रियाओं से आत्मा की शुद्धता मानते हैं; किन्तु कवि जोइंदु, मुनि रामसिंह, मुनि महयंद आदि बाह्य क्रिया-काण्ड का निषेध करते हैं। ‘पाहुडदोहा' में पत्र, पुष्प, फल आदि सभी सजीव वस्तुओं में उस परमात्मा की स्थिति मानी गई है जो चैतन्य स्वरूप है। अतः मुनि रामसिंह कहते हैं-हे योगी! तू पत्तियों को मत तोड़, फलों पर भी हाथ मत बढ़ा, जिस ईश्वर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए तू पत्तों, पुष्पों और फलों को तोड़ना चाहता है, उस मूर्ति को ही इन पर चढ़ा दे। क्योंकि पाषाण की मूर्ति निर्जीव है, किन्तु पत्र-पुष्प आदि सजीव हैं। (पाहुडदोहा, 161) इसी प्रकार जप-तप, व्रत आदि, तीर्थयात्रा, स्नान तथा केशलोंच की निरर्थकता का वर्णन किया गया है। हिन्दी के निर्गुणवादी सुप्रसिद्ध कवि कबीर ने इस खण्डन-पद्धति को पूर्ण रूप से अपनाया है। यथा
मुंडिय मुंडिय मुंडिया, सिर मुंडिय चित्तु ण मुंडिया। चित्तहं मुंडणु जे कियउ, संसारहं खंडणु ते कियउ ॥ पाहुडदोहा, 136 कबीर कहते हैं-केसों कहा बिगारिया, जो मूंडे सौ बार। मन को काहे न मुडिये, जामें विषे विकार ॥ कबीरग्रन्था 0, भेष को अंग, 12
इसी प्रकार जप, माला, तीर्थयात्रा आदि का भी कबीर ने निषेध किया है। यथार्थ में अपभ्रंश के इन कवियों की खण्डनपरक विचारधारा का पूर्ण प्रभाव हिन्दी के कवियों पर लक्षित होता है। मुनि जोइन्दु, मुनि रामसिंह तथा मुनि महचन्द्र आदि ने आत्मज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान कहा है और परमात्मा होने के लिये उसे परम आवश्यक माना है। “जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ" जो एक को जान लेता है, वह सब को जान लेता है। कबीरदास इन शब्दों में इस भाव को प्रकट करते हैं
24 : पाहुडदोहा