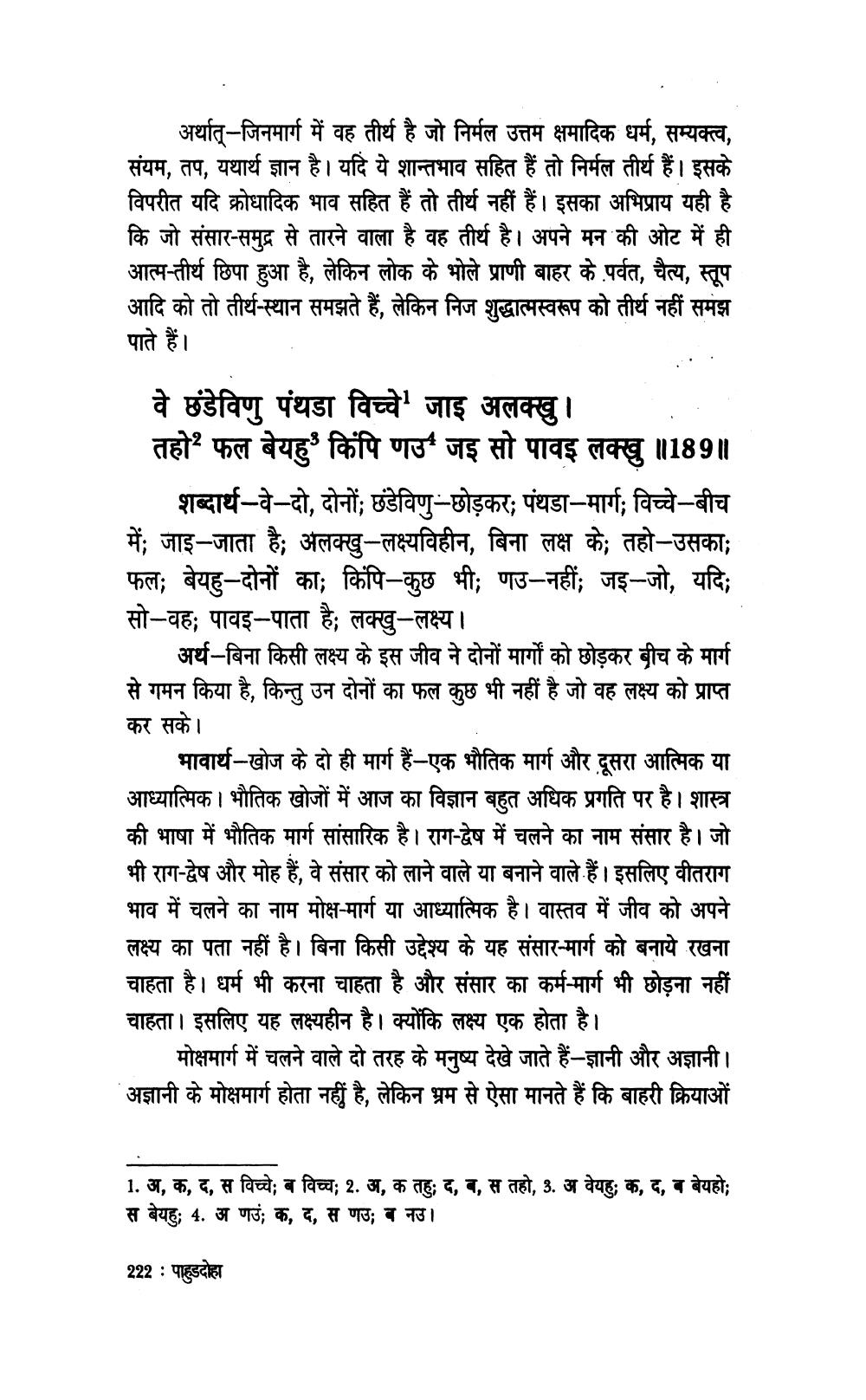________________
अर्थात् - जिनमार्ग में वह तीर्थ है जो निर्मल उत्तम क्षमादिक धर्म, सम्यक्त्व, संयम, तप, यथार्थ ज्ञान है । यदि ये शान्तभाव सहित हैं तो निर्मल तीर्थ हैं। इसके विपरीत यदि क्रोधादिक भाव सहित हैं तो तीर्थ नहीं हैं। इसका अभिप्राय यही है कि जो संसार - समुद्र से तारने वाला है वह तीर्थ है। अपने मन की ओट में ही आत्म-तीर्थ छिपा हुआ है, लेकिन लोक के भोले प्राणी बाहर के पर्वत, चैत्य, स्तूप आदि को तो तीर्थ-स्थान समझते हैं, लेकिन निज शुद्धात्मस्वरूप को तीर्थ नहीं समझ पाते हैं।
वे छंडेविणु पंथडा विच्चे' जाइ अलक्खु ।
तहो' फल बेयहु' किंपि णउ जइ सो पावइ लक्खु ॥189॥
शब्दार्थ-वे-दो, दोनों; छंडेविणु - छोड़कर ; पंथडा-मार्ग; विच्चे-बीच में; जाइ - जाता है; अलक्खु - लक्ष्यविहीन, बिना लक्ष के; तहो - उसका ; फल; बेयहु- दोनों का; किंपि - कुछ भी ; णउ-नहीं; जइ - जो, यदि; सो- वह; पावइ-पाता है; लक्खु - लक्ष्य ।
अर्थ - बिना किसी लक्ष्य के इस जीव ने दोनों मार्गों को छोड़कर बीच के मार्ग से गमन किया है, किन्तु उन दोनों का फल कुछ भी नहीं है जो वह लक्ष्य को प्राप्त कर सके ।
भावार्थ - खोज के दो ही मार्ग हैं - एक भौतिक मार्ग और दूसरा आत्मिक या आध्यात्मिक। भौतिक खोजों में आज का विज्ञान बहुत अधिक प्रगति पर है। शास्त्र की भाषा में भौतिक मार्ग सांसारिक है। राग-द्वेष में चलने का नाम संसार है। जो भी राग-द्वेष और मोह हैं, वे संसार को लाने वाले या बनाने वाले हैं। इसलिए वीतराग भाव में चलने का नाम मोक्ष - मार्ग या आध्यात्मिक है। वास्तव में जीव को अपने लक्ष्य का पता नहीं है। बिना किसी उद्देश्य के यह संसार - मार्ग को बनाये रखना चाहता है। धर्म भी करना चाहता है और संसार का कर्म-मार्ग भी छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए यह लक्ष्यहीन है। क्योंकि लक्ष्य एक होता है ।
मोक्षमार्ग में चलने वाले दो तरह के मनुष्य देखे जाते हैं - ज्ञानी और अज्ञानी । अज्ञानी के मोक्षमार्ग होता नहीं है, लेकिन भ्रम से ऐसा मानते हैं कि बाहरी क्रियाओं
1. अ, क, द, स विच्चे; ब विच्च; 2. अ, क तहु; द, ब, स तहो, 3. अ वेयहु; क, द, ब बेयहो; स बेयहु; 4. अ णउं; क, द, स णउ; ब नउ ।
222 : पाहुडोहा