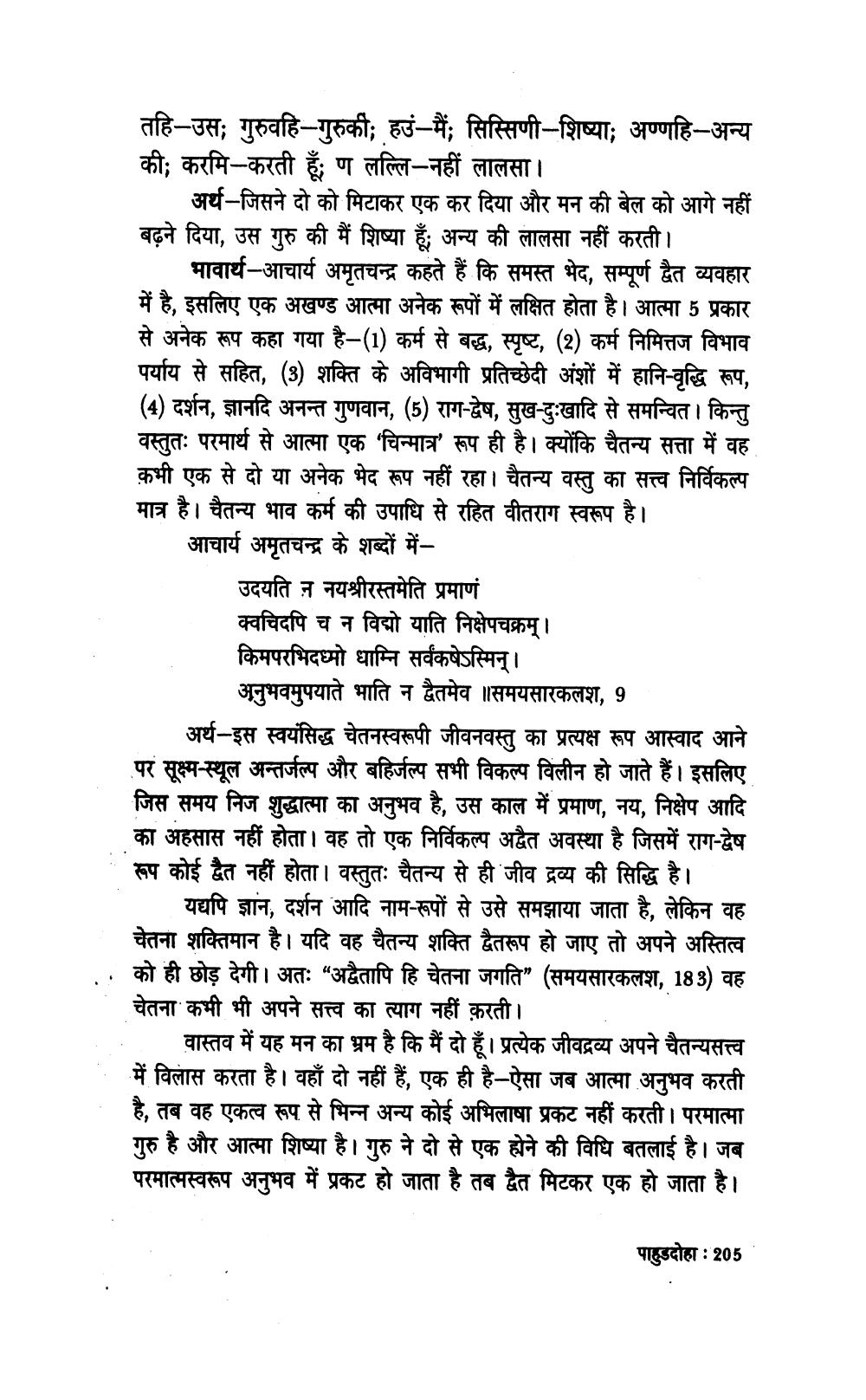________________
तहि-उस; गुरुवहि-गुरुकी; हउं-मैं; सिस्सिणी-शिष्या; अण्णहि-अन्य की; करमि-करती हूँ ण लल्लि-नहीं लालसा।
__ अर्थ-जिसने दो को मिटाकर एक कर दिया और मन की बेल को आगे नहीं बढ़ने दिया, उस गुरु की मैं शिष्या हूँ; अन्य की लालसा नहीं करती।
भावार्थ-आचार्य अमृतचन्द्र कहते हैं कि समस्त भेद, सम्पूर्ण द्वैत व्यवहार में है, इसलिए एक अखण्ड आत्मा अनेक रूपों में लक्षित होता है। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप कहा गया है-(1) कर्म से बद्ध, स्पृष्ट, (2) कर्म निमित्तज विभाव पर्याय से सहित, (3) शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेदी अंशों में हानि-वृद्धि रूप, (4) दर्शन, ज्ञानदि अनन्त गुणवान, (5) राग-द्वेष, सुख-दुःखादि से समन्वित। किन्तु वस्तुतः परमार्थ से आत्मा एक 'चिन्मात्र' रूप ही है। क्योंकि चैतन्य सत्ता में वह क़भी एक से दो या अनेक भेद रूप नहीं रहा। चैतन्य वस्तु का सत्त्व निर्विकल्प मात्र है। चैतन्य भाव कर्म की उपाधि से रहित वीतराग स्वरूप है। आचार्य अमृतचन्द्र के शब्दों में
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रम् । किमपरभिदध्मो धाम्नि सर्वंकषेऽस्मिन्।
अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥समयसारकलश, 9 अर्थ-इस स्वयंसिद्ध चेतनस्वरूपी जीवनवस्तु का प्रत्यक्ष रूप आस्वाद आने पर सूक्ष्म-स्थूल अन्तर्जल्प और बहिर्जल्प सभी विकल्प विलीन हो जाते हैं। इसलिए जिस समय निज शुद्धात्मा का अनुभव है, उस काल में प्रमाण, नय, निक्षेप आदि का अहसास नहीं होता। वह तो एक निर्विकल्प अद्वैत अवस्था है जिसमें राग-द्वेष रूप कोई द्वैत नहीं होता। वस्तुतः चैतन्य से ही जीव द्रव्य की सिद्धि है।
यद्यपि ज्ञान, दर्शन आदि नाम-रूपों से उसे समझाया जाता है, लेकिन वह चेतना शक्तिमान है। यदि वह चैतन्य शक्ति द्वैतरूप हो जाए तो अपने अस्तित्व को ही छोड़ देगी। अतः “अद्वैतापि हि चेतना जगति" (समयसारकलश, 183) वह चेतना कभी भी अपने सत्त्व का त्याग नहीं करती।
वास्तव में यह मन का भ्रम है कि मैं दो हूँ। प्रत्येक जीवद्रव्य अपने चैतन्यसत्त्व में विलास करता है। वहाँ दो नहीं हैं, एक ही है-ऐसा जब आत्मा अनुभव करती है, तब वह एकत्व रूप से भिन्न अन्य कोई अभिलाषा प्रकट नहीं करती। परमात्मा गुरु है और आत्मा शिष्या है। गुरु ने दो से एक होने की विधि बतलाई है। जब परमात्मस्वरूप अनुभव में प्रकट हो जाता है तब द्वैत मिटकर एक हो जाता है।
पाहुडदोहा : 205