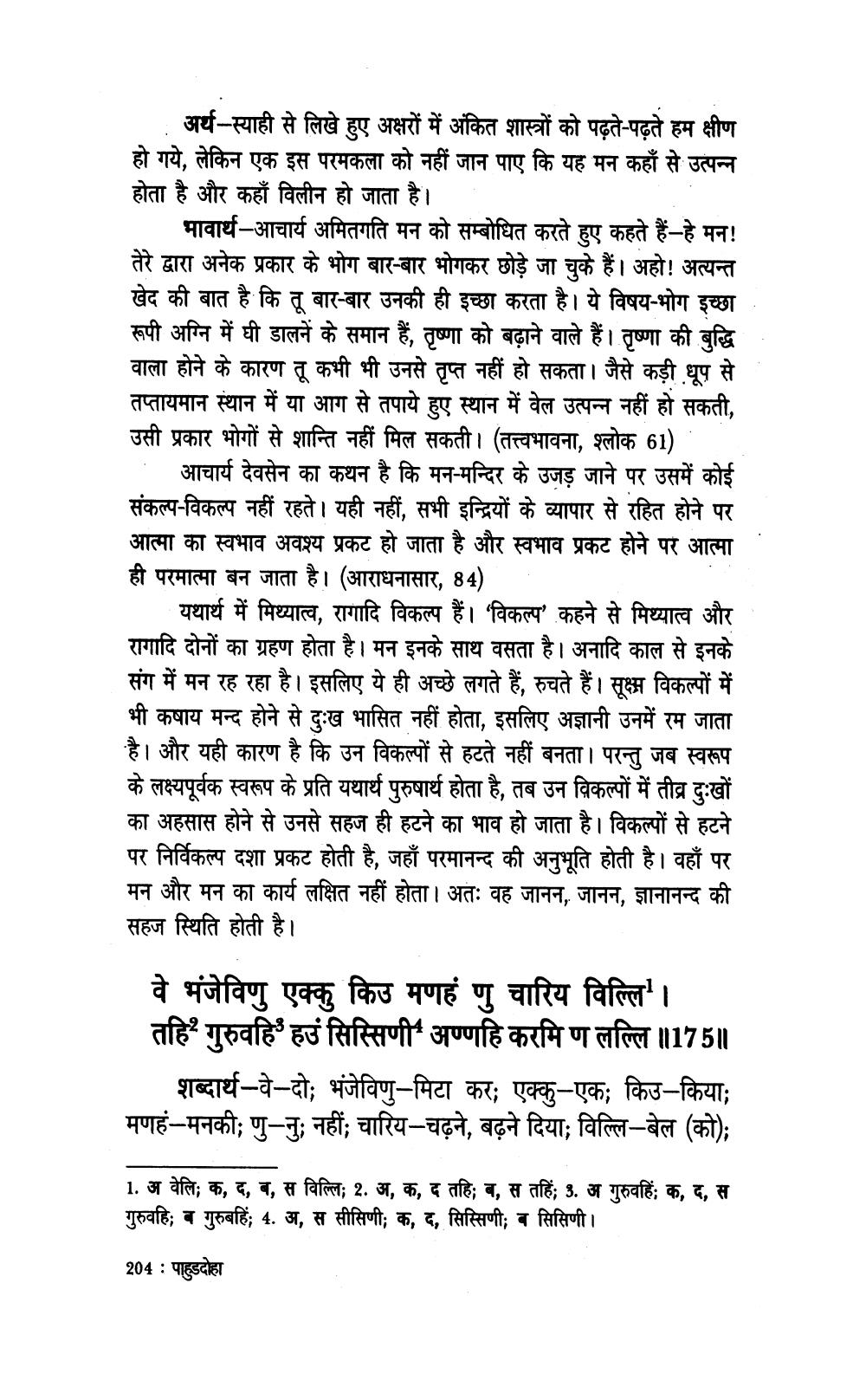________________
अर्थ-स्याही से लिखे हुए अक्षरों में अंकित शास्त्रों को पढ़ते-पढ़ते हम क्षीण हो गये, लेकिन एक इस परमकला को नहीं जान पाए कि यह मन कहाँ से उत्पन्न होता है और कहाँ विलीन हो जाता है।
भावार्थ-आचार्य अमितगति मन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं-हे मन! तेरे द्वारा अनेक प्रकार के भोग बार-बार भोगकर छोड़े जा चुके हैं। अहो! अत्यन्त खेद की बात है कि तू बार-बार उनकी ही इच्छा करता है। ये विषय-भोग इच्छा रूपी अग्नि में घी डालने के समान हैं, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। तृष्णा की बुद्धि वाला होने के कारण तू कभी भी उनसे तृप्त नहीं हो सकता। जैसे कड़ी धूप से तप्तायमान स्थान में या आग से तपाये हुए स्थान में वेल उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार भोगों से शान्ति नहीं मिल सकती। (तत्त्वभावना, श्लोक 61) - आचार्य देवसेन का कथन है कि मन-मन्दिर के उजड़ जाने पर उसमें कोई संकल्प-विकल्प नहीं रहते। यही नहीं, सभी इन्द्रियों के व्यापार से रहित होने पर आत्मा का स्वभाव अवश्य प्रकट हो जाता है और स्वभाव प्रकट होने पर आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। (आराधनासार, 84)
___ यथार्थ में मिथ्यात्व, रागादि विकल्प हैं। 'विकल्प' कहने से मिथ्यात्व और रागादि दोनों का ग्रहण होता है। मन इनके साथ वसता है। अनादि काल से इनके संग में मन रह रहा है। इसलिए ये ही अच्छे लगते हैं, रुचते हैं। सूक्ष्म विकल्पों में भी कषाय मन्द होने से दुःख भासित नहीं होता, इसलिए अज्ञानी उनमें रम जाता है। और यही कारण है कि उन विकल्पों से हटते नहीं बनता। परन्तु जब स्वरूप के लक्ष्यपूर्वक स्वरूप के प्रति यथार्थ पुरुषार्थ होता है, तब उन विकल्पों में तीव्र दुःखों का अहसास होने से उनसे सहज ही हटने का भाव हो जाता है। विकल्पों से हटने पर निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, जहाँ परमानन्द की अनुभूति होती है। वहाँ पर मन और मन का कार्य लक्षित नहीं होता। अतः वह जानन, जानन, ज्ञानानन्द की सहज स्थिति होती है।
वे भंजेविणु एक्कु किउ मणहं णु चारिय विल्लि। तहि गुरुवहि हउं सिस्सिणी अण्णहि करमिण लल्लि 1175॥
शब्दार्थ-वे-दो; भंजेविणु-मिटा कर; एक्कु-एक; किउ-किया; मणहं-मनकी; णु-नु; नहीं; चारिय-चढ़ने, बढ़ने दिया; विल्लि–बेल (को);
1. अ वेलि; क, द, ब, स विल्लि; 2. अ, क, द तहि; ब, स तहिं; 3. अ गुरुवहिं; क, द, स गुरुवहि; व गुरुबहिं; 4. अ, स सीसिणी; क, द, सिस्सिणी; व सिसिणी।
204 : पाहुडदोहा