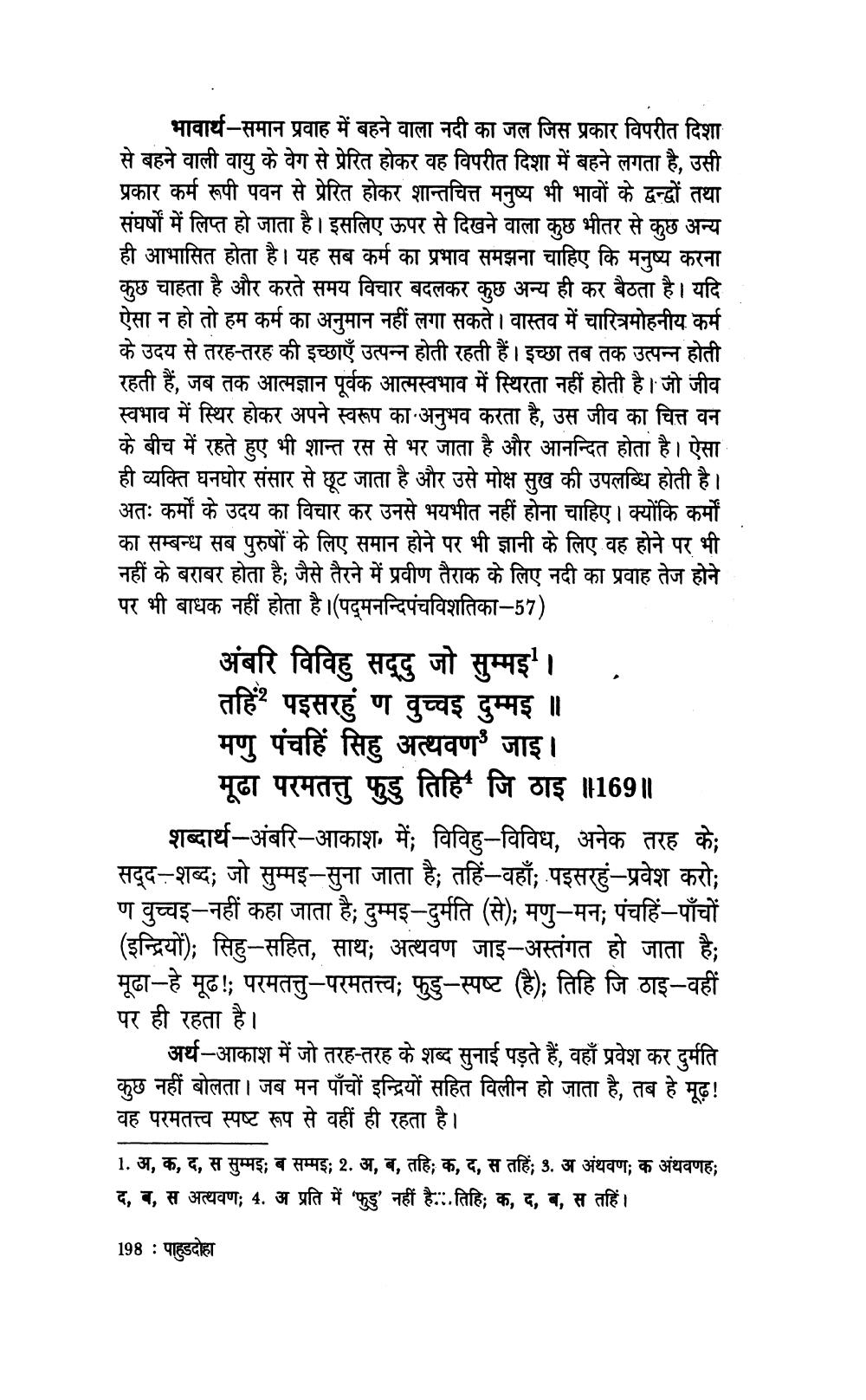________________
भावार्थ-समान प्रवाह में बहने वाला नदी का जल जिस प्रकार विपरीत दिशा से बहने वाली वायु के वेग से प्रेरित होकर वह विपरीत दिशा में बहने लगता है, उसी प्रकार कर्म रूपी पवन से प्रेरित होकर शान्तचित्त मनुष्य भी भावों के द्वन्द्वों तथा संघर्षों में लिप्त हो जाता है। इसलिए ऊपर से दिखने वाला कुछ भीतर से कुछ अन्य ही आभासित होता है। यह सब कर्म का प्रभाव समझना चाहिए कि मनुष्य करना कुछ चाहता है और करते समय विचार बदलकर कुछ अन्य ही कर बैठता है। यदि ऐसा न हो तो हम कर्म का अनुमान नहीं लगा सकते। वास्तव में चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से तरह-तरह की इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। इच्छा तब तक उत्पन्न होती रहती हैं, जब तक आत्मज्ञान पूर्वक आत्मस्वभाव में स्थिरता नहीं होती है। जो जीव स्वभाव में स्थिर होकर अपने स्वरूप का अनुभव करता है, उस जीव का चित्त वन के बीच में रहते हुए भी शान्त रस से भर जाता है और आनन्दित होता है। ऐसा ही व्यक्ति घनघोर संसार से छूट जाता है और उसे मोक्ष सुख की उपलब्धि होती है। अतः कर्मों के उदय का विचार कर उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कर्मों का सम्बन्ध सब पुरुषों के लिए समान होने पर भी ज्ञानी के लिए वह होने पर भी नहीं के बराबर होता है; जैसे तैरने में प्रवीण तैराक के लिए नदी का प्रवाह तेज होने पर भी बाधक नहीं होता है।(पद्मनन्दिपंचविशतिका-57)
अंबरि विविहु सदु जो सुम्मइ। तहिं पइसरहुं ण वुच्चइ दुम्मइ ॥ मणु पंचहिं सिहु अत्थवण जाइ।
मूढा परमतत्तु फुडु तिहि जि ठाइ ॥169॥ शब्दार्थ-अंबरि-आकाश. में; विविहु-विविध, अनेक तरह के सद्द-शब्द; जो सुम्मइ-सुना जाता है; तहिं-वहाँ; पइसरहुं-प्रवेश करो; ण वुच्चइ-नहीं कहा जाता है; दुम्मइ-दुर्मति (से); मणु-मन; पंचहिं-पाँचों (इन्द्रियों); सिहु-सहित, साथ; अत्थवण जाइ-अस्तंगत हो जाता है; मूढा-हे मूढ!; परमतत्तु-परमतत्त्व; फुडु-स्पष्ट (है); तिहि जि ठाइ-वहीं पर ही रहता है।
अर्थ-आकाश में जो तरह-तरह के शब्द सुनाई पड़ते हैं, वहाँ प्रवेश कर दुर्मति कुछ नहीं बोलता। जब मन पाँचों इन्द्रियों सहित विलीन हो जाता है, तब हे मूढ़! वह परमतत्त्व स्पष्ट रूप से वहीं ही रहता है। 1. अ, क, द, स सुम्मइ ब सम्मइ; 2. अ, ब, तहि क, द, स तहिं; 3. अ अंथवण; क अंथवणह; द, ब, स अत्थवण; 4. अ प्रति में 'फुडु' नहीं है...तिहि; क, द, ब, स तहिं।
198 : पाहुडदोहा