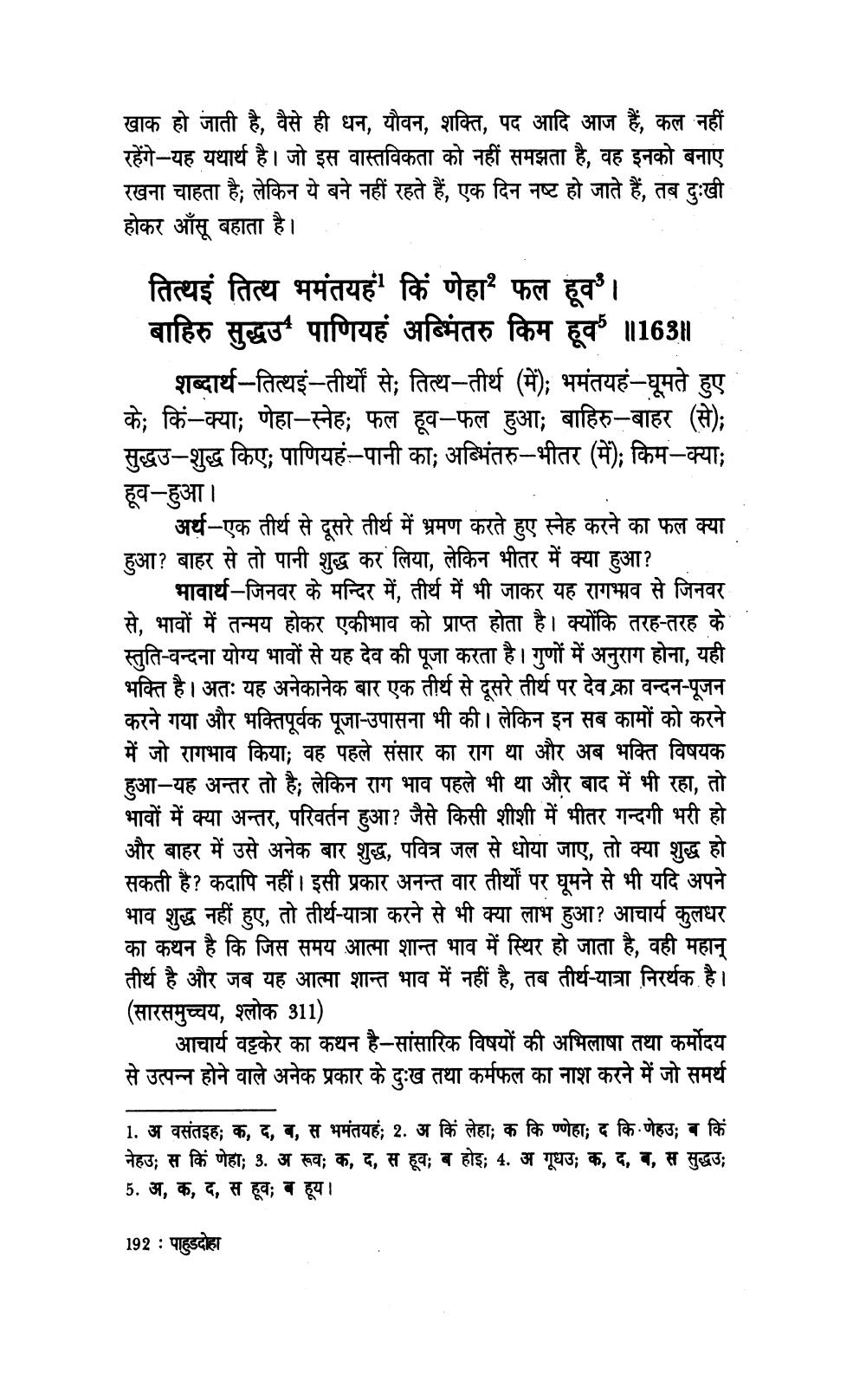________________
खाक हो जाती है, वैसे ही धन, यौवन, शक्ति, पद आदि आज हैं, कल नहीं रहेंगे-यह यथार्थ है। जो इस वास्तविकता को नहीं समझता है, वह इनको बनाए रखना चाहता है, लेकिन ये बने नहीं रहते हैं, एक दिन नष्ट हो जाते हैं, तब दुःखी होकर आँसू बहाता है।
तित्थई तित्थ भमंतयह किं हा फल हूव। बाहिरु सुद्धउ पाणियहं अमितरु किम हूव ॥163॥
शब्दार्थ-तित्थई-तीर्थों से; तित्थ-तीर्थ (में); भमंतयहं-घूमते हुए के; किं-क्या; णेहा-स्नेह; फल हूव-फल हुआ; बाहिरु-बाहर (से); सुद्धउ-शुद्ध किए; पाणियह-पानी का; अभिंतरु-भीतर (में); किम-क्या; हूव-हुआ।
अर्थ-एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में भ्रमण करते हुए स्नेह करने का फल क्या हुआ? बाहर से तो पानी शुद्ध कर लिया, लेकिन भीतर में क्या हुआ?
भावार्थ-जिनवर के मन्दिर में, तीर्थ में भी जाकर यह रागभाव से जिनवर से, भावों में तन्मय होकर एकीभाव को प्राप्त होता है। क्योंकि तरह-तरह के स्तुति-वन्दना योग्य भावों से यह देव की पूजा करता है। गुणों में अनुराग होना, यही भक्ति है। अतः यह अनेकानेक बार एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर देव का वन्दन-पूजन करने गया और भक्तिपूर्वक पूजा-उपासना भी की। लेकिन इन सब कामों को करने में जो रागभाव किया; वह पहले संसार का राग था और अब भक्ति विषयक हुआ-यह अन्तर तो है; लेकिन राग भाव पहले भी था और बाद में भी रहा, तो भावों में क्या अन्तर, परिवर्तन हुआ? जैसे किसी शीशी में भीतर गन्दगी भरी हो और बाहर में उसे अनेक बार शुद्ध, पवित्र जल से धोया जाए, तो क्या शुद्ध हो सकती है? कदापि नहीं। इसी प्रकार अनन्त वार तीर्थों पर घूमने से भी यदि अपने भाव शुद्ध नहीं हुए, तो तीर्थ-यात्रा करने से भी क्या लाभ हुआ? आचार्य कुलधर का कथन है कि जिस समय आत्मा शान्त भाव में स्थिर हो जाता है, वही महान् तीर्थ है और जब यह आत्मा शान्त भाव में नहीं है, तब तीर्थ-यात्रा निरर्थक है। (सारसमुच्चय, श्लोक 311)
आचार्य वट्टकर का कथन है-सांसारिक विषयों की अभिलाषा तथा कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के दुःख तथा कर्मफल का नाश करने में जो समर्थ
1. अ वसंतइह; क, द, ब, स भमंतयह; 2. अ किं लेहा; क कि ण्णेहा; द कि णेहउ; व किं नेहउ; स किं णेहा; 3. अ रूव; क, द, स हूव; ब होइ; 4. अ गूधउ; क, द, ब, स सुद्धउ; 5. अ, क, द, स हूव; ब हूय।
192 : पाहुडदोहा