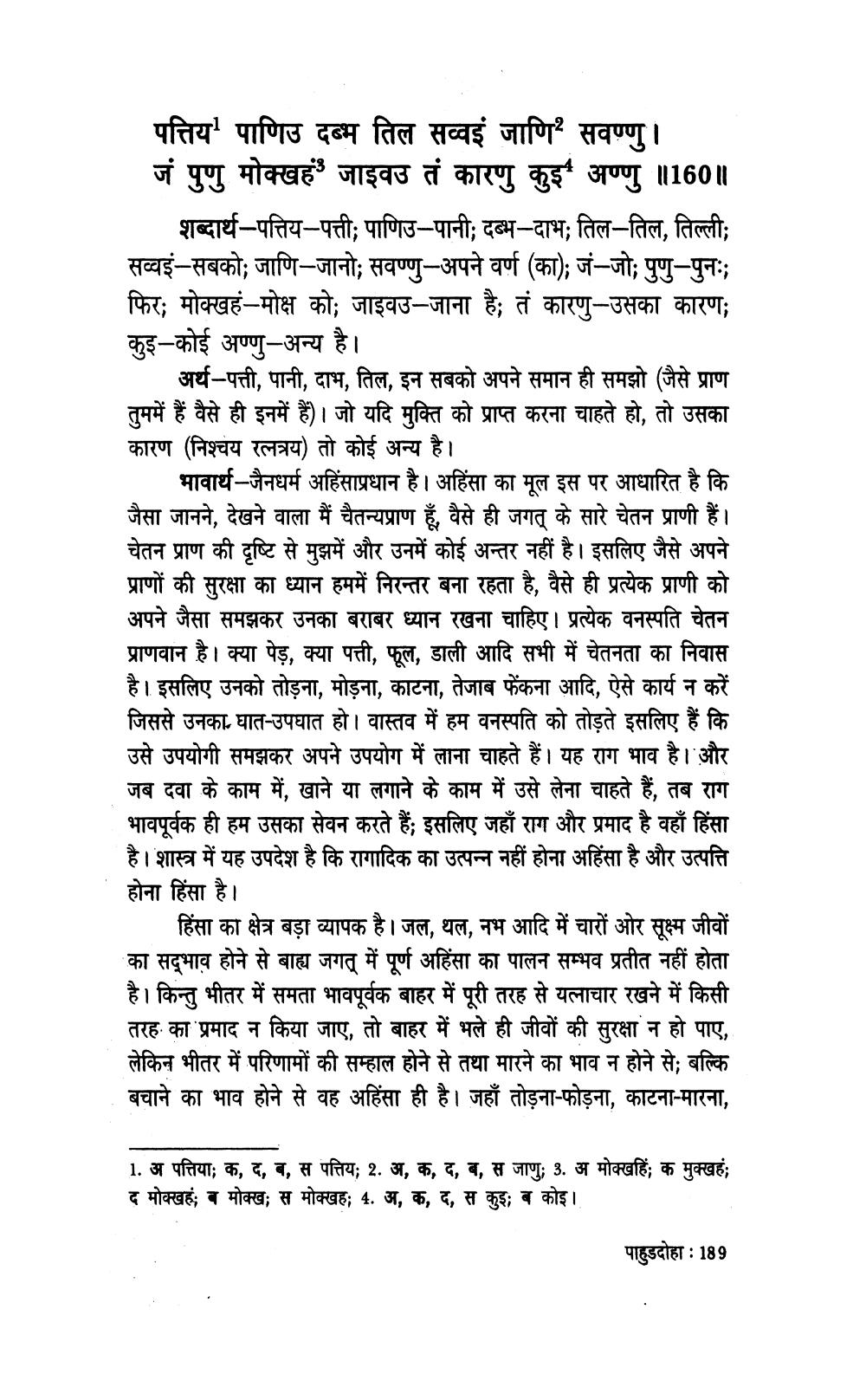________________
पत्तिय पाणिउ दब्भ तिल सव्वई जाणि' सवण्णु।
जं पुणु मोक्खहं जाइवउ तं कारणु कुइ' अण्णु ॥160॥ ___ शब्दार्थ-पत्तिय-पत्ती; पाणिउ-पानी; दब्भ-दाभ; तिल-तिल, तिल्ली; सव्वइं-सबको; जाणि-जानो; सवण्णु-अपने वर्ण (का); जं-जो; पुणु-पुनः; फिर; मोक्खहं-मोक्ष को; जाइवउ-जाना है; तं कारणु-उसका कारण; कुइ-कोई अण्णु-अन्य है।
अर्थ-पत्ती, पानी, दाभ, तिल, इन सबको अपने समान ही समझो (जैसे प्राण तुममें हैं वैसे ही इनमें हैं)। जो यदि मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका कारण (निश्चय रत्नत्रय) तो कोई अन्य है।
भावार्थ-जैनधर्म अहिंसाप्रधान है। अहिंसा का मूल इस पर आधारित है कि जैसा जानने, देखने वाला मैं चैतन्यप्राण हूँ, वैसे ही जगत् के सारे चेतन प्राणी हैं। चेतन प्राण की दृष्टि से मुझमें और उनमें कोई अन्तर नहीं है। इसलिए जैसे अपने प्राणों की सुरक्षा का ध्यान हममें निरन्तर बना रहता है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी को
अपने जैसा समझकर उनका बराबर ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक वनस्पति चेतन प्राणवान है। क्या पेड़, क्या पत्ती, फूल, डाली आदि सभी में चेतनता का निवास है। इसलिए उनको तोड़ना, मोड़ना, काटना, तेजाब फेंकना आदि, ऐसे कार्य न करें जिससे उनका घात-उपघात हो। वास्तव में हम वनस्पति को तोड़ते इसलिए हैं कि उसे उपयोगी समझकर अपने उपयोग में लाना चाहते हैं। यह राग भाव है। और जब दवा के काम में, खाने या लगाने के काम में उसे लेना चाहते हैं, तब राग भावपूर्वक ही हम उसका सेवन करते हैं, इसलिए जहाँ राग और प्रमाद है वहाँ हिंसा है। शास्त्र में यह उपदेश है कि रागादिक का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है और उत्पत्ति होना हिंसा है।
__ हिंसा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। जल, थल, नभ आदि में चारों ओर सूक्ष्म जीवों का सदभाव होने से बाह्य जगत में पूर्ण अहिंसा का पालन सम्भव प्रतीत नहीं होता है। किन्तु भीतर में समता भावपूर्वक बाहर में पूरी तरह से यत्नाचार रखने में किसी तरह का प्रमाद न किया जाए, तो बाहर में भले ही जीवों की सुरक्षा न हो पाए, लेकिन भीतर में परिणामों की सम्हाल होने से तथा मारने का भाव न होने से; बल्कि बचाने का भाव होने से वह अहिंसा ही है। जहाँ तोड़ना-फोड़ना, काटना-मारना,
1. अ पत्तिया; क, द, ब, स पत्तिय; 2. अ, क, द, ब, स जाणु; 3. अ मोक्खहिं; क मुक्खहं; द मोक्खह; व मोक्ख; स मोक्खह; 4. अ, क, द, स कुइ; व कोइ।
पाहुडदोहा : 189