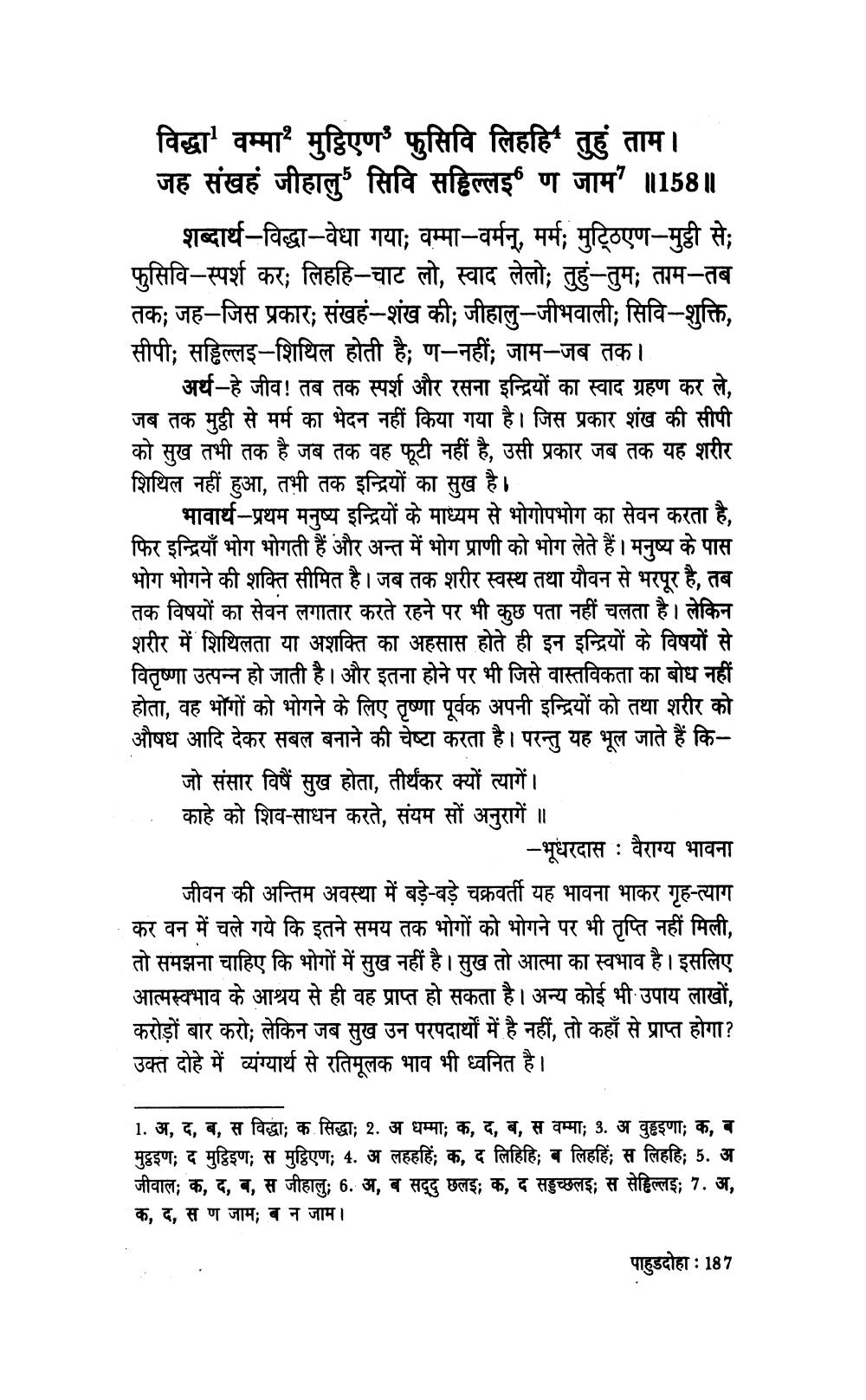________________
विद्धा' वम्मा' मुट्ठिएण' फुसिवि लिहहि तुहुं ताम । जह संखहं जीहालु सिवि सढिल्लई' ण जाम ॥158॥
शब्दार्थ-विद्धा-वेधा गया; वम्मा - वर्मनू, मर्म; मुट्ठिएण - मुट्ठी से; फुसिवि - स्पर्श कर; लिहहि - चाट लो, स्वाद लेलो; तुहुं- तुम; ताम- तब तक; जह - जिस प्रकार ; संखहं - शंख की जीहालु - जीभवाली, सिवि - शुक्ति, सीपी; सड्डिल्लइ–शिथिल होती है; ण-नहीं; जाम - जब तक ।
अर्थ - हे जीव ! तब तक स्पर्श और रसना इन्द्रियों का स्वाद ग्रहण कर ले, जब तक मुट्ठी से मर्म का भेदन नहीं किया गया है। जिस प्रकार शंख की सीपी को सुख तभी तक है जब तक वह फूटी नहीं है, उसी प्रकार जब तक यह शरीर शिथिल नहीं हुआ, तभी तक इन्द्रियों का सुख है ।
भावार्थ - प्रथम मनुष्य इन्द्रियों के माध्यम से भोगोपभोग का सेवन करता है, फिर इन्द्रियाँ भोग भोगती हैं और अन्त में भोग प्राणी को भोग लेते हैं। मनुष्य के पास भोग भोगने की शक्ति सीमित है। जब तक शरीर स्वस्थ तथा यौवन से भरपूर है, तब तक विषयों का सेवन लगातार करते रहने पर भी कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन शरीर में शिथिलता या अशक्ति का अहसास होते ही इन इन्द्रियों के विषयों से वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है । और इतना होने पर भी जिसे वास्तविकता का बोध नहीं होता, वह भोंगों को भोगने के लिए तृष्णा पूर्वक अपनी इन्द्रियों को तथा शरीर को औषध आदि देकर सबल बनाने की चेष्टा करता है । परन्तु यह भूल जाते हैं कि
-
जो संसार विषै सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागें । काहे को शिव-साधन करते, संयम सों अनुरागें ॥
- भूधरदास : वैराग्य भावना
जीवन की अन्तिम अवस्था में बड़े-बड़े चक्रवर्ती यह भावना भाकर गृह-त्याग कर वन में चले गये कि इतने समय तक भोगों को भोगने पर भी तृप्ति नहीं मिली, तो समझना चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। इसलिए आत्मस्वभाव के आश्रय से ही वह प्राप्त हो सकता है । अन्य कोई भी उपाय लाखों, करोड़ों बार करो; लेकिन जब सुख उन परपदार्थों में है नहीं, तो कहाँ से प्राप्त होगा ? उक्त दोहे में व्यंग्यार्थ से रतिमूलक भाव भी ध्वनित है।
1. अ, द, ब, स विद्धा; क सिद्धा; 2. अ धम्मा; क, द, ब, स वम्मा; 3. अ वुड्डइणा; क, ब मुट्ठइण; द मुट्ठिइण; स मुट्ठिएण; 4. अ लहहहिं; क, द लिहिहि; ब लिहहिं; स लिहहि; 5. अ जीवाल; क, द, ब, स जीहालु; 6. अ, ब सदु छलइ; क, द सड्डच्छलइ; स सेडिल्लइ; 7. अ, क, द, स ण जाम; ब न जाम।
पाहुदोहा : 187