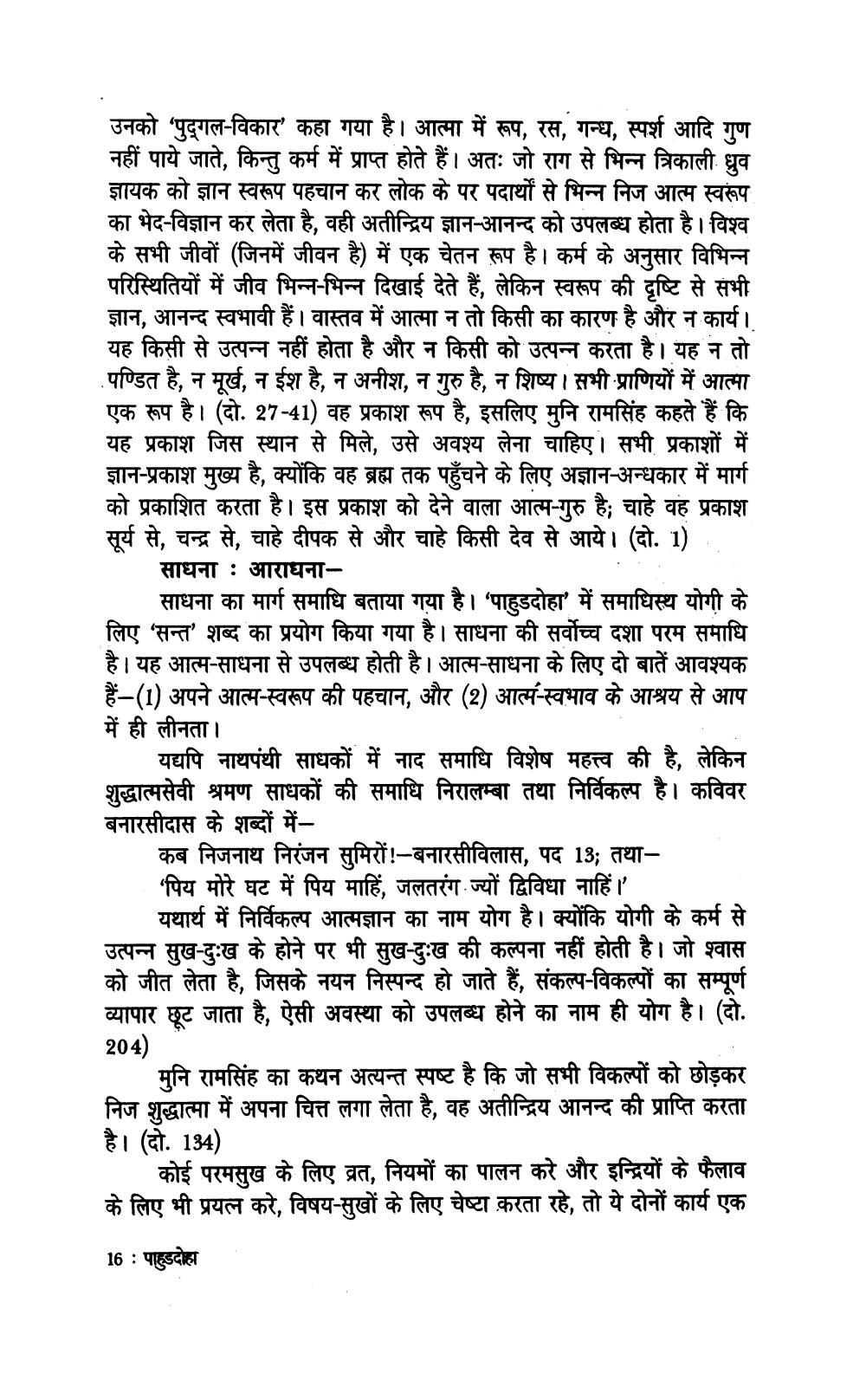________________
उनको ‘पुद्गल-विकार' कहा गया है। आत्मा में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि गुण नहीं पाये जाते, किन्तु कर्म में प्राप्त होते हैं। अतः जो राग से भिन्न त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक को ज्ञान स्वरूप पहचान कर लोक के पर पदार्थों से भिन्न निज आत्म स्वरूप का भेद-विज्ञान कर लेता है, वही अतीन्द्रिय ज्ञान-आनन्द को उपलब्ध होता है। विश्व के सभी जीवों (जिनमें जीवन है) में एक चेतन रूप है। कर्म के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में जीव भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से सभी ज्ञान, आनन्द स्वभावी हैं। वास्तव में आत्मा न तो किसी का कारण है और न कार्य। यह किसी से उत्पन्न नहीं होता है और न किसी को उत्पन्न करता है। यह न तो पण्डित है, न मूर्ख, न ईश है, न अनीश, न गुरु है, न शिष्य। सभी प्राणियों में आत्मा एक रूप है। (दो. 27-41) वह प्रकाश रूप है, इसलिए मुनि रामसिंह कहते हैं कि यह प्रकाश जिस स्थान से मिले, उसे अवश्य लेना चाहिए। सभी प्रकाशों में ज्ञान-प्रकाश मुख्य है, क्योंकि वह ब्रह्म तक पहुँचने के लिए अज्ञान-अन्धकार में मार्ग को प्रकाशित करता है। इस प्रकाश को देने वाला आत्म-गुरु है; चाहे वह प्रकाश सूर्य से, चन्द्र से, चाहे दीपक से और चाहे किसी देव से आये। (दो. 1) .
साधना : आराधना
साधना का मार्ग समाधि बताया गया है। ‘पाहुडदोहा' में समाधिस्थ योगी के लिए 'सन्त' शब्द का प्रयोग किया गया है। साधना की सर्वोच्च दशा परम समाधि है। यह आत्म-साधना से उपलब्ध होती है। आत्म-साधना के लिए दो बातें आवश्यक हैं-(1) अपने आत्म-स्वरूप की पहचान, और (2) आत्म-स्वभाव के आश्रय से आप में ही लीनता।
यद्यपि नाथपंथी साधकों में नाद समाधि विशेष महत्त्व की है, लेकिन शुद्धात्मसेवी श्रमण साधकों की समाधि निरालम्बा तथा निर्विकल्प है। कविवर बनारसीदास के शब्दों में
कब निजनाथ निरंजन सुमिरों!-बनारसीविलास, पद 13; तथा'पिय मोरे घट में पिय माहिं, जलतरंग ज्यों द्विविधा नाहिं।'
यथार्थ में निर्विकल्प आत्मज्ञान का नाम योग है। क्योंकि योगी के कर्म से उत्पन्न सुख-दुःख के होने पर भी सुख-दुःख की कल्पना नहीं होती है। जो श्वास को जीत लेता है, जिसके नयन निस्पन्द हो जाते हैं, संकल्प-विकल्पों का सम्पूर्ण व्यापार छूट जाता है, ऐसी अवस्था को उपलब्ध होने का नाम ही योग है। (दो. 204)
मुनि रामसिंह का कथन अत्यन्त स्पष्ट है कि जो सभी विकल्पों को छोड़कर निज शुद्धात्मा में अपना चित्त लगा लेता है, वह अतीन्द्रिय आनन्द की प्राप्ति करता है। (दो. 134)
कोई परमसुख के लिए व्रत, नियमों का पालन करे और इन्द्रियों के फैलाव के लिए भी प्रयत्न करे, विषय-सुखों के लिए चेष्टा करता रहे, तो ये दोनों कार्य एक 16 : पाहुडदोहा