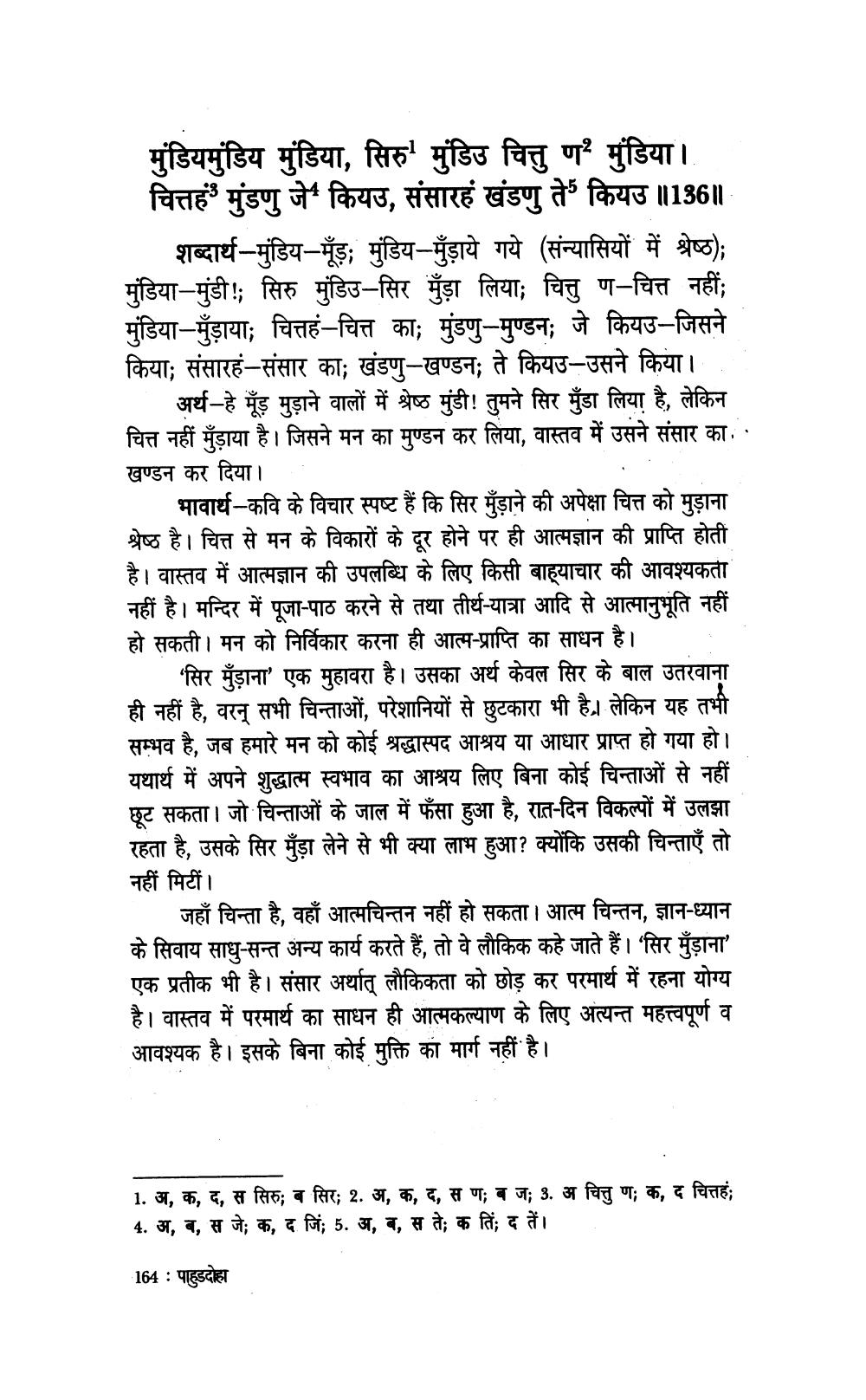________________
मुंडियमुंडिय मुंडिया, सिरु' मुंडिउ चित्तु ण मुंडिया। चित्तह मुंडणु जे कियउ, संसारहं खंडणु ते कियउ॥136॥
शब्दार्थ-मुंडिय-मूंड; मुंडिय-मुंडाये गये (संन्यासियों में श्रेष्ठ); मुंडिया-मुंडी!; सिरु मुंडिउ-सिर मुंडा लिया; चित्तु ण-चित्त नहीं; मुंडिया-मुंडाया; चित्तहं-चित्त का; मुंडणु-मुण्डन; जे कियउ-जिसने किया; संसारहं-संसार का; खंडणु-खण्डन; ते कियउ-उसने किया। ___अर्थ-हे मूंड़ मुड़ाने वालों में श्रेष्ठ मुंडी! तुमने सिर मुंडा लिया है, लेकिन चित्त नहीं मुंडाया है। जिसने मन का मुण्डन कर लिया, वास्तव में उसने संसार का. . खण्डन कर दिया।
भावार्थ-कवि के विचार स्पष्ट हैं कि सिर मुंडाने की अपेक्षा चित्त को मुड़ाना श्रेष्ठ है। चित्त से मन के विकारों के दूर होने पर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तव में आत्मज्ञान की उपलब्धि के लिए किसी बाह्याचार की आवश्यकता नहीं है। मन्दिर में पूजा-पाठ करने से तथा तीर्थ यात्रा आदि से आत्मानुभूति नहीं हो सकती। मन को निर्विकार करना ही आत्म-प्राप्ति का साधन है।
___ 'सिर मुंडाना' एक मुहावरा है। उसका अर्थ केवल सिर के बाल उतरवाना ही नहीं है, वरन् सभी चिन्ताओं, परेशानियों से छुटकारा भी है। लेकिन यह तभी सम्भव है, जब हमारे मन को कोई श्रद्धास्पद आश्रय या आधार प्राप्त हो गया हो। यथार्थ में अपने शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय लिए बिना कोई चिन्ताओं से नहीं छूट सकता। जो चिन्ताओं के जाल में फँसा हुआ है, रात-दिन विकल्पों में उलझा रहता है, उसके सिर मुंडा लेने से भी क्या लाभ हुआ? क्योंकि उसकी चिन्ताएँ तो नहीं मिटीं।
जहाँ चिन्ता है, वहाँ आत्मचिन्तन नहीं हो सकता। आत्म चिन्तन, ज्ञान-ध्यान के सिवाय साधु-सन्त अन्य कार्य करते हैं, तो वे लौकिक कहे जाते हैं। 'सिर मुंडाना' एक प्रतीक भी है। संसार अर्थात् लौकिकता को छोड़ कर परमार्थ में रहना योग्य है। वास्तव में परमार्थ का साधन ही आत्मकल्याण के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व आवश्यक है। इसके बिना कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है।
1. अ, क, द, स सिरु; ब सिर; 2. अ, क, द, स ण; ब ज; 3. अ चित्तु ण; क, द चित्तहं; 4. अ, ब, स जे; क, द जिं; 5. अ, ब, स ते; क तिं; द तें।
164 : पाहुडदोहा