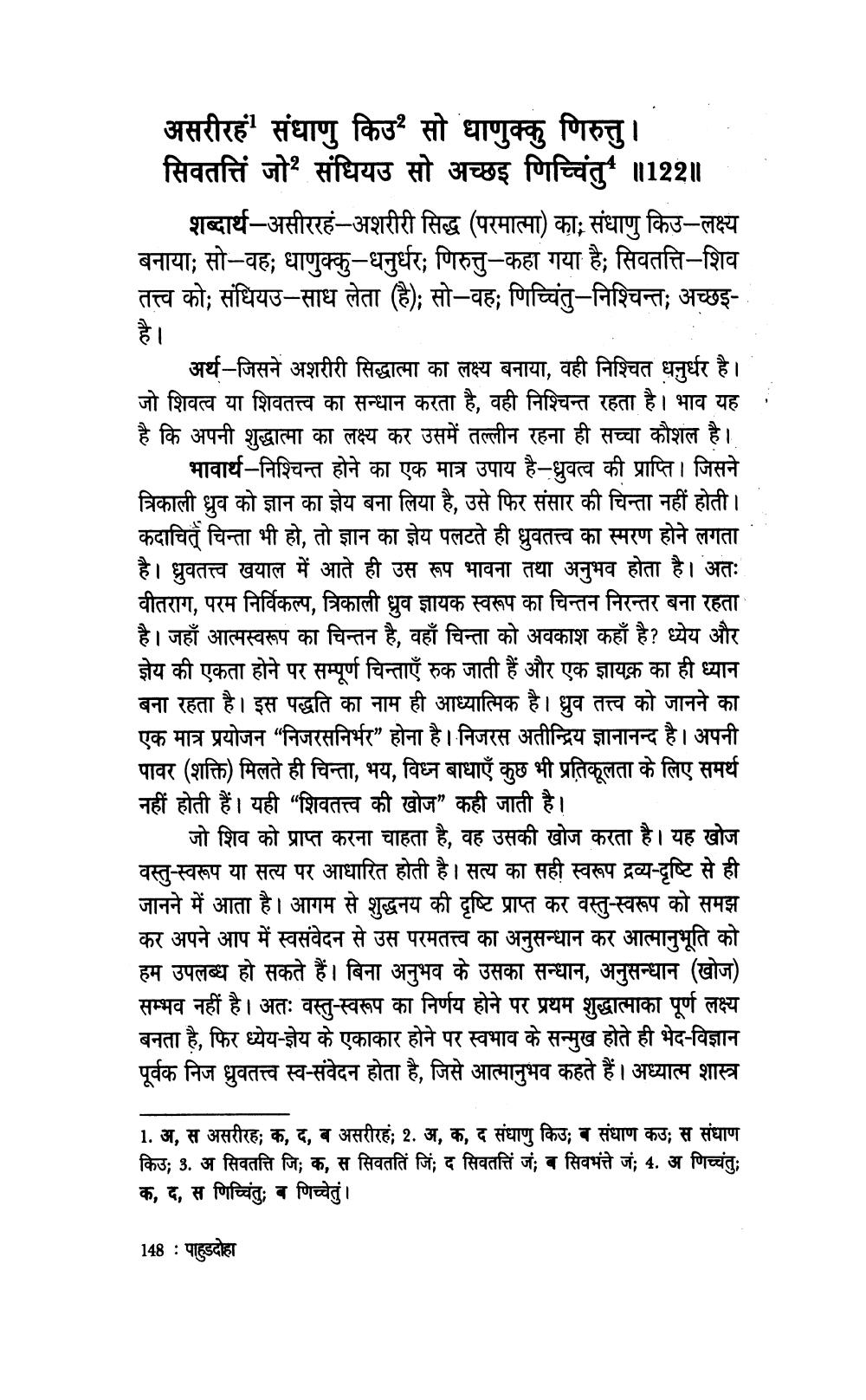________________
असरीरहं' संधाणु किउ' सो धाणुक्कु णिरुत्तु । सिवतत्तिं जो' संघियउ सो अच्छइ णिच्विंतु ॥122॥
शब्दार्थ - असीररहं- अशरीरी सिद्ध (परमात्मा) का संधाणु किउ - लक्ष्य बनाया; सो - वह; धाणुक्कु- धनुर्धर; णिरुत्तु - कहा गया है; सिवतत्ति-शिव तत्त्व को; संधियउ-साध लेता (है); सो - वह; णिच्चिंतु–निश्चिन्त; अच्छइ
1
अर्थ-जिसने अशरीरी सिद्धात्मा का लक्ष्य बनाया, वही निश्चित धनुर्धर है । जो शिवत्व या शिवतत्त्व का सन्धान करता है, वही निश्चिन्त रहता है । भाव यह है कि अपनी शुद्धात्मा का लक्ष्य कर उसमें तल्लीन रहना ही सच्चा कौशल है । भावार्थ - निश्चिन्त होने का एक मात्र उपाय है - ध्रुवत्व की प्राप्ति । जिसने त्रिकाली ध्रुव को ज्ञान का ज्ञेय बना लिया है, उसे फिर संसार की चिन्ता नहीं होती । कदाचित् चिन्ता भी हो, तो ज्ञान का ज्ञेय पलटते ही ध्रुवतत्त्व का स्मरण होने लगता है । ध्रुवतत्त्व खयाल में आते ही उस रूप भावना तथा अनुभव होता है। अतः वीतराग, परम निर्विकल्प, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप का चिन्तन निरन्तर बना रहता है । जहाँ आत्मस्वरूप का चिन्तन है, वहाँ चिन्ता को अवकाश कहाँ है? ध्येय और ज्ञेय की एकता होने पर सम्पूर्ण चिन्ताएँ रुक जाती हैं और एक ज्ञायक का ही ध्यान बना रहता है। इस पद्धति का नाम ही आध्यात्मिक है । ध्रुव तत्त्व को जानने का एक मात्र प्रयोजन "निजरसनिर्भर ” होना है । निजरस अतीन्द्रिय ज्ञानानन्द है । अपनी पावर (शक्ति) मिलते ही चिन्ता, भय, विघ्न बाधाएँ कुछ भी प्रतिकूलता के लिए समर्थ नहीं होती हैं । यही “शिवतत्त्व की खोज” कही जाती है ।
जो शिव को प्राप्त करना चाहता है, वह उसकी खोज करता है। यह खोज वस्तु-स्वरूप या सत्य पर आधारित होती है । सत्य का सही स्वरूप द्रव्य-दृष्टि से ही जानने में आता है। आगम से शुद्धनय की दृष्टि प्राप्त कर वस्तु-स्वरूप को समझ कर अपने आप में स्वसंवेदन से उस परमतत्त्व का अनुसन्धान कर आत्मानुभूति को हम उपलब्ध हो सकते हैं। बिना अनुभव के उसका सन्धान, अनुसन्धान (खोज) सम्भव नहीं है। अतः वस्तु स्वरूप का निर्णय होने पर प्रथम शुद्धात्माका पूर्ण लक्ष्य बनता है, फिर ध्येय - ज्ञेय के एकाकार होने पर स्वभाव के सन्मुख होते ही भेद - विज्ञान पूर्वक निज ध्रुवतत्त्व स्व-संवेदन होता है, जिसे आत्मानुभव कहते हैं । अध्यात्म शास्त्र
1. अ, स असरीरह; क, द, ब असरीरहं; 2. अ, क, द संघाणु किउ; व संधाण कउ स संधाण किउ; 3. असिवतत्ति जि; क, स सिवततिं जिं; द सिवतत्तिं जं; ब सिवभंत्ते जं; 4. अ णिच्चंतु; क, द, स णिच्छिंतु; ब णिच्चेतुं ।
148 : पाहु