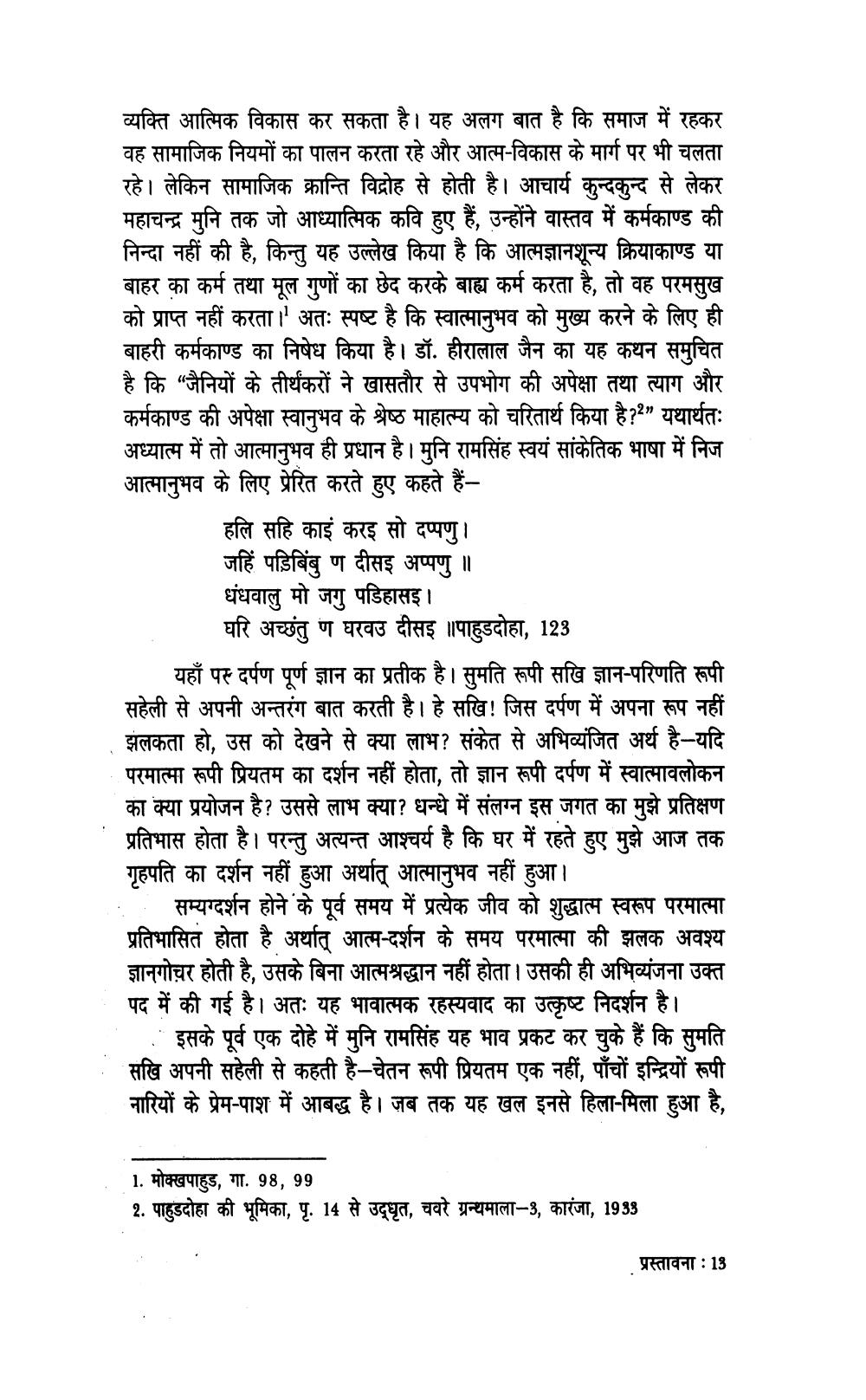________________
व्यक्ति आत्मिक विकास कर सकता है। यह अलग बात है कि समाज में रहकर वह सामाजिक नियमों का पालन करता रहे और आत्म-विकास के मार्ग पर भी चलता रहे। लेकिन सामाजिक क्रान्ति विद्रोह से होती है। आचार्य कुन्दकुन्द से लेकर महाचन्द्र मुनि तक जो आध्यात्मिक कवि हुए हैं, उन्होंने वास्तव में कर्मकाण्ड की निन्दा नहीं की है, किन्तु यह उल्लेख किया है कि आत्मज्ञानशून्य क्रियाकाण्ड या बाहर का कर्म तथा मूल गुणों का छेद करके बाह्य कर्म करता है, तो वह परमसुख को प्राप्त नहीं करता। अतः स्पष्ट है कि स्वात्मानुभव को मुख्य करने के लिए ही बाहरी कर्मकाण्ड का निषेध किया है। डॉ. हीरालाल जैन का यह कथन समुचित है कि “जैनियों के तीर्थंकरों ने खासतौर से उपभोग की अपेक्षा तथा त्याग और कर्मकाण्ड की अपेक्षा स्वानुभव के श्रेष्ठ माहात्म्य को चरितार्थ किया है?" यथार्थतः अध्यात्म में तो आत्मानुभव ही प्रधान है। मुनि रामसिंह स्वयं सांकेतिक भाषा में निज आत्मानुभव के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं
हलि सहि काइं करइ सो दप्पणु। जहिं पडिबिंबु ण दीसइ अप्पणु ॥ धंधवालु मो जगु पडिहासइ।
घरि अच्छंतु ण घरवउ दीसइ ॥पाहुडदोहा, 123 यहाँ पर दर्पण पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। सुमति रूपी सखि ज्ञान-परिणति रूपी सहेली से अपनी अन्तरंग बात करती है। हे सखि! जिस दर्पण में अपना रूप नहीं झलकता हो, उस को देखने से क्या लाभ? संकेत से अभिव्यंजित अर्थ है-यदि परमात्मा रूपी प्रियतम का दर्शन नहीं होता, तो ज्ञान रूपी दर्पण में स्वात्मावलोकन का क्या प्रयोजन है? उससे लाभ क्या? धन्धे में संलग्न इस जगत का मुझे प्रतिक्षण प्रतिभास होता है। परन्तु अत्यन्त आश्चर्य है कि घर में रहते हुए मुझे आज तक गृहपति का दर्शन नहीं हुआ अर्थात् आत्मानुभव नहीं हुआ।
सम्यग्दर्शन होने के पूर्व समय में प्रत्येक जीव को शुद्धात्म स्वरूप परमात्मा प्रतिभासित होता है अर्थात् आत्म-दर्शन के समय परमात्मा की झलक अवश्य ज्ञानगोचर होती है, उसके बिना आत्मश्रद्धान नहीं होता। उसकी ही अभिव्यंजना उक्त पद में की गई है। अतः यह भावात्मक रहस्यवाद का उत्कृष्ट निदर्शन है।
. इसके पूर्व एक दोहे में मुनि रामसिंह यह भाव प्रकट कर चुके हैं कि सुमति सखि अपनी सहेली से कहती है-चेतन रूपी प्रियतम एक नहीं, पाँचों इन्द्रियों रूपी नारियों के प्रेम-पाश में आबद्ध है। जब तक यह खल इनसे हिला-मिला हुआ है,
1. मोक्खपाहुड, गा. 98, 99 2. पाहुडदोहा की भूमिका, पृ. 14 से उद्धृत, चवरे ग्रन्थमाला-3, कारंजा, 1933
प्रस्तावना: 13