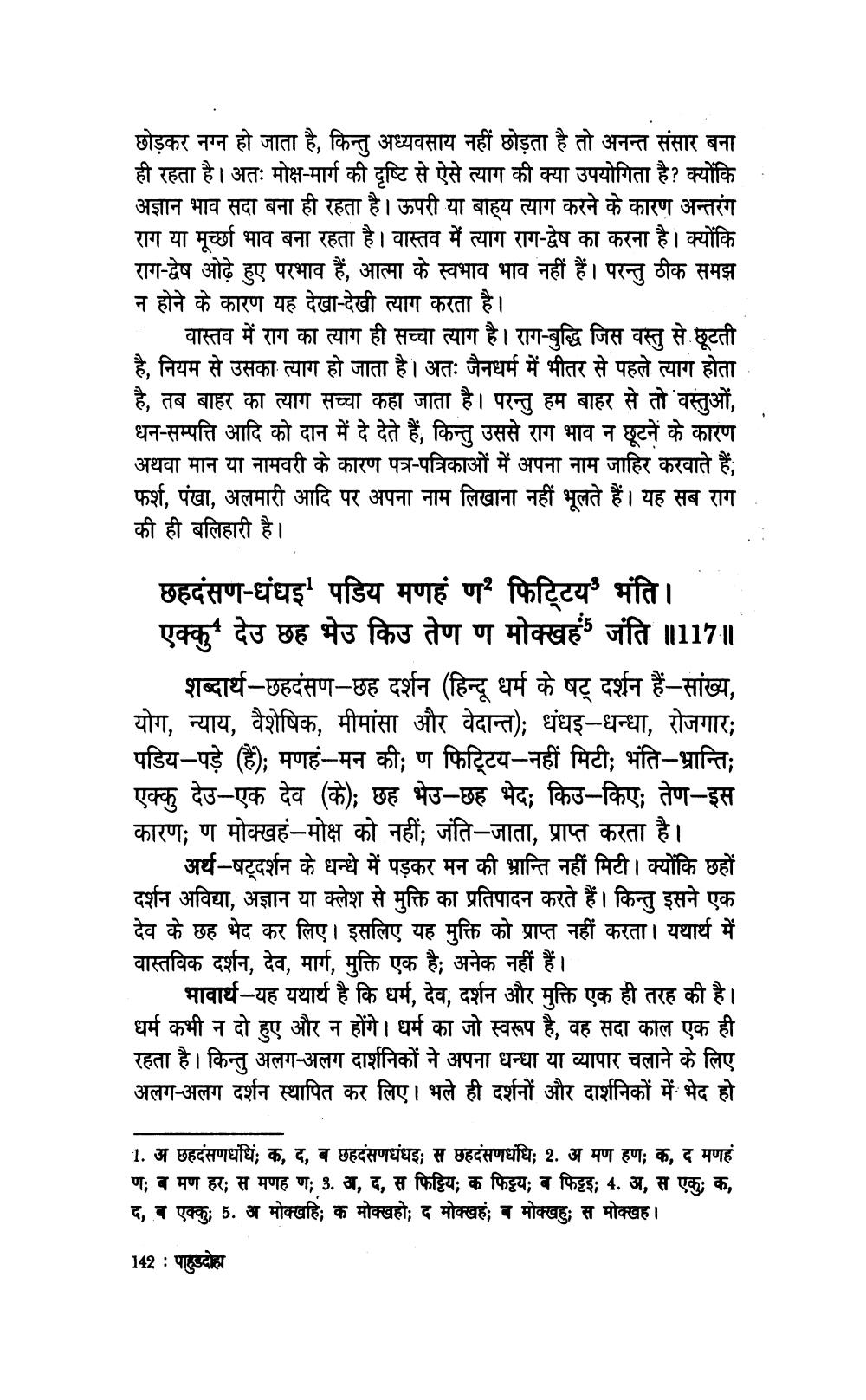________________
छोड़कर नग्न हो जाता है, किन्तु अध्यवसाय नहीं छोड़ता है तो अनन्त संसार बना ही रहता है। अतः मोक्ष-मार्ग की दृष्टि से ऐसे त्याग की क्या उपयोगिता है? क्योंकि अज्ञान भाव सदा बना ही रहता है। ऊपरी या बाह्य त्याग करने के कारण अन्तरंग राग या मूर्छा भाव बना रहता है। वास्तव में त्याग राग-द्वेष का करना है। क्योंकि राग-द्वेष ओढ़े हुए परभाव हैं, आत्मा के स्वभाव भाव नहीं हैं। परन्तु ठीक समझ न होने के कारण यह देखा-देखी त्याग करता है। - वास्तव में राग का त्याग ही सच्चा त्याग है। राग-बुद्धि जिस वस्तु से छूटती है, नियम से उसका त्याग हो जाता है। अतः जैनधर्म में भीतर से पहले त्याग होता है, तब बाहर का त्याग सच्चा कहा जाता है। परन्तु हम बाहर से तो वस्तुओं, धन-सम्पत्ति आदि को दान में दे देते हैं, किन्तु उससे राग भाव न छूटने के कारण अथवा मान या नामवरी के कारण पत्र-पत्रिकाओं में अपना नाम जाहिर करवाते हैं, फर्श, पंखा, अलमारी आदि पर अपना नाम लिखाना नहीं भूलते हैं। यह सब राग की ही बलिहारी है।
छहदसण-धंधइ पडिय मणहं ण' फिट्टिय मंति। एक्कु देउ छह भेउ किउ तेण ण मोक्खह जंति ॥17॥
शब्दार्थ-छहदसण-छह दर्शन (हिन्दू धर्म के षट् दर्शन हैं-सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त); धंधइ-धन्धा, रोजगार; पडिय-पड़े हैं); मणहं-मन की; ण फिट्टिय-नहीं मिटी; भंति-भ्रान्ति; एक्कु देउ-एक देव (के); छह भेउ-छह भेद; किउ-किए; तेण-इस कारण; ण मोक्खहं-मोक्ष को नहीं; जंति-जाता, प्राप्त करता है।
अर्थ-षट्दर्शन के धन्धे में पड़कर मन की भ्रान्ति नहीं मिटी। क्योंकि छहों दर्शन अविद्या, अज्ञान या क्लेश से मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं। किन्तु इसने एक देव के छह भेद कर लिए। इसलिए यह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। यथार्थ में वास्तविक दर्शन, देव, मार्ग, मुक्ति एक है; अनेक नहीं हैं।
भावार्थ-यह यथार्थ है कि धर्म, देव, दर्शन और मुक्ति एक ही तरह की है। धर्म कभी न दो हुए और न होंगे। धर्म का जो स्वरूप है, वह सदा काल एक ही रहता है। किन्तु अलग-अलग दार्शनिकों ने अपना धन्धा या व्यापार चलाने के लिए अलग-अलग दर्शन स्थापित कर लिए। भले ही दर्शनों और दार्शनिकों में भेद हो
1. अ छहदंसणधंधि; क, द, ब छहदसणधंध; स छहदसणधंधि; 2. अ मण हण; क, द मणहं ण; ब मण हर; स मणह ण; 3. अ, द, स फिट्टिय; क फिट्टय; व फिट्टइ; 4. अ, स एकु; क, द, व एक्कु; 5. अ मोक्खहि; क मोक्खहो; द मोक्खह; व मोक्खहुः स मोक्खह।
142 : पाहुडदोहा