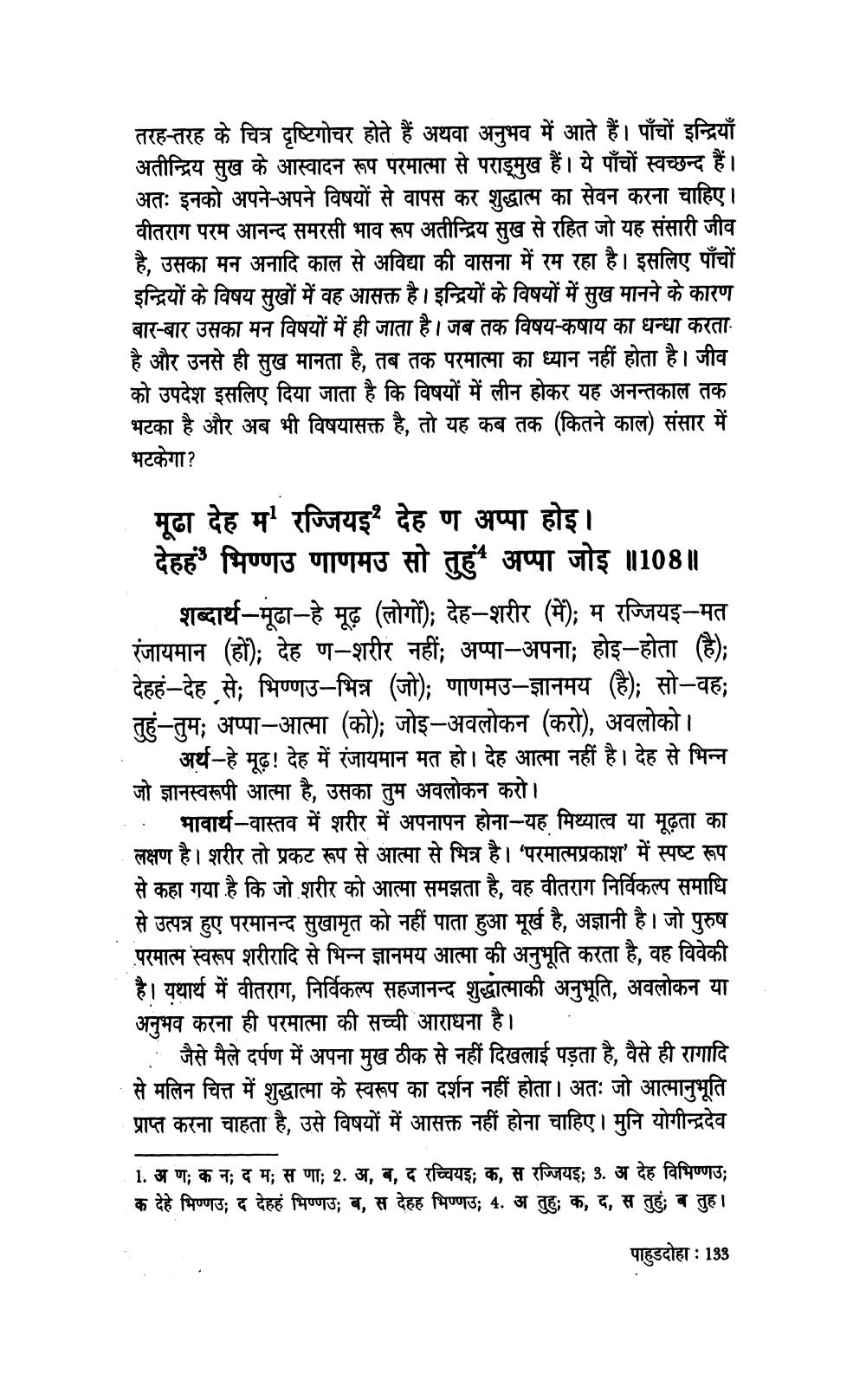________________
तरह-तरह के चित्र दृष्टिगोचर होते हैं अथवा अनुभव में आते हैं। पाँचों इन्द्रियाँ अतीन्द्रिय सुख के आस्वादन रूप परमात्मा से पराङ्मुख हैं। ये पाँचों स्वच्छन्द हैं। अतः इनको अपने-अपने विषयों से वापस कर शुद्धात्म का सेवन करना चाहिए। वीतराग परम आनन्द समरसी भाव रूप अतीन्द्रिय सुख से रहित जो यह संसारी जीव है, उसका मन अनादि काल से अविद्या की वासना में रम रहा है। इसलिए पाँचों इन्द्रियों के विषय सुखों में वह आसक्त है। इन्द्रियों के विषयों में सुख मानने के कारण बार-बार उसका मन विषयों में ही जाता है। जब तक विषय-कषाय का धन्धा करता है और उनसे ही सुख मानता है, तब तक परमात्मा का ध्यान नहीं होता है। जीव को उपदेश इसलिए दिया जाता है कि विषयों में लीन होकर यह अनन्तकाल तक भटका है और अब भी विषयासक्त है, तो यह कब तक (कितने काल) संसार में भटकेगा?
मूढा देह म रज्जियइ देह ण अप्पा होइ। देहह भिण्णउ णाणमउ सो तुहुँ' अप्पा जोइ ॥108॥
शब्दार्थ-मूढा-हे मूढ़ (लोगों); देह-शरीर (में); म रज्जियइ-मत रंजायमान (हों); देह ण-शरीर नहीं; अप्पा-अपना; होइ-होता (है); देहहं-देह से; भिण्णउ-भिन्न (जो); णाणमउ-ज्ञानमय (है); सो-वह; तुहुं-तुम; अप्पा-आत्मा (को); जोइ-अवलोकन (करो), अवलोको।।
अर्थ-हे मूढ़! देह में रंजायमान मत हो। देह आत्मा नहीं है। देह से भिन्न जो ज्ञानस्वरूपी आत्मा है, उसका तुम अवलोकन करो। . भावार्थ-वास्तव में शरीर में अपनापन होना-यह मिथ्यात्व या मूढ़ता का लक्षण है। शरीर तो प्रकट रूप से आत्मा से भिन्न है। 'परमात्मप्रकाश' में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो शरीर को आत्मा समझता है, वह वीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुए परमानन्द सुखामृत को नहीं पाता हुआ मूर्ख है, अज्ञानी है। जो पुरुष परमात्म स्वरूप शरीरादि से भिन्न ज्ञानमय आत्मा की अनुभूति करता है, वह विवेकी है। यथार्थ में वीतराग, निर्विकल्प सहजानन्द शुद्धात्माकी अनुभूति, अवलोकन या अनुभव करना ही परमात्मा की सच्ची आराधना है। ... जैसे मैले दर्पण में अपना मुख ठीक से नहीं दिखलाई पड़ता है, वैसे ही रागादि से मलिन चित्त में शुद्धात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं होता। अतः जो आत्मानुभूति प्राप्त करना चाहता है, उसे विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। मुनि योगीन्द्रदेव
1. अ ण; क न; द म; स णा; 2. अ, ब, द रच्चियइ; क, स रज्जियइ; 3. अ देह विभिण्णउ; क देहे भिण्णउ; द देहहं भिण्णउ; ब, स देहह भिण्णउ; 4. अ तुहु; क, द, स तुहूं; व तुह।
पाहुडदोहा : 133